
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
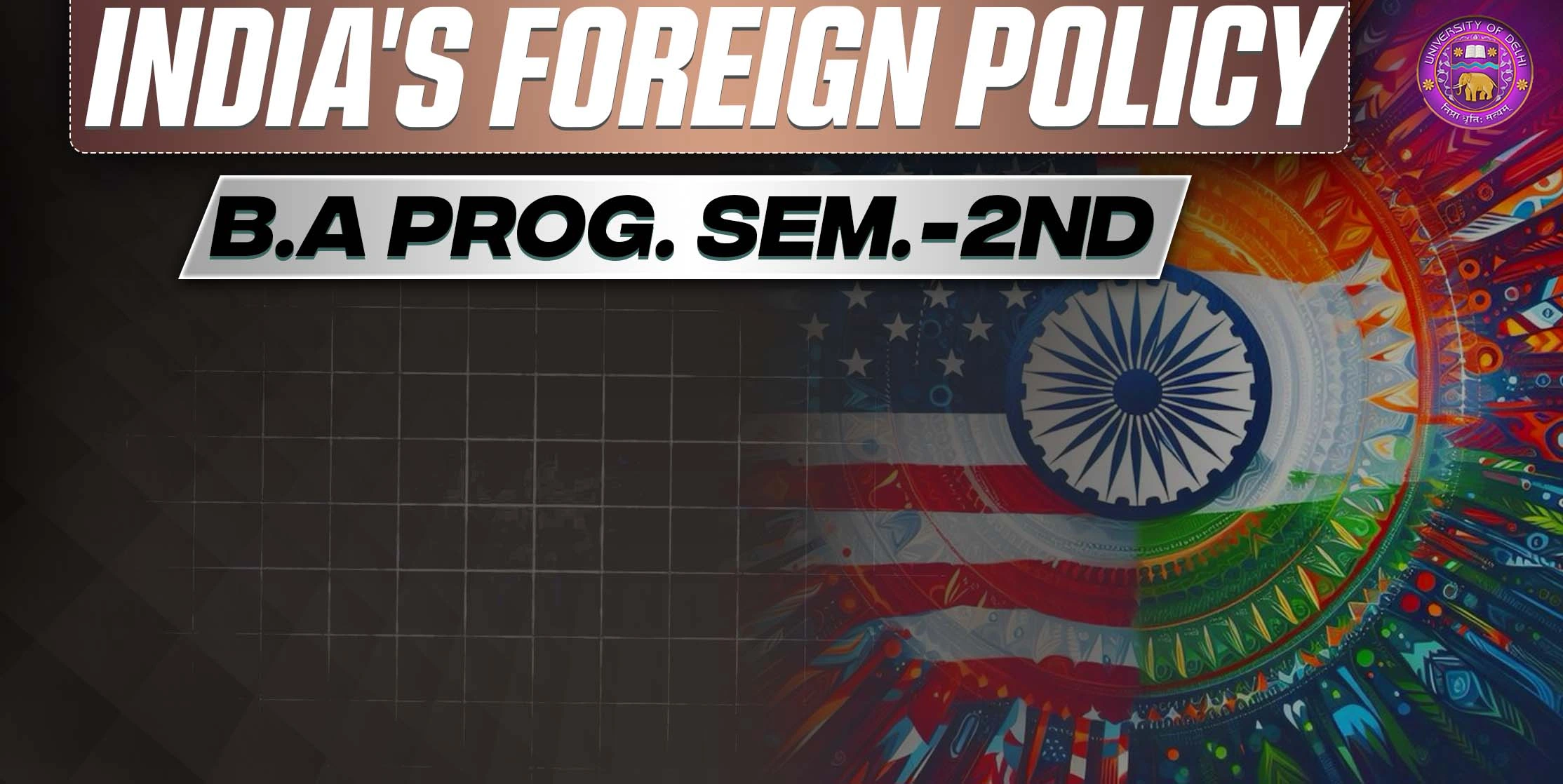
उत्तर - परिचय
किसी भी स्वतन्त्र व प्रभुसत्तासम्पन्न देश की विदेश नीति मूल रूप में उन सिद्धान्तों, हितों तथा लक्ष्यों का समूह होती है जिनके माध्यम से वह देश दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने, उन सिद्धान्तों, हितों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत् रहता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी आन्तरिक नीति का ही एक भाग होती है जिसे उस देश की सरकार ने बनाया है। वास्तव में विदेश नीति शासक वर्ग की इच्छा का परिणाम होती है जिसे क्रियान्वित करना सरकारी व गैर-सरकारी अभिकरणों का प्रमुख कर्त्तव्य है ।
विदेश नीति को कई विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :-
मॉडेल्स्की के अनुसार:- "कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय करता है, विदेश नीति कहलाती है। "
ग्लाइचर के अनुसार:- " अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य सम्बन्धों का संचालित करने के लिए करता है।"
वाल्ट्ज के अनुसार:- किसी भी देश की विदेश नीति को उसके हितों को बढ़ावा देने वाली अर्थात् राष्ट्रीय हित में निहित शब्दावली से जाना जाता है।
भारतीय विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक तत्व:

किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण अनेक तत्वों से होता है। इसके पीछे मूल विचार यह होता है कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन विदेश नीति पहले जैसी ही रहती है। यद्यपि व्यवहार में तो कुछ अन्तर अवश्य हो सकता है, परन्तु सिद्धान्त तौर पर विदेश नीति के लक्ष्य व सिद्धान्त पहले जैसे ही रहते हैं ।
उदाहरण के रूप में हम भारत की विदेश नीति को ले सकते हैं। भारत में नेहरु युग से वर्तमान वाजपेयी युग तक विदेश नीति के अधिकार सिद्धान्त वही हैं जो नेहरु जी ने दिए थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि विदेश नीति का निर्धारण कुछ स्थायी तत्वों से होता है जिसके कारण विदेश नीति की गतिशीलता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।
फैडल फोर्ड और लिंकन का कहना है-“मूल रूप से विदेश नीति की जड़ें ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, राजनीतिक संस्थाओं, परम्पराओं, आर्थिक आवश्यकताओं, शक्ति के तत्वों, अभिलाषाओं, भौगोलिक परिस्थितियों तथा राष्ट्र के मूल्यों में पाई जाती हैं"
ब्रेशर भी विदेश नीति के निर्धारिक तत्वों में भूगोल, अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश, व्यक्तित्व, आर्थिक और सैनिक स्थिति तथा जनमत को शामिल करता है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत की विदेश नीति का निर्धारण भी इन्हीं तत्वों के आधार पर होता है।
ये तत्व निम्नलिखित हैं:-
भूगोल (Geography) :- किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उस देश की विदेश नीति का निर्धारण करती है। जो देश भौगोलिक दृष्टी से सुरक्षित होता है, वह स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्माण कर सकता है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। देश के विशाल आकार, उसकी जलवायु, उसकी अवस्थिति (Location) और भू-आकृति (Topography) ने भारत की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत उत्तर में हिमालय तथा बाकी तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। जहां यह स्थिति भारत को सुरक्षित राष्ट्र घोषित करती है, वहीं यह सामरिक दृष्टी से भारत के लिए चिन्ता का कारण भी है।
भारत को हिमालय क्षेत्र से घुसपैठ रोकने के लिए तथा अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारी सैनिक व्यय करना पड़ता है। समुद्री मार्ग भारत के व्यापार के लिए जितने आवश्यक है, उनकी सुरक्षा के लिए उतना ही भारी व्यय भारत को करना पड़ता है। भारत की भौगोलिक स्थिति पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है। हिन्द महासागर के क्षेत्र में बढ़ती अमेरिका, रूस व ब्रिटेन की गतिविधियों से उसका चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। इसलिए वह संयुक्त राष्ट्र संघ मे हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र (Zone of Peace) घोषित करवाने का प्रयास करता रहता है। पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियां भी उसकी चिन्ता का कारण है।
आर्थिक व सैनिक तत्व (Economic and Military Factors) :- अपनी स्वतन्त्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास की थी। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी होता है कि उस देश के साथ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन व उनके दोहन की क्षमता हो। भारत के पास प्राकृतिक साधन तो प्रचूर मात्रा में थे, लेकिन उनका दोहन करने के लिए पूंजी व तकनीक का अभाव था । इसलिए भारत ने अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों से सम्बन्ध स्थापित किए। साथ में उसने रूस को भी नाराज नहीं किया। इसलिए उसने गुट निरपेक्षता का पालन करते हुए विश्व की दोनों महाशक्तियों से सम्बन्ध जोड़े रखे। इससे उसकी विदेश नीति की स्वतन्त्रता भी बरकरार रही। यद्यपि बार-बार भारत पर अमेरिका व रूस द्वारा दबाव बनाया गया कि वह उनके साथ शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने ऐसा न करके अपनी प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा की, परन्तु आर्थिक निर्भरता ने भारत को बौद्धिक सम्पदा कानून व बहुराष्ट्रीय निगमों की अनुचित शर्तों को मानना पड़ा है।
आज भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक उदारीकरण के दौर में है। और वह WTO के नियन्त्रण में है । यद्यपि भारत अपने निकटवर्ती देशों के साथ मिलकर दक्षिण एशिया के देशों में पारस्परिक अन्तनिर्भरता का विकास करना चाहता है। इसके लिए वह ASEAN तथा SAARC में SAFTA का विचार रखकर दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी भारत WTO के अमीर देशों पर निर्भरता कम नहीं हुई है। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह विकास का राजनय (diplomacy) अपनाए। लेकिन उसे ऐसा करते समय अपनी सम्प्रभुता व प्रादेशिक अखण्डता का ध्यान रखना चाहिएं यद्यपि भारत आज नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) की मांग भी करता है, लेकिन वह WTO के पास से मुक्त नहीं है। इसलिए वह विश्व के विकसित देशों के साथ मधुर व सौहार्दपूर्ण आर्थिक सम्बन्धों को प्राथमिकता देता है । भारत के आर्थिक विकास को चुनौती देने वाला एक प्रमुख तत्व सैनिक तत्व है।
भारत के आर्थिक विकास को चुनौती देने वाला एक प्रमुख तत्व सैनिक तत्व है। भारत को प्रतिवर्ष अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करना पड़ता है। इससे भारत का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। भारत ने रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों से कई सामरिक समझौते भी किए हैं। भारत द्वारा अस्त्र खरीदने का कार्यक्रम उसकी अर्थव्यवस्था को गम्भीर खतरा पैदा कर सकता है।
इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह युद्ध की सम्भावनाओं को रोके और भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व शान्ति के प्रयास करे । उसे विश्व के अन्य देशों से आर्थिक सहायता लेते समय भी सावधानी से कार्य करना चाहिए। इसलिए भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का भी सोच समझकर ही क्रियान्वयन करना चाहिए ताकि किसी आर्थिक शक्ति की नाराजगी मोल न लेनी पड़े। वैसे तो आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था में सुधारों की दिशा में कार्यरत है, लेकिन उसे आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यापारिक सम्बन्ध अधिक से अधिक देशों के साथ कायम करने चाहिए और साथ में ही उसे स्वयं को सामरिक दृष्टी से सुरक्षित भी बनाना चाहिए, यही भारत की विदेश नीति का ध्येय है।
वैचारिक तत्व (Ideological Factors) :- किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारण करने में विचारधारा का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत की विदेश नीति गांधीवादी विचारधारा पर आधारित रही है। भारत ने लोकतन्त्रीय समाजवाद को ही अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया है। इसलिए भारत की विदेश नीति सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की रही है।
नेहरु जी ने प्रजातन्त्र व साम्यवाद दोनों विचारधाराओं को अपनी विदेश नीति में जगह दी । अर्थात् नेहरु जी की विदेश नीति में उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ नेहरु जी ने अहिंसावाद की परम्परा को गांधी जी से ग्रहण करते हुए अपना पंचशील और शान्तिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धान्त भी पेश किया जो आज भी भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
आन्तरिक या घरेलु राजनीति (Internal Politics) :- किसी भी देश की घरेलु राजनीति व विदेश नीति में गहरा सम्बन्ध होता है। मीब्रेल ने कहा है- "विदेश नीति दूसरे माध्यमों से घरेलु नीतियों का ही विस्तार है ।" नेहरु जी की गुटनिरपेक्षता की सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रसंशा की गई है।
भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक-नौकरशाही, राजनीतिक दल, दबाव समूह व जनमत हैं। आज भारत की विदेश नीति का निर्माण एक स्वतन्त्र विदेश विभाग करता है जो सेना, नौकरशाही तथा राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर ही कोई निर्णय लेता है। कई बार देश की आंतरिक परिस्थितियां विदेश नीति काफी शिथिल हो जाती है। राजनीतिक दलों की विचारधारा, ढांचा तथा उनकी आन्तरिक कमजोरियां विदेश नीति को भी उल्ट रूप प्रदान कर देती हैं।
बहुदलीय प्रणाली की प्रकृति आम सहमति के बिना विदेश नीति के निर्माण में बाधक बन जाती है। यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सांझा सरकार का संचालन करते हुए भी एक सुदढ़ विदेश नीति का संचालन करते हुए भी एक सुदृढ़ विदेश नीति का संचालन किया। लेकिन ऐसा हमेशा सम्भव नहीं होता। इसी तरह व्यवसायिक दबाव समूहों की दबावकारी भूमिका भी आधुनिक समय में भारत की विदेश नीति को व्यापारिक हितों के अनुकूल चलने को बाध्य करती है । उदारीकरण के दौर ने तो दबाव समूहों की प्रभावकारी भूमिका को और अधिक सशक्त किया है।
अटल जी की विदेश नीति के अंतर्गत 21वीं सदी की शुरुआत में भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यूरोपियन संघ एवं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन व कई अन्य यूरोपियन देशों के साथ आर्थिक और सामाजिक तथा सामरिक समझौते हुए।
वर्तमान मनमोहन सरकार (2004) में विदेश नीति पर श्रमिक संघों का पूरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नजर आती है। आधुनिक युग में जनमत की उपेक्षा करना भी सरकार के लिए खतरे का सूचक है। किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में जनमत का ध्यान रखना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों व दबाव समूहों की प्रभावकारी भूमिका इस बात से आंकी जा सकती है कि जहां कुछ राजनीतिक दल अमेरिका के साथ सम्बन्धों को प्राथमिकता देते हैं तो कुछ सोवियत संघ के साथ। दक्षिणपंथी दलों व प्रगतिशील दबाव समूहों का झुकाव साम्यवाद की तरफ है। देश के मुस्लिम संगठन अरब देशों से सम्बन्ध कायम करने के पक्षधर हैं तो श्रमिक संगठन साम्यवादी देशों से। अतः किसी भी देश की विदेश नीति राजनीतिक व्यवस्था, दलगल राजनीति, सम्भ्रान्त वर्ग (Elite Class), दबाव समूहों आदि घरेलु तत्वों से भी प्रभावित होती है।
अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश (International Milieu ) :- किसी भी देश की विदेश नीति अपने चारों ओर विश्व में घट रही घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकती। उसे हर हालत में प्रत्येक घटना का गहराई से अवलोकन करके उसे स्वयं के साथ सम्बन्धित करना पड़ता है। यही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वास्तविकता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का उदय हुआ उसें शीतयुद्ध कहा जाता है। इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास करना भी सभी भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व देशों का प्राथमिक कर्तव्य बनता था। इसलिए विश्वशांति के आदर्श के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। भारत ने तीसरी दुनिया के नवोदित स्वतन्त्र देशों को एक मंच पर लाकर शीत युद्ध के तनाव पर अंकुश लगाने के प्रयास किए और गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनाया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों को भी भारत ने अपनी विदेश नीति में जगह दी। विश्व शान्ति का सिद्धान्त, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा, उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीति का विरोध आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं जो भारत की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण जगह बनाये हुए है। कोरिया संकट, स्वेज नहर संकट, कांगों विवाद, अरब-इजराइल संघर्ष आदि में भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को परीक्षण स्थल प्रदान किया है।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आज भी गुटनिरपेक्षता नए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में काम कर रही है। आज नई अन्तर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण ध्येय आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों पर वरीयता देना है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बढ़ती भूमिका का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति पर पड़ रहा है। इसी तरह क्षेत्रीय संगठनों की राजनीति भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। आज भारत 'SAFTA' को महत्व देता है ताकि दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर आपसी सम्बन्धों में मधुरता लाई जा सके और आर्थिक हितों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसलिए भारत SAARC, ASEAN तथा 'हिन्द महासागर रिम' जैसे क्षेत्रीय संगठनों की राजनीति के अनुरूप अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है।
निष्कर्ष
इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पर कुछ घरेलु तथा कुछ बाहरी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जहां घरेलु तत्वों के रूप में भूगोल, अर्थव्यवस्था, सैनिक तत्व, इतिहास, परम्पराएं, विचारधारा, व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यवस्था, हित व दबाव समूहों, नौकरशाही, जनमत आदि ने इसे प्रभावित किया है, वहीं बाहरी तत्वों के रूप में क्षेत्रीय संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा बदलते विश्व परिवेश ने भी इसे काफी प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति जितनी अधिक घरेलु वातावरण से प्रभावित हुई है, उतनी ही अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश से भी हुई है। सत्य तो यह है कि भारत ने घरेलु राजनीतिक प्रतिक्रिया के साथ-साथ विश्व समुदाय की राजनीति प्रतिक्रिया के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति को बनाया है। इसी कारण आज भारत की विदेश नीति सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों का पूरा सम्मान करती है।
0 Response