
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
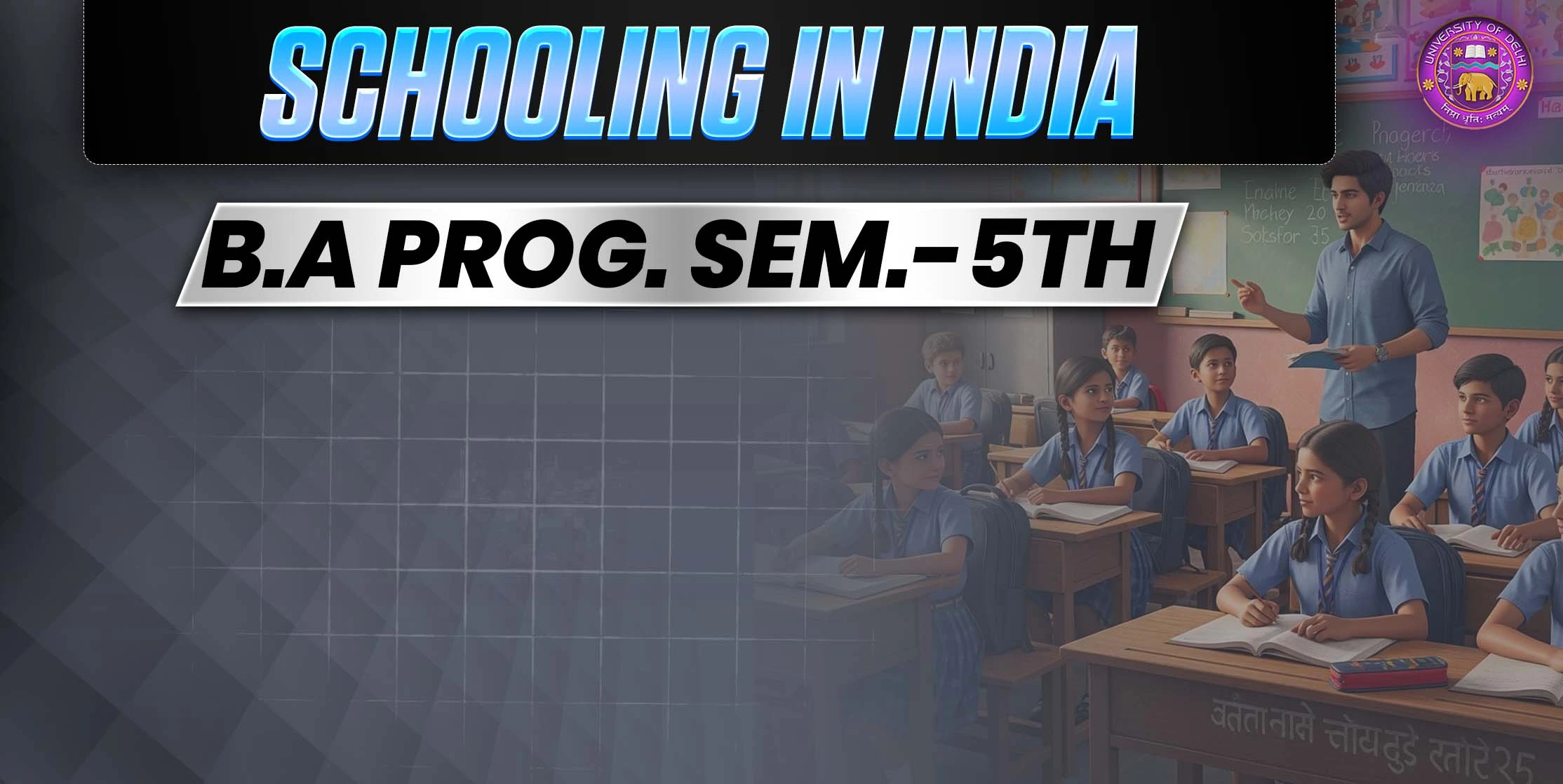
परिचय- उत्तर
वैदिक कालीन शिक्षा भारत के प्राचीनतम काल की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी, जिसका उद्देश्य नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना था। भारत में शिक्षा तथा विज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं हुई, बल्कि इसे धर्म के रास्ते पर चलकर मोक्ष पाने का एक व्यवस्थित प्रयास माना जाता था। मोक्ष को जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य माना जाता था। इस काल में शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग माना जाता था। शिक्षा का मुख्य आधार वेद थे, विशेष रूप से ऋग्वेद।
भारत की वैदिक कालीन शिक्षा

प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत की उथल-पुथल और विद्राह से दूर, प्रकृति की शांति में अपने गुरु के पास बैठकर जीवन की समस्याओं को सुनते, सोचते और समझते थे। उनका जीवन बहुत सरल और पवित्र होता था, जीवन उनके लिए प्रयोगशाला थी। वे केवल पुस्तकीय शब्द-ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि जन-समूह के सम्पर्क में आकर जगत व समाज काव्यावरहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे।
भारतीयों का विश्वास था कि सत्य का अनुभव केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी किया जाना चाहिए। इसलिए, प्राचीन भारतीय विद्यार्थी सत्य को समझने के लिए सीधे अनुभव करते थे और समाज का निर्माण उसी ज्ञान के आधार पर करते थे।
1. गुरु-गृह में विद्यार्थी का निवास : विद्यार्थी का गुरु-गृह में रहना और उनकी सेवा करना एक अनोखी भारतीय परंपरा थी। इससे विद्यार्थी गुरु के साथ लगातार संपर्क में आते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके अंदर गुरु के गुण विकसित होते थे। विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहने के दौरान न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि उनके जीवन के आदर्श, नैतिकता और सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी सीखते थे। इस प्रकार, गुरु के साथ विद्यार्थियों का निकट संपर्क उन्हें समाज की सभी परंपराओं से परिचित कराता था।
2. भिक्षान्न से जीवन-निर्वाह : भारतीय परंपरा में विद्यार्थियों का जीवन-निर्वाह और गुरु-सेवा के लिए भिक्षान्न प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। प्राचीन समय में भिक्षा लेना एक सम्मानित कार्य माना जाता था। शनपथ ब्राह्मण में इसे शिक्षा के रूप में माना गया है। यह प्रथा विद्यार्थी में त्याग तथा मानवीय गुणों का विकास करती थी। इससे विद्यार्थी का अहंकार और घमंड दूर होता था और वह असल जिंदगी के बारे में समझ पाता था। समाज के संपर्क में आकर उसे जीवन के असली पहलुओं का ज्ञान होता था। यह विद्यार्थी के लिए आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति उसके कर्तव्य और आभार का पाठ था।
भारतीय शिक्षा-प्रणाली की विशेषता
भारतीय शिक्षा-प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा जीवनोपयोगी थी। विद्यार्थी जब गुरु के आश्रम में रहते थे, तो उन्हें समाज से जुड़ने का मौका मिलता था। गुरु के लिए लकड़ी और पानी लाना, और अन्य काम करना उनके कर्तव्यों में आता था। इस तरह, वे न केवल गृहस्थ जीवन की शिक्षा लेते थे, बल्कि श्रम का सम्मान और सेवा का महत्व भी सीखते थे।
ऋग्वेद-कालीन शिक्षा
ऋग्वेद-युग में छोटे-छोटे पारिवारिक विद्यालय थे, जिनका संचालन शिक्षक स्वयं ही करता था। विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी गुरुगृह पर ही होती थी, जहाँ रहन-सहन और व्यवहार के नियम तय होते थे प्रारंभिक शिक्षा सभी ब्राह्मणों को दी जाती थी। उच्च शिक्षा केवल उन्ही को दी जाती थी जो इसके योग्य होते थे। जो विद्यार्थी इसके योग्य नही होते थे वे कृषि, उद्योग या व्यापार में भेज दिये जाते थे। उन्हें आध्यात्मिक जीवन जीने की अनुमति नहीं थी।
ऋग्वेद-कालीन शिक्षा की विशेषताएँ:
1. गुरु-गृह का महत्व : शिक्षा का केंद्र गुरु-गृह था, जहाँ विद्यार्थी उपनयन संस्कार के बाद गुरु के संरक्षण में जीवन-भर निवास करता था। शिक्षक, पिता के समान संरक्षक होते थे और विद्यार्थी के खान- पान की व्यवस्था स्वयं करते थे।
2. नैतिकता और सदाचार : गुरु-गृह में विद्यार्थी का प्रवेश केवल उसके नैतिक बल और सदाचार के आधार पर ही होता था। जो विद्यार्थी सदाचार में निम्न स्तर का माना जाता था, उसे आश्रम में रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी।
3. ब्रह्मचर्य का पालन: ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य था। हालांकि विवाहित युवक भी पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति नहीं थी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता था इंद्रियों पर नियंत्रण, शुद्धता और ब्रह्म में स्थिर रहना।
4. गुरु-सेवा का महत्व : विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य गुरु-सेवा माना जाता था। आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी हमेशा गुरु की सेवा के लिए तैयार रहता था। प्रायः उनके गृह-कार्य का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। वह मन, वाणी और कर्म से गुरु का भक्त होता था तथा गुरु को पिता या ईश्वर समझ कर उनकी
उपासना करता था।
5. अनुशासन और सदाचार का पालन: ऐसे विद्यार्थी जो गुरु-सेवा करने में असमर्थ थे या किसी अन्य प्रकार से सदाचार के प्रतिकूल अपना आचरण प्रदर्शित करते थे, उनके लिए विद्याध्ययन निषिद्ध था तथा उन्हें विद्यालय से निकाल दिया जाता था।
निष्कर्ष
वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित थी। गुरु- गृह में रहते हुए विद्यार्थी न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति अपना कर्तव्य भी समझते थे। यह प्रणाली जीवनोपयोगी और अनुशासनयुक्त थी, जो आत्मनिर्भरता और सेवाभाव को बढ़ावा देती थी।
0 Response