
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
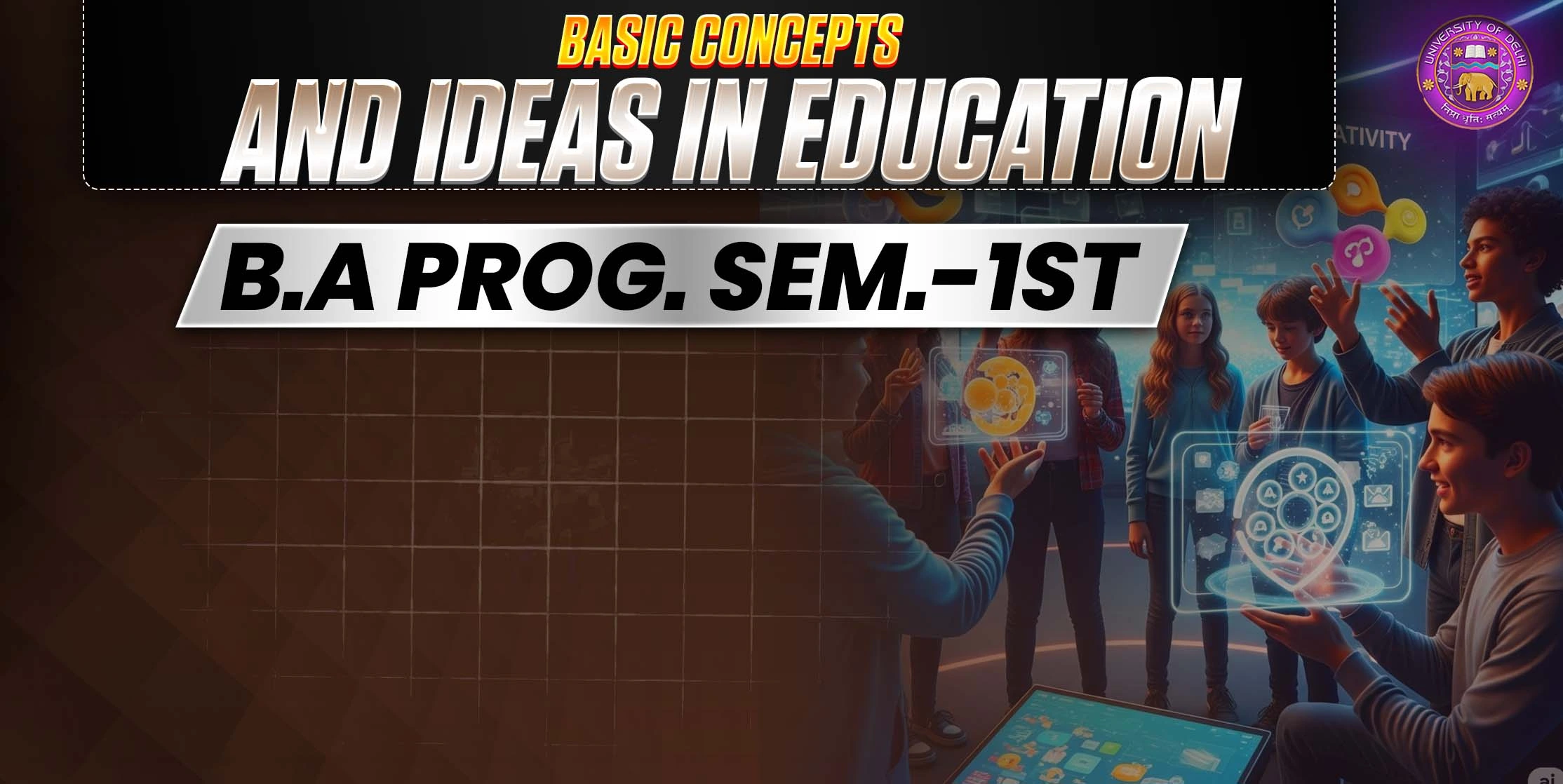
उत्तर - परिचय
शिक्षा के सन्दर्भ में वर्तमान समाज का स्वरूप सामान्यतः 'ज्ञान आधारित समाज' का है अथवा शिक्षा एवं दर्शन के सम्बन्ध में दोनों का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना एवं उसके जीवन का विकास करना है। यह वह आधार है जिस पर संपूर्ण शैक्षिक संरचना का निर्माण किया जाता है। ज्ञान शिक्षा के मूलभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है, वह आधार बनता है जिस पर सीखने, समझने और आलोचनात्मक सोच की पूरी प्रक्रिया निर्मित होती है।
ज्ञानमीमांसा का अर्थ -
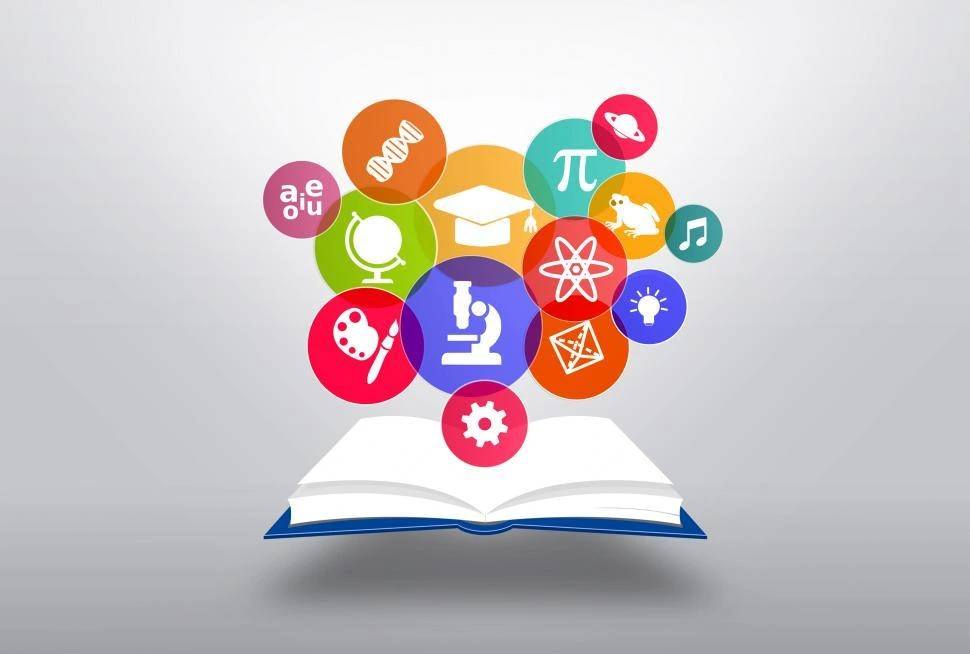
ज्ञानमीमांसा- ज्ञानमीमांसा दर्शनशास्त्र का एक क्षेत्र है, जो मानवीय ज्ञान से संबंधित है। यह एक प्रकार की दार्शनिक जाँच/पड़ताल का वह क्षेत्र है, जो ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, वैधता, ज्ञान की विधियाँ एवं सीमाओं की खोज करता है। ज्ञानमीमांसा (Epistemology) ग्रीक शब्द 'Episteme' अर्थात्, ज्ञान तथा 'LOGOS' अर्थात्, विज्ञान या परिचर्चा से आया है।
ज्ञान का अर्थ -
ज्ञान से आशय वास्तविकता के किसी पक्ष के प्रति जागरूकता तथा समझ से है जोकि सत्य विश्वास पर आधारित हो। यह स्पष्ट व सुबोध सूचना या तथ्य है जोकि तार्किक प्रक्रिया के अनुप्रयोग के द्वारा वास्तविकता से प्राप्त किया जाता है।
शिक्षा के ज्ञानात्मक/ज्ञानमीमांसीय आधार के रूप में ज्ञान का महत्व :
ज्ञानमीमांसा दर्शन का एक क्षेत्र है जो मानव ज्ञान से संबंधित है। यह दार्शनिक जाँच/पड़ताल का वह क्षेत्र है, जो ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, वैधता, ज्ञान की विधियाँ एवं सीमाओं की खोज करता है। यह खोज प्रायः इस तथ्य से संबंधित है कि ज्ञानमीमांसा वास्तव में दर्शनशास्त्र की एक शाखा है, जिसने ज्ञान के विस्फोट के कारण विचारकों का ध्यान आकर्षित किया है।
निष्कर्ष
ज्ञानमीमांसा वह आधारशिला बनाती है जिस पर शैक्षिक प्रणालियाँ निर्मित की जाती हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने, व्यवस्थित करने और संचारित करने के तरीके का मार्गदर्शन करती हैं। ज्ञानमीमांसा, ज्ञान के अपने दार्शनिक अन्वेषण के माध्यम से, न केवल हमारी समझ को आकार देती है बल्कि शैक्षिक प्रयासों के सार को भी प्रभावित करती है।
0 Response