
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
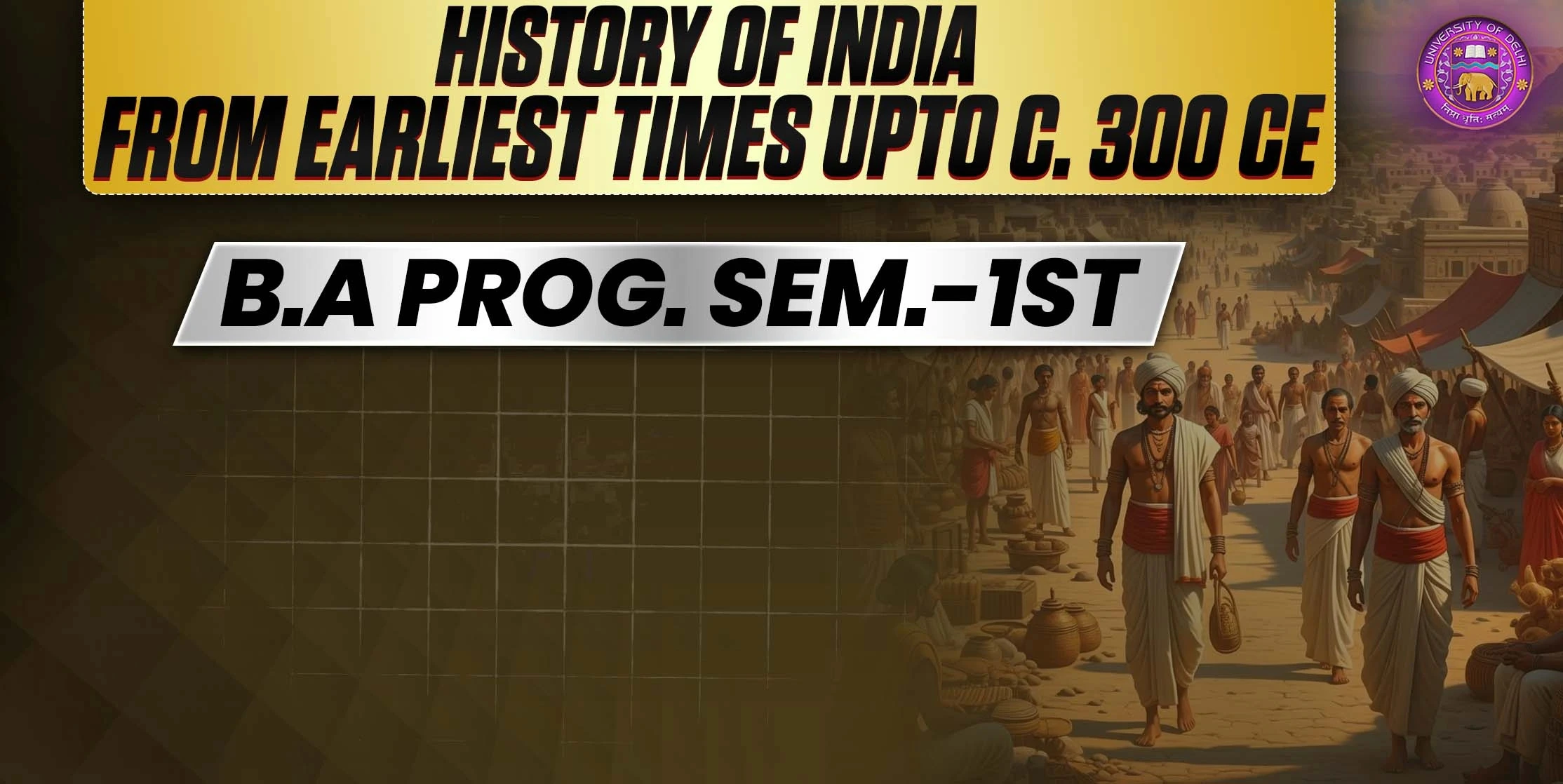
उत्तर - परिचय
प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और इसके इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन स्रोतों से हम जान पाते हैं कि मानव-समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया? यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, धातुकर्म आदि की शुरूआत कैसे की, कैसे जानवरों की स्फाई की, और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अन्ततः राज्यों की स्थापना की।
भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का महत्त्व :
साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन हमें भारतीय इतिहास के बेहतर अध्ययन और समझने में मदद करता है। इन स्रोतों का संयोजन हमारी सोच को विस्तृत करता है और हमें उस समय की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, और आर्थिक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है।
साहित्यिक स्रोत
साहित्यिक स्रोत, वे स्रोत है, जो साहित्य अर्थात् पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। यह साहित्य धार्मिक, लौकिक एवं विदेशी लेखकों के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-
(1) धार्मिक साहित्य तथा (2) ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य।
1. धार्मिक साहित्य -
प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य से हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है।
धार्मिक ग्रन्थ
ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक साहित्य प्रमुख है। वैदिक साहित्य भारतीय विद्वानों की अद्भुत सृजनशीलता का परिचायक है। वैदिक साहित्य का सृजन लगभग 1500 - 200 ई० पू० के मध्य किया गया। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक और सूत्र साहित्य आता हैं।
बौद्ध धर्म-ग्रन्थ -
बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। बौद्ध साहित्य से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएँ है-
जैन ग्रन्थ - जैन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैन साहित्य से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम साहित्य का स्थान सर्वोपरि है, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंदसूत्र, नन्दिसूत्र, अनुयोगद्वार और मूल-सूत्र सम्मिलित हैं।
2. ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रन्थ
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में लौकिक, समसामयिक तथा ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ प्रचूर मात्रा में स्रोत सामग्री उपलब्ध कराते है। ये ग्रंथ तत्कालीन जन-जीवन, भौतिक संस्कृति, प्रशासन एवं राजनीति पर व्यापक जानकारी देते है।
पुरातात्विक स्रोत
पुरातत्व उन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, जिनका निर्माण और उपयोग मनुष्य ने किया है। अतः वे समस्त भौतिक वस्तुएँ जो अतीत में मनुष्य द्वारा निर्मित एवं उपयोग की गयी है, वे सभी वस्तुएँ पुरातत्व के अंतर्गत आती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाती है।
पुरातात्विक स्रोत सामग्री को 6 भागों में बाँटा जा सकता है-
(1) अभिलेख, (2) सिक्के अथवा मुद्राएँ, (3) स्मारक, (4) मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि।

निष्कर्ष
भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का महत्त्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्रोत विभिन्न कालों में हुई घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों और संस्कृति के विकास को समझने में मदद करते हैं। इन स्रोतों का विशेष महत्त्व इसलिए है क्योंकि वे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की मूल अवधारणा को समझने में मदद करते है
0 Response