
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
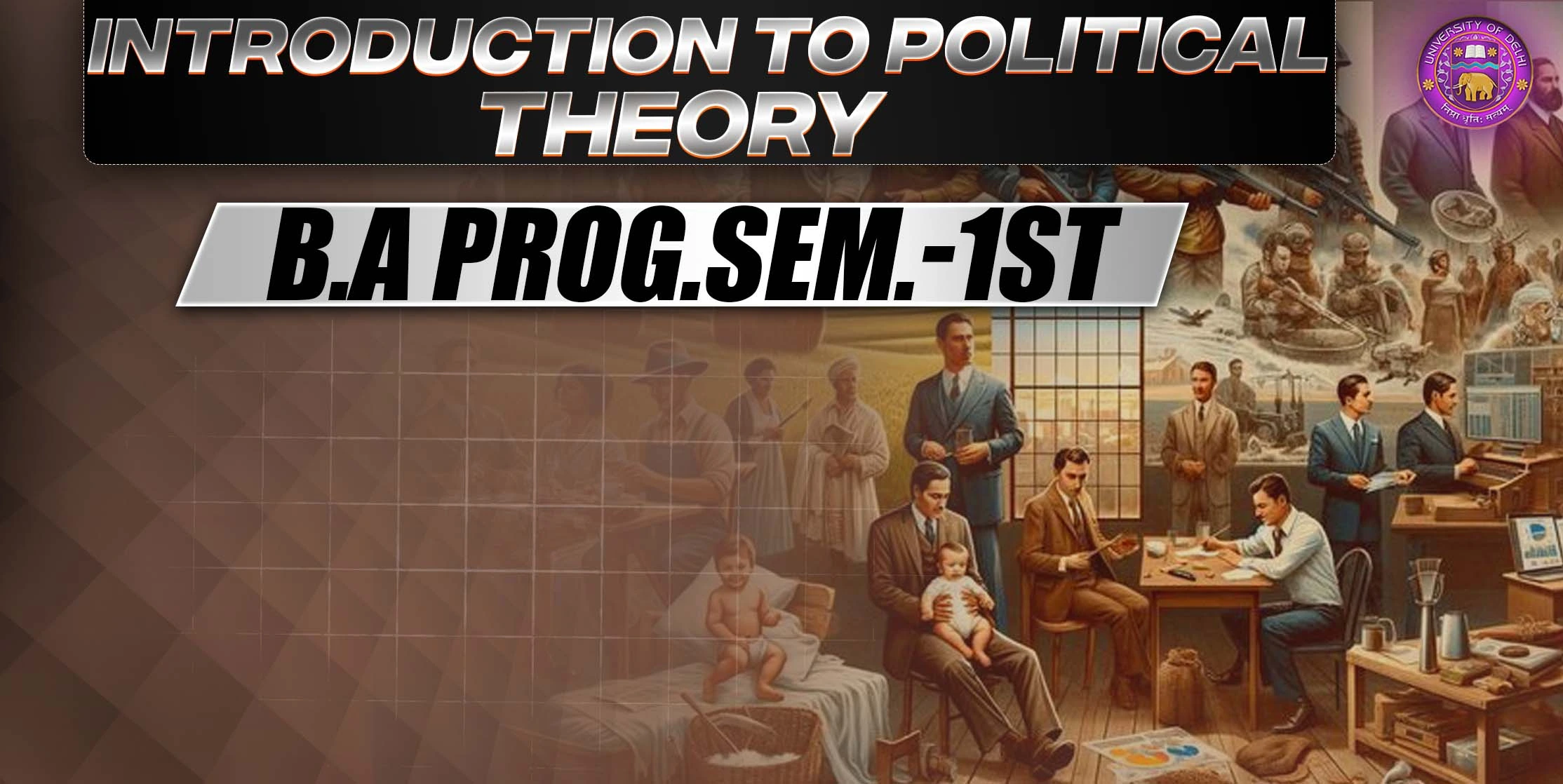
अथवा
राजनीतिक सिद्धान्त की प्रासंगिकता विवेचना कीजिए।
उत्तर- परिचय
राजनीति-शास्त्र एक प्राचीन और समकालीन विषय है, जिसकी जड़ें प्लेटो और अरस्तू जैसे महान विचारकों तक फैली हैं। यह विषय निरंतर नई सामग्री और नवीन दृष्टिकोणों को समाहित करता रहा है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और महत्व समय के साथ बढ़ता गया है। 'राजनीतिक सिद्धांत' दो शब्दों से मिलकर बना है: राजनीतिक और 'सिद्धांत' । राजनीतिक' शब्द ग्रीक भाषा के 'पोलिस' से लिया गया है, जिसका अर्थ नगर-राज्य होता है। 'सिद्धांत' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक 'थ्योरिया' से हुई है, जिसका अर्थ चिंतन और मनन की अवस्था है।
राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ
राजनीतिक सिद्धांत राज्य, सरकार और समाज से जुड़े विचारों और संस्थानों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है, उनके प्रभाव को समझता है, और आदर्श राज्य व समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है। राजनीतिक सिद्धांत का सम्बन्ध राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों से है, और इसकी महत्वता इसलिए है क्योंकि यह नीति निर्माण तथा शासन को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाता है।
राजनीतिक सिद्धांत पर विभिन्न विचारकों के विचार :
एंड्रयू हैकर के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है, तो दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी का मिश्रण है।"
डेविड हेल्ड के अनुसार: "राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक जीवन से सम्बंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना-बाना है, जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है।"
राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति:
राजनीतिक सिद्धांत समय और युग की परिस्थितियों के अनुसार बदलता और विकसित होता रहा है। इस विकास में अनेक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान रहा, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों कानिर्माण किया। राजनीतिक सिद्धांत ने विकास के क्रम में तीन प्रमुख रूप धारण किए हैं :-
1. परम्परागत राजनीतिक सिद्धांत :
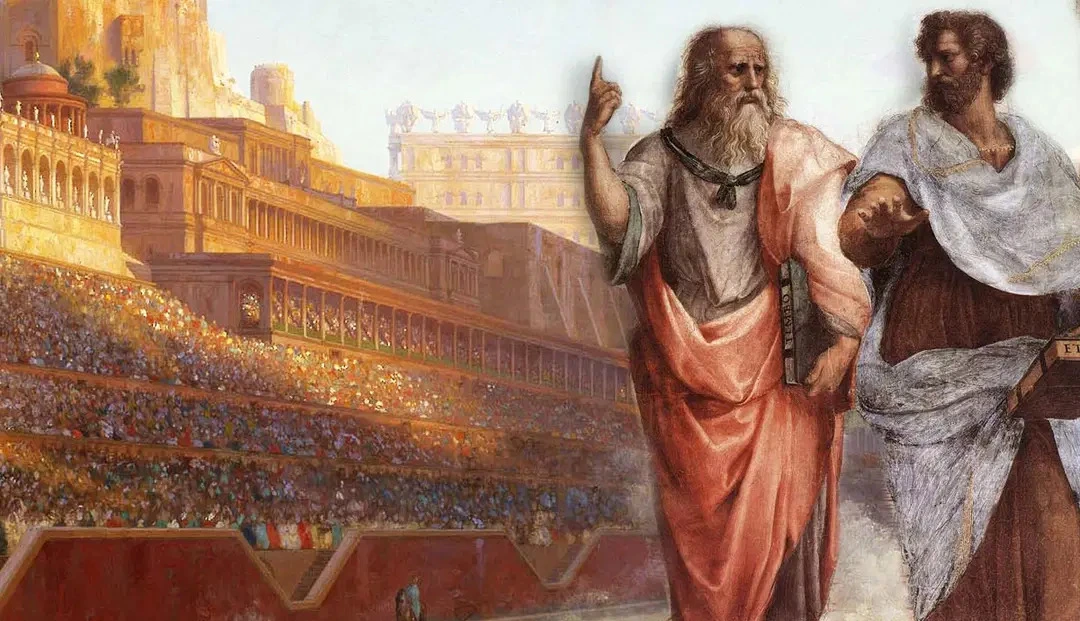
परम्परागत जिसे आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत उन आदर्श विचारों और कल्पनाओं पर आधारित है जो एक आदर्श राज्य या शासन व्यवस्था की संरचना करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, प्लेटो ने "दार्शनिक राजाओं" (Philosopher Kings) की परिकल्पना की और उसके आधार पर एक आदर्श राज्य का ढांचा प्रस्तुत किया।
प्लेटो की "दार्शनिक राजाओं की अवधारणा उनके ग्रंथ " द रिपब्लिक" में प्रस्तुत आदर्श राज्य का आधार है। ये शासक ज्ञान, तर्क, न्याय, और नैतिकता में निपुण होते हैं। वे निजी स्वार्थ से मुक्त होकर सत्य, समानता, और सामाजिक न्याय स्थापित करते हैं।
2. आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत :
3. समकालीन राजनीतिक सिद्धांत :
राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और प्रासंगिकता
1. राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की समझ : राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों को समझने में मदद करता है। यह विभिन्न राजनीतिक ढांचे, जैसे लोकतंत्र, तानाशाही, और संघीय प्रणाली के कामकाज को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
2. समाज के मूल्यों का संरक्षण : राजनीतिक सिद्धांत समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों जैसे मूल्यों को संरक्षित करने के लिए दिशा प्रदान करता है। और हमें यह समझने में मदद करता है कि भविष्य में कैसे इन मूल्यों को लागू किया जा सकता है।
3. राजनीतिक निर्णयों में मार्गदर्शन : राजनीतिक सिद्धांत नीतियों और निर्णयों को समझने में सहायक होता है। यह राजनीतिक विचारकों को यह सुझाव देता है कि राजनीतिक फैसलों के पीछे की तर्कशक्ति और उनके सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, जिससे अच्छे शासन की दिशा में मदद मिलती है।
4. वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग : समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, जैसे 'ब्रायन बेरी' और 'जॉन रॉल्स' के विचारों के अनुसार, राजनीतिक घटनाओं और सिद्धांतों को समझने के लिए वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांतों को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाता है।
5. सामाजिक समस्याओं का समाधान : राजनीतिक सिद्धांत समाज में मौजूद विभिन्न समस्याओं जैसे असमानता, संघर्ष, और अन्याय के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सिद्धांत समाज के लिए न्यायपूर्ण और स्थिर समाधान प्रस्तुत करने में सहायक है।
निष्कर्ष
राजनीतिक सिद्धांत का विकास निरंतर जारी है। नवमार्क्सवाद, सामुदायिकतावाद, और अस्तित्ववाद जैसे नए विचार इसकी प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं। यह समाज, सरकार और संविधान को दिशा प्रदान करता है, साथ ही स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या भी करता है।साथ ही यह वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को समझने में सहायक है, जिससे नीति निर्माण और शासन को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाया जा सके।
0 Response