
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
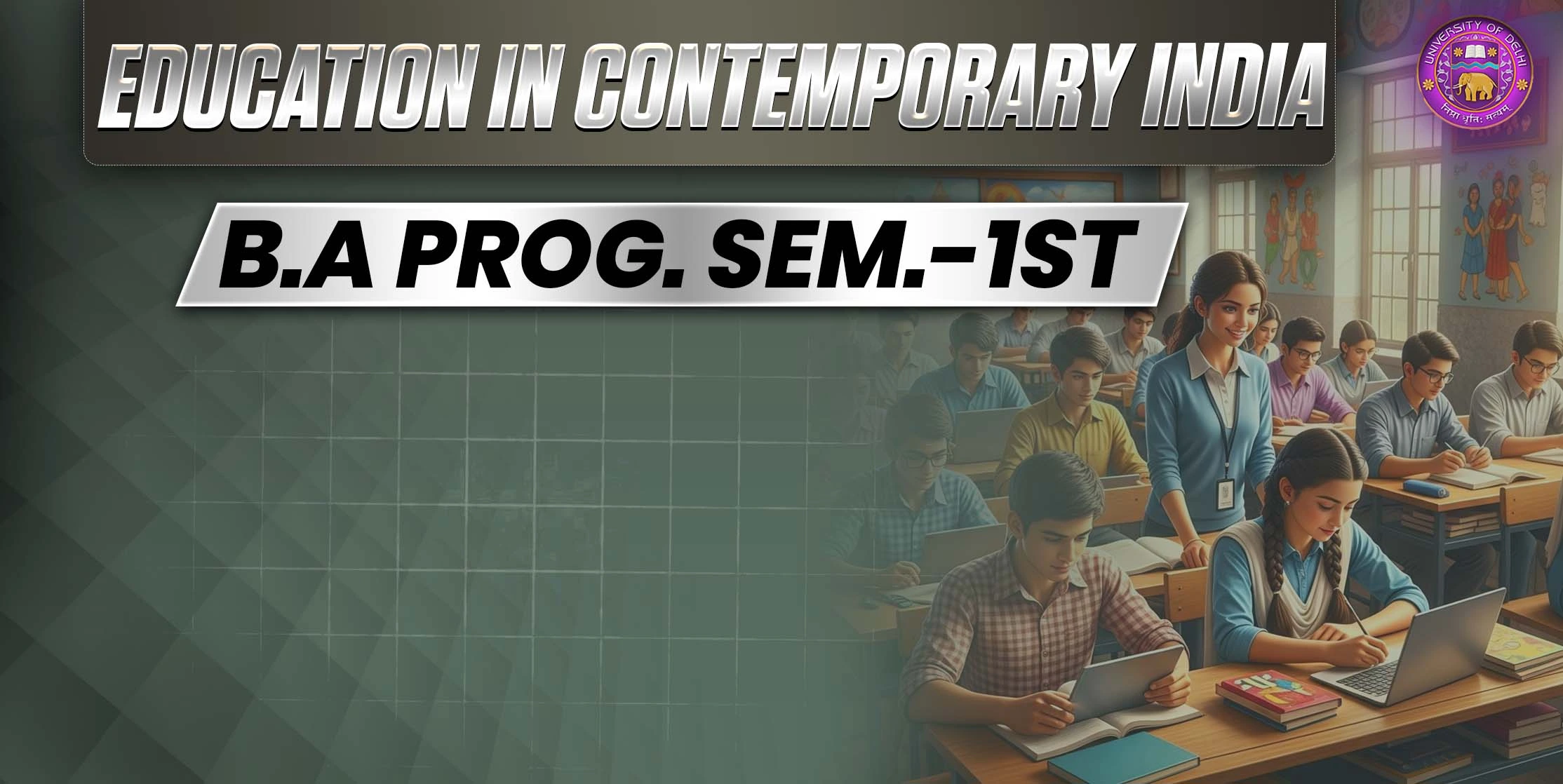
उत्तर - परिचय
देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE) लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट के इस प्रवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया, जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसी खामियां व चुनौतियां हैं, जिसके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएँ

1. निःशुल्क शिक्षा
'नि: शुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि एक बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा, जिसे उसके माता-पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला दिया है, जो उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी प्रकार के शुल्क या शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अनिवार्य शिक्षा
6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और प्रवेश, उपस्थिति ओट प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर एक दायित्व डालता है। इसके साथ, भारत एक अधिकार आधारित ढांचे की ओर बढ़ गया है, जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निहित इस मौलिक बाल अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी दायित्व डालता है।
2. अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार -
यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारणवश कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान होगा।
3. राज्य सरकारों और स्थानीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य -
इस अधिनियम के लागू होने के 3 सालों के भीतर राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को पड़ोस के स्कूलों को स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में एक स्कूल नहीं है वहाँ स्कूलों को बनाना होगा।
4. वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना -
केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों की एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और साधन उपलब्ध कराएगी जिससे विद्यालय स्थापित किए जा सकेंगे हैं।
5. राज्य सरकारों के कर्तव्य -
राज्य सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति निश्चित करेगी। साथ ही यह भी वह सुनिश्चित करेगी, कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके। राज्य सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता निश्चित करेंगी और बच्चों को उन्नत किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराएगी ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके।
6.स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य -
स्थानीय पदाधिकारी उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार समस्त कर्तव्यों के साथ-साथ अपने क्षेत्र में बालकों का अभिलेख करेगी विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित होगी और शैक्षिक कैलेंडर तैयार होंगे।
7. माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य -
प्रत्येक अभिभावक और माता-पिता का यह उत्तरदायित्व कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए जरूर भेजें।
RTE Act 2009 के उद्देश्य
1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य यह है की 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएँ ताकि जिन बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ नहीं पाते तो उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए।
2. अगर कोई भी व्यक्ति या फिर विद्यालय RTE Act 2009 का पालन न करके उस बच्चे से फीस की मांग करता है तो उस विद्यालय को उस विद्यालय की फीस का 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा और केवल यह ही नहीं सरकार द्वारा उस विद्यालय की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है।
3. अगर सर्कार द्वारा किसी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाती है लेकिन अगर उस विद्यालय को उसके बाद भी चलाया गया तो उस विद्यालय को 1 लाख रुपये और 10 हजार रुपये प्रतिदिन का भुगतान करना होगा।
4. अगर कोई बच्चा विकलांग है तो RTE Act 2009 के तहत उन् बच्चों के लिए सीमित आयु को 14 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी यानि के उन बच्चों को केंद्र सरकार के द्वारा ही मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है।
6. RTE Act 2009 के अनुसार कोई विद्यालय अगर बच्चे का या फिर उसके माता पिता का इंटरव्यू लेते है तब उस विद्यालय से 25 हजार रुपये सरकार के द्वारा जुर्माने के रूप में वसूल किया जायेंगे।
7. अगर वह चीज को दोबारा दोहराते हैं तब जुर्माने की राशि 25000 से बढाकर 50 हजार कर दी जायेगी।
8. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय का कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते।
9. यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों पर होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ है और वह इसको रोकता भी है।
10. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के के द्वारा बच्चों के लिए केंद्रित शिक्षा प्रणाली की भी शुरुआत की गयी है।
आरटीई कार्यान्वयन के लिए प्रमुख चुनौतियां
वित्तीय आवंटन का अभाव- करीब दो दशक से प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा के लिए देश के आम बजट में कम से कम 6% आवंटित करने की मांग की जा रही है, लेकिन यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है।
सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के प्रति उदासीनता- आज के समय में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के प्रति उदासीनता की शिकार हो गई है। देश के अंदर मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना स्टेटस सिंबल समझते हैं। इनके बीच सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना उनके गरिमा खिलाफ है। पब्लिक स्कूल प्रणाली को जब सामान्य सामुदायिक संसाधनों के रूप में देखा जाने लगेगा, तो इसमें काफी सुधार होगा।
सामूहिक प्रयास का अभाव- इस एक्ट की मांग है कि कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज भी हम अपने आसपास अनेक मासूम बच्चों को चाय की दुकान पर खाली कप उठाते और ढाबे पर बर्तन साफ करते देख सकते हैं। सरकार का प्रयास इस कानून के माध्यम से इन मासूमों को स्कूल की राह दिखाना है। लेकिन न तो अकेली सरकार और न ही अभिभावक इस प्रयास को परवान चढ़ा सकते हैं, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही शिक्षा के अधिकार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी कई नियमों की तरह यह कानून भी कागजों में सिमट कर रह जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी।
निष्कर्ष
शिक्षा के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है।
0 Response