
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
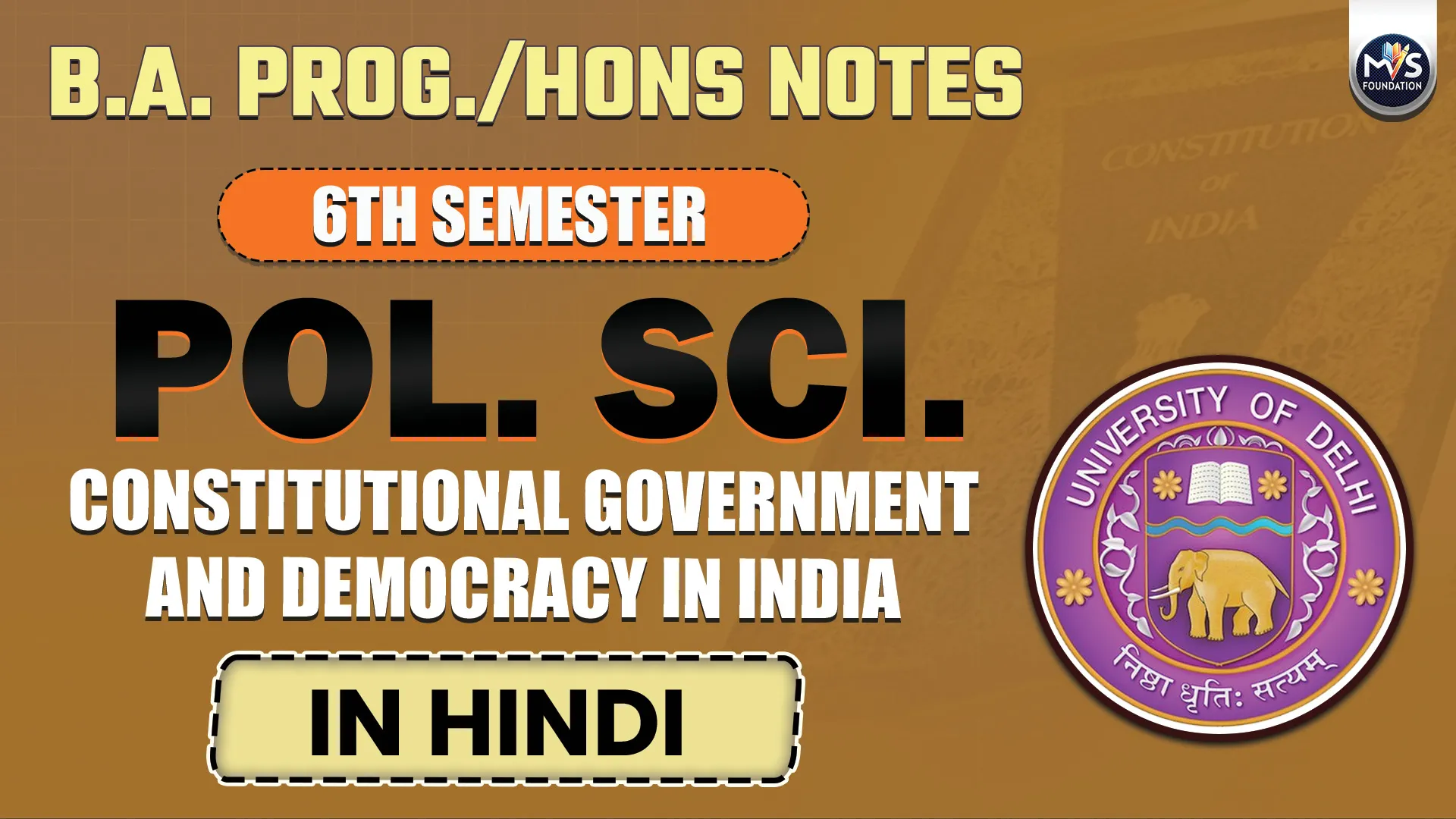
प्रश्न 1 भारतीय संविधान की विषेशताओं का विवेचन कीजिए। प्रस्तावना किस सीमा तक इन विषेशताओं का प्रतिनिधित्व करती है ?
अथवा
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं और दर्शन पर विवेचना कीजिए ?
उत्तर -
परिचय
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे कई देशों के अनुभवों और मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह केवल शासन की व्यवस्था नहीं बताता, बल्कि समाज और राजनीति के विचारों को भी दर्शाता है। इसकी प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है, जो इसके मूल आदर्शों और विशेषताओं का सार प्रस्तुत करती है।
भारतीय संविधान पर कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ :
1. समानता की धारणा भारतीय संविधान केवल कानून के समक्ष समानता की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी महत्व देता है। यह कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। विचारक नुसबौम और जोया हसन मानती हैं कि ये प्रावधान समाज में वास्तविक समानता लाने के महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
2. विशेष प्रावधान - संविधान समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ, वृद्ध, और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विशेष प्रावधान करता है। रोड्रिक्स के अनुसार, ये प्रावधान समानता को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम हैं।
3. अल्पसंख्यक अधिकार - भारतीय संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रख सकें। इसका उद्देश्य भारत की विविधता को सुरक्षित रखना है।। यह अधिकार उन्हें अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने और प्रशासन में भागीदारी का अवसर भी देता है। इससे अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना और राष्ट्र के प्रति समरसता बढ़ती है।
4. मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार - संविधान द्वारा दिए गए वे अधिकार हैं जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार, कोई भी ऐसा कानून जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो, अमान्य होगा। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था नागरिकों के इन अधिकारों का हनन न कर सके। इसके साथ ही, संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए।
5. नीति निदेशक तत्व (अनु. 36-51) - संविधान के अनुच्छेद 38 से 47 तक नीति निदेशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, पोषण और लैंगिक समानता जैसे उद्देश्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हें ऑस्टिन ने "क्रांति के उपकरण" कहा है। ये तत्व गैर-न्यायिक होते हुए भी नीति निर्माण की दिशा तय करते हैं।
6. संघीय ढाँचा - भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से करता है - केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची के तहत कुछ राज्यों जैसे नागालैंड और मिजोरम को खास अधिकार दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में एक जैसा नहीं, बल्कि राज्यों की ज़रूरतों के अनुसार संघीय ढाँचा है।
प्रस्तावना द्वारा इन विषेशताओं का प्रतिनिधित्व :
संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा मानी जाती है। यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्शों को सामने रखती है। ये आदर्श संविधान की सभी विशेषताओं जैसे - समानता, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, विशेष प्रावधान, और संघीय ढाँचे को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान की सभी मूल विशेषताओं का संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करती है।
भारतीय संविधान का दर्शन :
1. राजीव भार्गव का दृष्टिकोण सामाजिक प्रभुत्व को तोड़ने वाला संविधान
कमल कुमार मानते हैं कि संविधान केवल शासन का ढांचा नहीं था, बल्कि वह लिंग, जाति और धर्म के आधार पर होने वाले अन्यायों को समाप्त करने की उम्मीद से जुड़ा था। सामाजिक न्याय से जुड़े अनुच्छेद जैसे 15 (3) और 15(4) राज्य को सशक्त बनाते हैं ताकि वह कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण दे सके और समान अवसर सुनिश्चित कर सके। विशेषकर वंचित और दलित वर्गों के लिए यह आशा और परिवर्तन का प्रतीक बना।
2. एस. एन. अग्रवाल और ऑस्टिन का दृष्टिकोण गांधीवादी बनाम पश्चिमी सोच
संविधान सभा के सदस्य एस. एन. अग्रवाल गांधीवादी सोच के समर्थक थे। वे चाहते थे कि राज्य की भूमिका कम हो और नागरिक स्वयं समाज सुधार में आगे आएँ। दूसरी ओर, ऑस्टिन के अनुसार, संविधान सभा ने पश्चिमी परंपराओं को अपनाया, जिसमें राज्य की मजबूत भूमिका को महत्व दिया गया ताकि सामाजिक क्रांति और गहन परिवर्तन लाया जा सके। यह दृष्टिकोण संविधान को सक्रिय परिवर्तनकारी दस्तावेज के रूप में देखता है।
3. एस. के. चौबे का दृष्टिकोण सीमित सामाजिक क्रांति का संविधान -
एस. के. चौबे के अनुसार, भारतीय संविधान में सामाजिक क्रांति की जो क्षमता थी, वह संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कमजोर कर दी गई। वे मानते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य यूरोप में 1848 तक प्राप्त हो चुके थे, इसलिए भारतीय संविधान की सामाजिक क्रांति नवीन नहीं थी। कई महत्वपूर्ण प्रावधान जो गहरी सामाजिक क्रांति ला सकते थे, वे संविधान बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही पराजित हो गए।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की विशेषताएँ इसे विश्व में अनोखा बनाती हैं। इसकी प्रस्तावना संविधान के मूल मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्रभावी रूप से दर्शाती है, यह संविधान केवल शासन का ढाँचा नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और समावेशी समाज की परिकल्पना है, जो आज वर्तमान के संदर्भ में भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है।
0 Response