
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
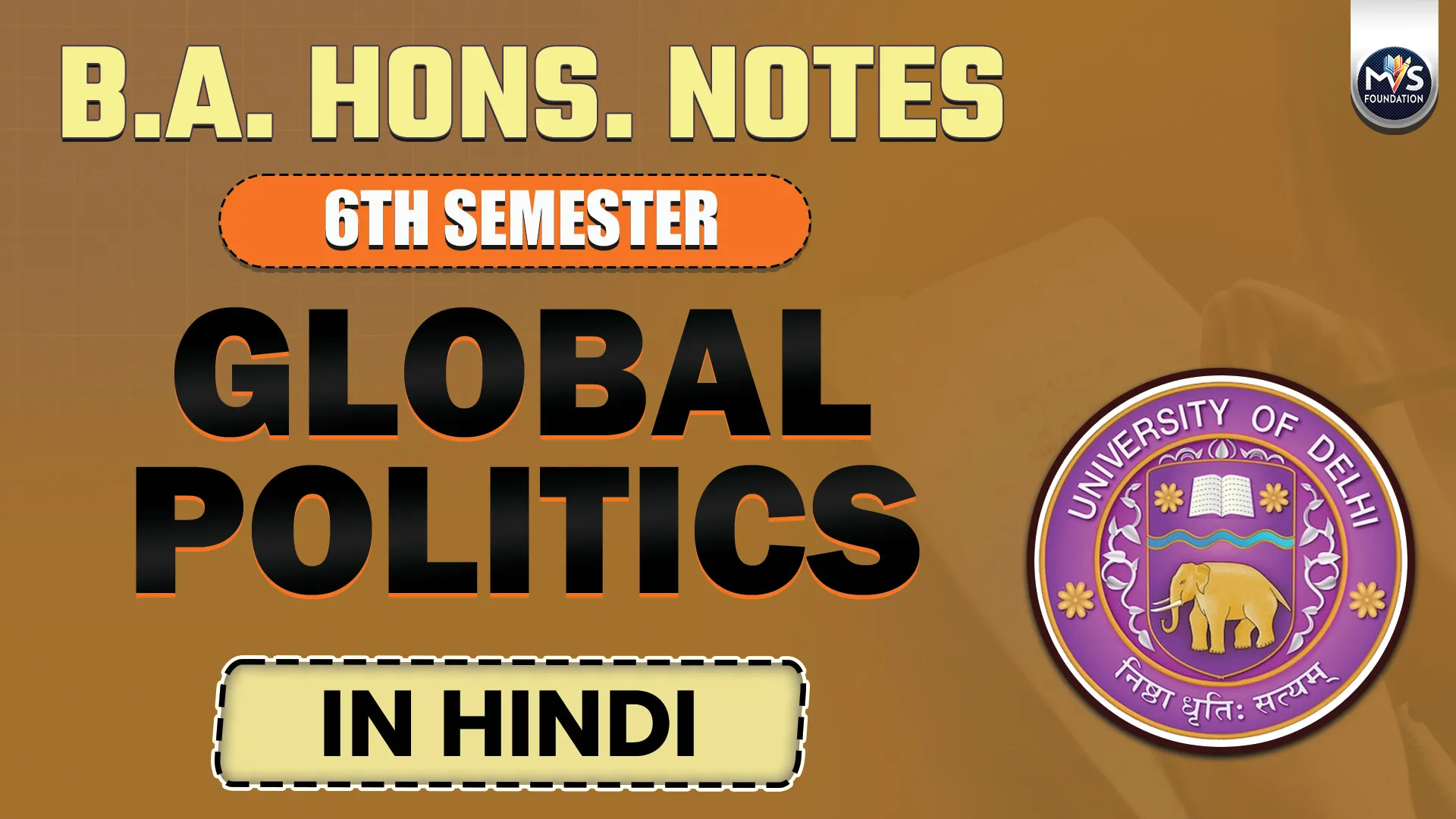
प्रश्न 1 - वैश्वीकरण में पूर्वी बनाम पश्चिमी सभ्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
उत्तर -
परिचय
वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशों, संस्थाओं और लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ता है। वैश्वीकरण के चलते ही पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच अनेक समानताएं और अंतर उभरे हैं। इस प्रक्रिया में, पश्चिमीकरण का प्रभाव अधिक देखा गया है। हालांकि, पूर्वी सभ्यताओं ने भी अपनी सांस्कृतिक को बचाते हुए वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगम ने दोनों सभ्यताओं के मध्य संवाद और संघर्ष दोनों को उत्पन्न किया है।
पश्चिमी सभ्यता :
पश्चिमी सभ्यता मुख्यतः यूरोप और उत्तर अमेरिका से संबंधित है। इसके प्रमुख लक्षणों में वैज्ञानिक सोच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शामिल हैं। पश्चिमी सभ्यता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके अलावा, पश्चिमी सभ्यता में मानव अधिकारों, कानून के शासन, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया जाता है।
पूर्वी सभ्यता :
पूर्वी सभ्यता मुख्यतः एशिया, विशेष रूप से चीन, जापान, भारत, और अन्य एशियाई देशों से संबंधित है। इसके प्रमुख लक्षणों में आध्यात्मिकता, सामूहिकता और पारंपरिक पर जोर शामिल हैं। पूर्वी सभ्यता ने योग, ध्यान, आयुर्वेद, और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, इसमें सांस्कृतिक परंपराओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
यूरोकेंद्रित और गैर-यूरोकेंद्रित विचारधारा :
यूरोकेंद्रित विचारधारा
यूरोकेंद्रित विचारधारा का मानना है कि पश्चिमी सभ्यता की जड़े प्राचीन यूनान और रोमन सभ्यताओं में निहित हैं। इस विचारधारा के अनुसार, पुनर्जागरण और सुधार काल (15वीं-16वीं सदी) ने यूरोपवासियों के लिए साहित्य, विज्ञान, अन्वेषण और यात्रा के नए युग का आरंभ किया, जिससे पश्चिमी दुनिया में ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति, और पूँजीवाद का विकास हुआ।
1. कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण:
2. प्रगतिशील मूल्य
यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार, पश्चिमी समाज को प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि वह नवाचारी और विकासशील मुद्दों को ध्यान में रखता है। इसमें विज्ञान, तकनीक, और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी देशों की उपलब्धियों को महत्व दिया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उनकी प्रगतिशीलता उन्हें आधुनिक तकनीक के लिए विख्यात बनाती है, जो समाज में सुधार लाती है।
3. विवेकशीलता :
यह दृष्टिकोण पश्चिमी समाज को तर्कसंगत, वैज्ञानिक सोच और विवेकशीलता का प्रतीक मानता है। इसमें यह माना जाता है कि पश्चिम ने ज्ञान, शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से दुनिया को प्रगति की राह पर अग्रसर किया है।
4. सभ्यता और स्वतंत्रता :
यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण में पश्चिमी समाज को सभ्य, सुसंस्कृत और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला माना जाता है। लोकतंत्र, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पश्चिमी समाज की विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
गैर-यूरोकेंद्रित विचारधाराः
गैर-यूरोकेंद्रित विचारधारा यूरोकेंद्रितता की आलोचना करते हुए विविध संस्कृतियों, परंपराओं और सभ्यताओं को समान महत्व और सम्मान देती है। यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक विविधता और बहुलता को महत्व देता है और पश्चिम के बाहर की संस्कृतियों और समाजों को भी मानव इतिहास और विकास का अभिन्न हिस्सा मानता है।
1. असभ्य और निरंकुशता का खंडनः
गैर-यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि पश्चिमी विचारधारा द्वारा अन्य संस्कृतियों को असभ्य या निरंकुश के रूप में चित्रित करना अनुचित और भटकाने वाला है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि हर संस्कृति की अपनी विशिष्टता और मूल्य हैं।
2. सांस्कृतिक विविधताः
इस दृष्टिकोण में, संस्कृतिक विविधता को महत्व दिया जाता है। जिसके अंतर्गत, विभिन्न संस्कृतियों के अद्वितीय धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं को समझा जाता है। इसे न केवल समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह संसार की सांस्कृतिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है।
3. अविवेकशीलता का खंडन:
गैर-यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण यह मानता है कि विवेकशीलता और तर्कसंगतता केवल पश्चिम की विशेषता नहीं है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में भी विज्ञान, तर्क और ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिससे उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को महत्व मिला है।
4. स्थिर अर्थव्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन:
यह विचारधारा पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर और शक्तिहीन मानने के बजाय उनके ऐतिहासिक योगदान और आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण कर ती है। इसमें विभिन्न आर्थिक मॉडल और प्रथाओं की विविधता को समझने का प्रयास किया जाता है।
आलोचनात्मक मूल्यांकन:
यूरोकेंद्रित तर्क/ विचारधारा गलत है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहास बताता है कि विश्व की विकास की कहानी में पूर्व का प्रमुख योगदान रहा है, जबकि पश्चिमी शक्तियाँ पहले एशिया के मुकाबले कमजोर थीं। कई खोजें आविष्कार और क्रांतियाँ, जिन पर पश्चिमी देश दावा करते हैं, पहले ही पूर्व में हो चुकी थीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि पूर्व ने ही विश्व की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाई है।
1. जेफ्री गुन का तर्क
जैफ्री गुन ने दक्षिणपूर्वी एशिया और यूरोप के बीच संबंधों को प्रथम वैश्वीकरण के रूप में उजागर किया। उन्होंने यह प्रारंभिक वैश्वीकरण को उदाहरण देकर दिखाया कि यूरोकेंद्रित दृष्टिकोण ने इसे हमेशा अनदेखा किया है। उदाहरण के लिए, चीन और भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी महत्त्वपूर्ण और प्रभुत्वकारी भूमिका अदा की जिससे सत्रहवीं शताब्दी से पूर्व एशियाई नेतृत्य का पता चलता है।
2. हॉब्सन का विरोध
हॉब्सन ने मार्क्स की विचारधारा की आलोचना की और कहा कि पश्चिमी विकास में पूर्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके अनुसार, यदि पूर्व की सहायता न होती, तो पश्चिम आधुनिकता को प्राप्त नहीं कर पाता। हॉब्सन ने पश्चिम के पक्षपातपूर्ण और संकीर्ण दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे वैज्ञानिक और निष्पक्ष नहीं माना।
3. जेम्स ब्लॉट की आलोचना:
जेम्स ब्लॉट ने भी पश्चिम की सर्वोच्चता के विचार को चुनौती दी और यूरोपवासियों को 'इतिहास के निर्माता' कहे जाने के विचार की आलोचना की। उन्होंने इसे 'यूरोकेंद्रित सुरंग इतिहास' कहा, क्योंकि इस दृष्टिकोण में निष्पक्षता का अभाव था।
एक अंग्रेज उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कविता पूर्व और पश्चिम की गाथा' (The Ballard of East and West-1889) में इस तक को प्रस्तुत करते हुए कहा है- पूरब पूरब है और पश्चिम पश्चिम है और दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इसने आगे पश्चिमी असाधारणता (Western Exceptionalism) के विचार को जन्म दिया।
निष्कर्ष
अंततः हम कह सकते हैं यह विचार कि केवल पश्चिम ने वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया, अन्य समाजों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अनदेखा करता है। गैर-पश्चिमी सभ्यताओं को अक्सर ऐतिहासिक विवरणों में हीन या पिछड़े के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने वैश्विक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसे पहचानना और इतिहास को अधिक निष्पक्ष, अधिक संतुलित तरीके से बताना महत्वपूर्ण है।
0 Response