
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
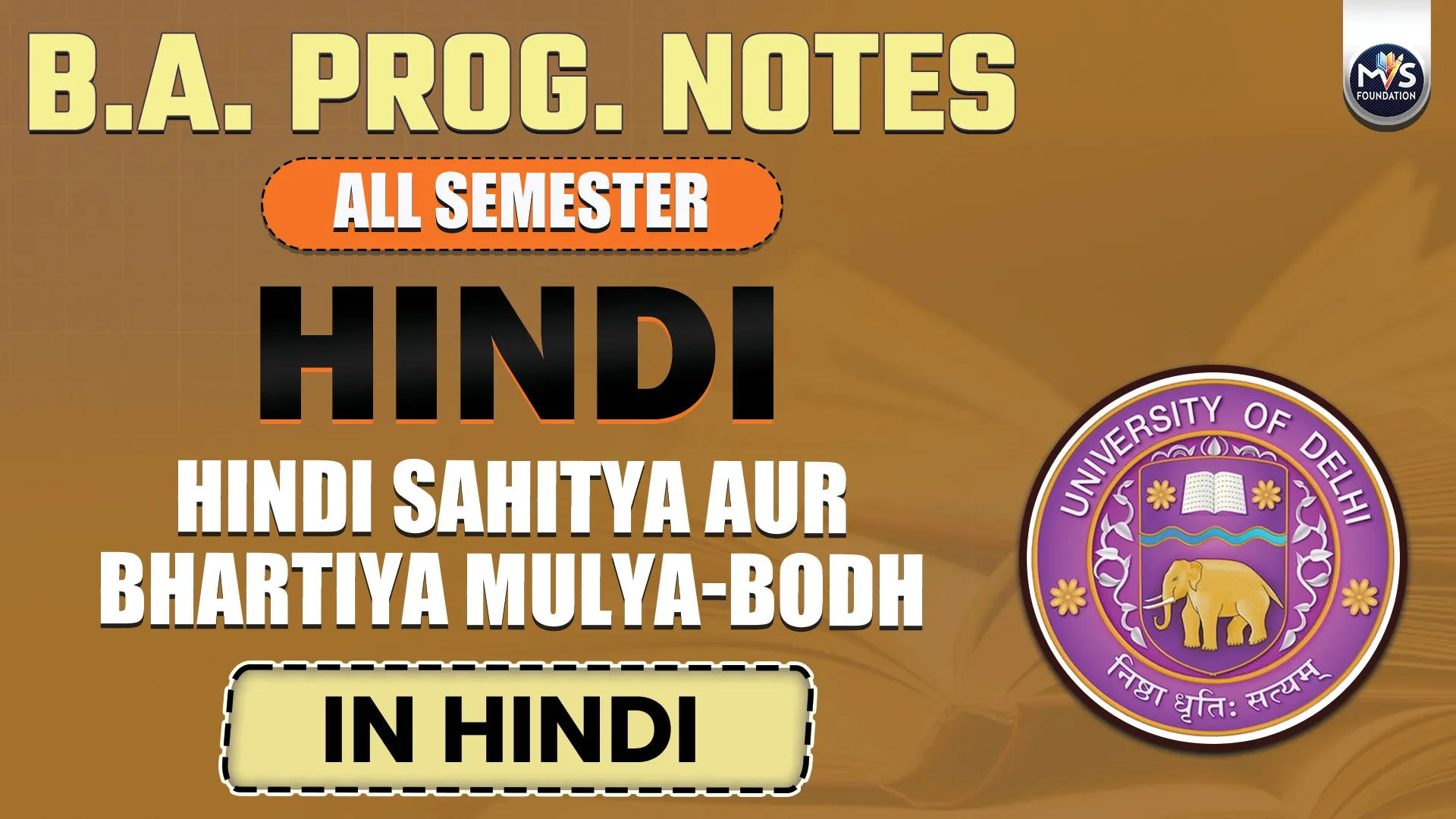
प्रश्न 1 - भारतीय मूल्य-बोध की अवधारणा और हिंदी साहित्य में इसकी विकास यात्रा का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
उत्तर-
परिचय
भारतीय मूल्य-बोध हमारे आदर्श हैं जो हमें परंपरा से विरासत में मिलते हैं। मूल्य-बोध शिक्षा समाज, परिवार, शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों, साहित्य, दार्शनिकों, संतों, महात्माओं, धार्मिक गुरुओं तथा अन्य स्रोतो के माध्यम से हमें इनकी प्राप्ति होती है। मूल्य शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ मूल्य के आर्थिक पक्ष से जुड़ा होता है जो चीज़ों की क़ीमतों पर आधारित होता है। दूसरा अर्थ मूल्य के सामाजिक मामलों से जुड़ा होता है। यह एक प्रकार का सामाजिक दायित्व होता है जो व्यक्ति को निरंतर निभाना पड़ता है। हिंदी साहित्य ने प्रारंभ से ही भारतीय मूल्य-बोध को केंद्र में रखकर समाज को दिशा देने का कार्य किया है। प्रत्येक युग में साहित्यकारों ने समय की परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों को नए रूपों में प्रस्तुत किया।
मूल्य-बोध की अवधारणा मूल्य शब्द का अर्थ 'मूल्य' संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति 'मूल' धातु से हुई है जिसका आशय है कीमत, मोल, लागत इत्यादि। अंग्रेजी में मूल्य के लिए value शब्द का प्रचलन है जो लैटिन के valere शब्द से बना है, इसका अर्थ है-उचित, उपयुक्त आदि। मूल्य शब्द का अन्य अर्थ है-व्यक्ति में निहित आदर्श या सर्वमान्य गुण। किसी वस्तु के संदर्भ में मूल्य का अर्थ होता है उसके विनिमय में दिया जाने वाला पैसा या वस्तु।
मूल्य-बोध की अन्य परिभाषा
डॉ. बैजनाथ सिंहल के अनुसार, "वे (मूल्य) संपूर्ण मानवता का निर्देश करते हैं। मूल्य जीवन में उसी प्रकार संचरित रहते हैं जिस प्रकार शरीर में खून। शरीर के किसी भाग में खून न पहुँचने पर जिस प्रकार शरीर का कोई अंग मर जाता है, वैसे ही मूल्यभाव में मानव जीवन का कोई पहलू दृष्टिविहीन अथवा समाप्त हो जाता है-मूल्य वह सिद्धि है, जो कर्त्ता और वस्तु की सापेक्ष संगति द्वारा उपलब्ध होती है।"
भारतीय मूल्य-बोध की अवधारणा और हिंदी साहित्य में इसकी विकास यात्रा
मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ आदर, मान, सम्मान, अहिंसा, ममता, दया, हिंसा, प्रेम, करुणा, उदारता, क्षमा, दान, सत्यता, असत्यता, सेवा, पूजा, आशीर्वाद, श्राप, जैसे अनेक मानव मूल्यों ने भी जन्म लिया था। भारत की सभ्यता उतनी ही पुरानी है जिनता पुराना मानव समाज का हैं, जैसे- मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिश्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, आदि। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को तीन हिस्सों में बाँटा गया है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीनों में से भक्तिकाल, यानी मध्यकाल का पहला भाग, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल के चार प्रमुख कवि हैं- कबीरदास, सूरदास, जायसी और तुलसीदास। तुलसीदास जिन्होंने अपने काव्य में भगवान श्रीराम के चरित्र के ज़रिए आदर्श जीवन के मूल्य दिखाए हैं। उनकी महान रचना रामचरितमानस में बहुत सुंदर मानवीय मूल्य प्रस्तुत किए गए हैं।
1. आदिकाल, मध्यकाल भारतीय साहित्य और मूल्य-बोध: भारतीय मूल्य-बोध का आधार प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। वेद, उपनिषद, महाभारत, और रामायण जैसे ग्रंथ भारतीय समाज के मूल्य-बोध के निर्माण में अत्यंत प्रभावी रहे हैं। वेदों में धर्म और सत्य की विशेष रूप से चर्चा की गई है। उपनिषदों में जीवन के गूढ़ रहस्यों, आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध, और मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य भारतीय मूल्य-बोध के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। रामायण में आदर्श जीवन और मर्यादा का पालन प्रमुख है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श राजा, पुत्र, और भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाया गया है, और इसके माध्यम से जीवन के जटिल नैतिक प्रश्नों पर विचार किया गया है। इन ग्रंथों ने भारतीय समाज में सत्य, धर्म, और नैतिकता के महत्व को प्रदर्शित किया।
2. भक्ति काल में मूल्य-बोध का विकास: भक्तिकाल के कवि जैसे कबीरदास, सूरदास, जायसी, और रहीम ने अपनी कविताओं के ज़रिए समाज में मूल्यों को फैलाने की कोशिश की। मध्यकाल का साहित्य धर्म से जुड़ा हुआ था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के जीवन के माध्यम से आदर्श धर्म, कर्तव्य, और समाज के प्रति जिम्मेदारी को प्रस्तुत किया। उनका काव्य भारतीय मूल्य-बोध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इन कवियों ने सगुण (राम-कृष्ण जैसे ईश्वर) और निर्गुण (निराकार ईश्वर) दोनों रूपों में भगवान की भक्ति की। उन्होंने लोगों को अन्याय छोड़कर सत्य, अहिंसा, और समानता जैसे अच्छे रास्तों पर चलने की सीख दी। उनकी रचनाओं में दी गई शिक्षा बहुत ही गहरी और मूल्यवान है। जो निम्न है:
साईं इतना दीजिये, जा में कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय।
अर्थात, इंसान को उतना ही माँगना चाहिए जितना उसके और उसके परिवार के लिए जरूरी हो। अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो वह दूसरों की मदद के लिए हो।
मध्यकाल के लगभग सभी कवियों की रचनाओं में भी भारतीय साहित्य और मूल्य-बोध देखने को मिलते है। उत्तर मध्यकालीन कवि बिहारीलाल को आमतौर पर श्रृंगार के कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने भी मूल्यपरक दोहों की रचना की है जो जीवन में उचित मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। बिहारीलाल का निम्नलिखित दोहा जिसमें वे अपने आश्रदाता महाराज जयसिंह को उचित मार्ग पर चलने की नैतिक शिक्षा दे रहे
नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहि बिकासु इहिं काल।
अली कली ही सौं बंध्यौ, आगे कौन हवाल।।
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भी इस प्रकार की अनेक मूल्यपरक रचनाएँ देखने को मिलती हैं। आधुनिक काल में लिखा गया साहित्य विषयवस्तु की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती साहित्य से काफी हद तक भिन्न है। हिंदी साहित्य को मध्यकालीन वातावरण से आधुनिकता के आलोक तक ले आने का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को दिया जाता है।
इस प्रकार, भक्ति काल में हिंदी साहित्य ने भारतीय मूल्य-बोध के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष को प्रमुखता से प्रस्तुत किया।
3. आधुनिक काल में साहित्य और मूल्य-बोध: आधुनिक हिंदी साहित्य में केवल कविता नहीं, बल्कि गद्य में भी नए विचार और मूल्यबोध सामने आए। इस समय के कवियों और लेखकों ने सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम, और नारी अधिकार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, और महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों ने भारतीय समाज के नैतिक और सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत किया।
गुलेरी की कहानी 'उसने कहा था' ने मानवता की नई मिसाल पेश की। भारतेन्दु और उनके मंडल के साहित्यकारों ने राष्ट्रभक्ति को अपनी रचनाओं का मुख्य स्वर बनाया था। चाहे नाटक हो या निबंध अथवा कविता हर विधा में उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयत्न किया था। 'अंधेर नगरी', 'भारत दुर्दशा' आदि नाटकों में राष्ट्रभक्ति के संदेश मौजूद हैं। देशभक्ति वह नया मूल्य-बोध है जो कि भारतेन्दु युग के पहले के साहित्य में नहीं दिखाई देता था। भारतेन्दु ने लिखा है-
अँगरेज राज सुख साज सजे सबभारी।
पै धन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी।।
आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रभाव गाँधीवादी मूल्य-बोध का पड़ा है। गाँधी जी ने कोई मौलिक विचार प्रस्तुत नहीं किया था, बल्कि भारतीय प्राचीन सनातन परंपरा से उन्होंने सत्य, अहिंसा, समरसता, प्रेम, सद्भाव हो। आदि के विचारों को समाज के सामने नए सिरे से प्रस्तुत किया था। इस प्रयोग में गाँधी जी अत्यन्त सफल भी हुए थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरी दुनिया को मानव-मूल्य का संदेश दिया।
भारतेंदु हरिश्चन्द्र के बाद हिंदी साहित्य की कमान महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाली थी। मूल्य-बोध की दृष्टि से देखा जाए तो द्विवेदीयुगीन साहित्य में देश भक्ति, समाज सुधार, नैतिकता, मानवतावाद आदि प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने राष्ट्रवाद को भी साहित्य के प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका का संपादन कार्य हाथ में लेते ही सबसे पहले भाषा सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और अपने समय के साहित्यकारों को नैतिक मूल्य का पाठ पढ़ाया करते थे। श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरीऔध' द्विवेद्वी युग के प्रतिनिधि कवि बनकर उभरे और साहित्य में ऐसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जो पहले हिंदी साहित्य में प्रचलित नहीं थे।
निष्कर्ष
इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि साहित्य के माध्यम से जीवन में अच्छे मूल्यों को पहचाना और अपनाया जाए। मूल्य शब्द का अर्थ अलग-अलग विषयों के अनुसार बदलता है। भारत में मूल्यों को समझने की कई दृष्टियाँ हैं, लेकिन सत्य, अहिंसा, प्रेम्, करुणा, बंधुत्व जैसे शाश्वत (मानवीय) मूल्य सभी जगह समान होते हैं। हर देश के अपने कुछ विशेष मूल्य होते हैं, जो इन्हीं शाश्वत मूल्यों पर आधारित होते हैं। इस पाठ में भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और पारिवारिक मूल्यों को समझा है।
0 Response