
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
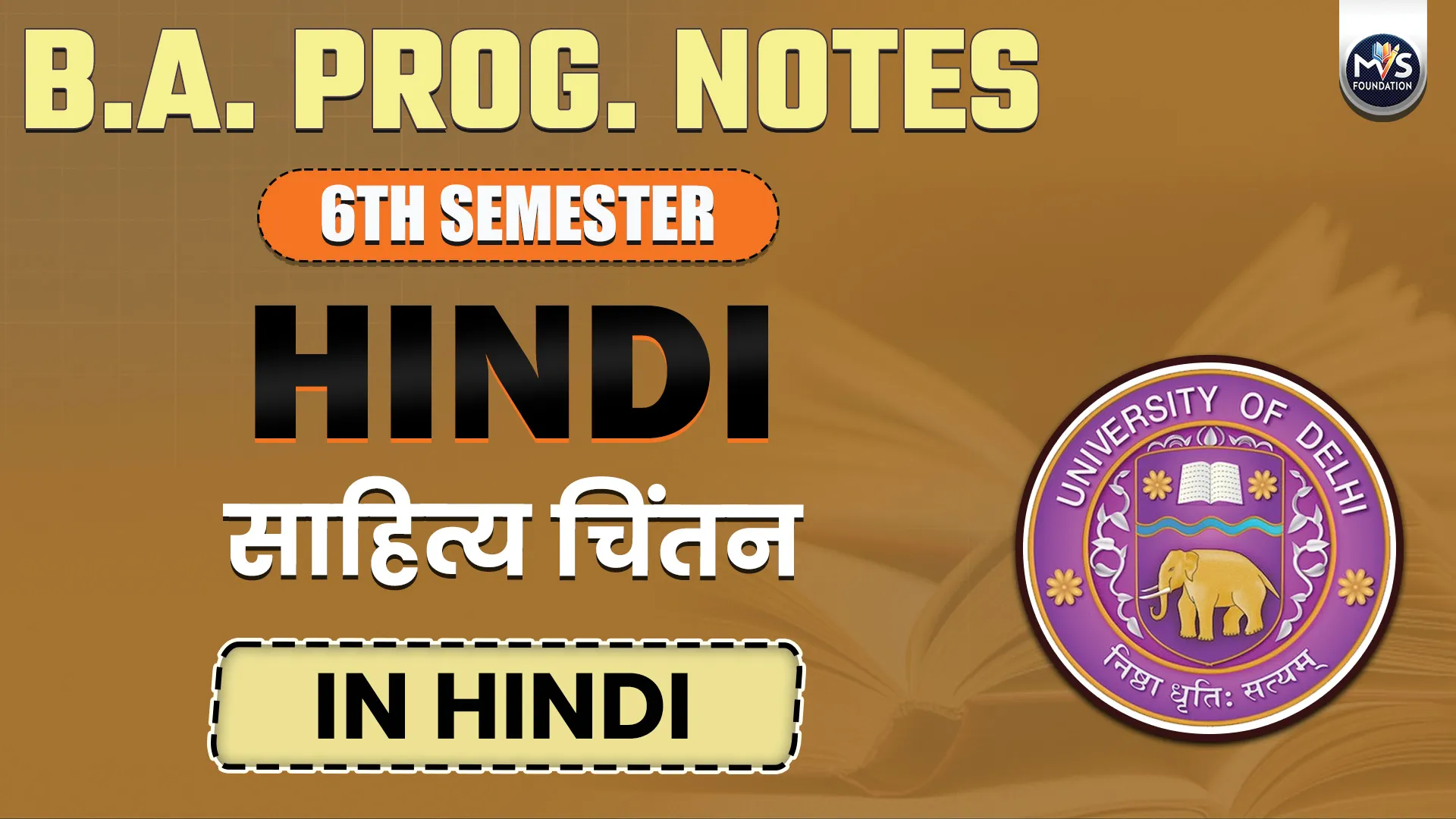
प्रश्न 1 - काव्य की प्रमुख आधुनिक विधा" आख्यानपरक कविता, नवगीत और प्रगीतात्मक कविता का अर्थ और इसके महत्व एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
उत्तर-
परिचय
आधुनिक हिंदी साहित्य का काल सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों से भरा हुआ है। इस समय कविता में नई चेतना आई, जिससे आख्यानपरक कविता, प्रगीतात्मक कविता, नवगीत, छंदमुक्त और मुक्तछंद जैसी विधाओं का जन्म हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम और पश्चिमी प्रभावों के कारण समाज में बदलाव आया, जो कविता की भाषा, विषय और अभिव्यक्ति में झलकता है। छायावाद, प्रगतिवाद, नयी कविता और नवगीत जैसी प्रवृत्तियों ने कविता को आत्माभिव्यक्ति के साथ-साथ सामाजिक यथार्थ से भी जोड़ा। अब कविता केवल सौंदर्य या मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार और बदलाव का माध्यम बन गई है।
आख्यानपरक कविता का अर्थ
आख्यानपरक कविता साहित्य की वह विधा है, जिसमें किसी घटना, कहानी, चरित्र या सामाजिक संदर्भ को काव्यात्मक शैली में वर्णित किया जाता है। इसमें कविता की सुंदरता और कहानी की रोचकता दोनों एक साथ दिखाई देती है। आख्यानपरक कविताएँ किसी पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या काल्पनिक कथा को लयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करती है, जिससे वह साहित्य और पाठक के बीच एक संवाद स्थापित कर सके। 'आख्यान' एक साहित्यिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'वर्णन करना। गद्य साहित्य में इसे कहानी या उपाख्यान' भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की कथा या कहानी होती है, जो किसी विशेष घटना, पात्र तथा विषय के बारे में बताती है। आख्यान में अक्सर पात्र, घटना, स्थान तथा समय इत्यादि तत्व होते हैं। इसे गाथा भी कहा जाता है।
आख्यान मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम 'पौराणिक आख्यान' है। इस तरह के आख्यानों में पौराणिक कथाओं, दंत कथाओं तथा लोक कथाओं को आधार रूप में लिया जाता है। दूसरा 'ऐतिहासिक आख्यानों में मुख्यतः ऐतिहासिक घटनाओं एवं उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तीसरा 'साहित्यिक आख्यान' मुख्यतः साहित्यिक कृतियों और कवियों पर आधारित होते हैं।
आख्यान की विशेषताएँ
1) आख्यान एक ऐसी रचना होती है जिसमें किसी घटना, पात्र या कथा को कहानी की तरह सुनाया जाता है। कई आख्यान गाए भी जाते थे, इसलिए इनमें गीत और कविता जैसा भाव भी होता है। आख्यान पहले मौखिक रूप में सुनाए जाते थे, जिससे ये लोककथाओं का रूप ले लेते थे। अब ये लिखित रूप में भी बहुत प्रचलित है।
2) आख्यान की जड़ें वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत जैसी प्राचीन रचनाओं में मिलती हैं। इनमें देवताओं, ऋषियों और राजाओं की कथाएँ शामिल होती हैं। आख्यान भारत की प्राचीन संस्कृति, धार्मिकता और परंपरा को जीवित रखने में मदद करते हैं। ये सत्य, धर्म, प्रेम, त्याग और करुणा जैसे मानवीय गुणों को सामने लाते हैं।
उदाहरण : ऋग्वेद में इंद्र और अश्विन कुमारों के कई आख्यान मिलते हैं जो उनके पराक्रम और उपकार की कहानियाँ बताते हैं।
3) सी.डब्लू.पी. ने कहा है कि "आख्यान एक गीतात्मक वर्णन प्रधान काव्य है। यह केवल वर्णनात्मक ही नहीं बल्कि गीतात्मक काव्यरूप में वर्णनात्मक कविता है। इस तरह की आख्यानपरक कविता में व्यक्ति की निजी भावनाएँ या अनुभव प्रमुख नहीं होते, बल्कि समाज की सामूहिक भावना और अनुभव प्रधान होते हैं।
नवगीत कविता का अर्थ
हिंदी साहित्य में 1950-60 के दशक में नवगीत का विकास हुआ। जिसका अर्थ है 'नया'। इसमें 'नव' का शाब्दिक अर्थ 'आधुनिक' है। इसका अर्थ है "नया गीत", जो परंपरागत गीतों की तरह छंद और लय में रचा जाता है, लेकिन विषयवस्तु के रूप में यह आधुनिक जीवन की सच्चाइयों, समाज की समस्याओं, राजनीति, संघर्ष, और मानवीय भावनाओं को उजागर करता है। नवगीत छायावादी युग के बाद की कविता है, जो भावनात्मकता के साथ-साथ यथार्थ को भी प्रस्तुत करती है।
नवगीत कविता की विशेषताएँ
1) नवगीत की भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली होती है, जिससे यह आम पाठकों से गहराई से जुड़ता है। इसमें तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय शब्दों के साथ-साथ कहावतों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया जाता है।
2) नवगीत का मूल उद्देश्य बदलते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में मानवीय भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करना है। इसमें परंपरागत गीतात्मकता के साथ आधुनिकता का समावेश होता है, जो इसे अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाता है।
3) नवगीत कविता के केंद्र में मनुष्य और समाज होता है। मनुष्य की प्रवृत्तियां जैसे राग-द्वेष, दुख-दर्द, चिंता, आकांक्षा आदि नवगीत के विषय है। नवगीतकारों में प्रमुख नाम हैं: शंभूनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ओम प्रभाकर, धर्मवीर भारती, और सोम ठाकुर। इन रचनाकारों ने नवगीत को न सिर्फ लोकप्रिय बनाया, बल्कि इसे साहित्य में एक नई और सार्थक दिशा दी। इस प्रकार, नवगीत हिंदी साहित्य में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।
प्रगीतात्मक कविता का अर्थ
प्रगीतात्मक कविता उस प्रकार की कविता होती है जिसमें कवि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अनुभूतियों और विचारों को सीधे, सुंदर और संगीतात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इसे अंग्रेजी में "Lyric" (लिरिक) कहा जाता है। यह कविता भावनाओं की तीव्रता और आंतरिक संवेदनाओं पर आधारित होती है, जिसमें प्रेम, पीड़ा, उल्लास, दुःख, चिंता जैसे भावनात्मक अनुभवों को सहज और लयबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वैयक्तिकता की गहरी छाप होती है, यानी कवि अपनी आत्मा की बात करता है।
प्रगीतात्मक कविता की विशेषताएँ
1) प्रगीतात्मक कविता की सबसे बड़ी विशेषता होती है गेयता, अर्थात इसे गाया जा सकता है। इसकी भाषा सरल, संगीतमय और भावप्रधान होती है, जिससे यह सीधे पाठक या श्रोता के हृदय को छूती है। यह कविता आमतौर पर आकार में छोटी होती है, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई बहुत होती है।
2) महादेवी वर्मा ने प्रगीत को "व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द जो गेय हो सके" कहा है। यानी यह कविता व्यक्ति के भीतरी अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है, जो सुनने में भी मधुर लगे। हरिवंश राय बच्चन भी मानते थे कि गीतों की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी वही है - भावों की एकता, तीव्रता और संगीतमयता।
3) प्रगीतात्मक कविता की परंपरा प्राचीन लोकगीतों से जुड़ी है। संस्कार गीत, ऋतु गीत, धार्मिक गीत, उत्सव गीत जैसे कई रूप गांवों में लोक परंपराओं के साथ विकसित हुए, जिनमें लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं की झलक मिलती है। इस तरह प्रगीतात्मक कविता एक ओर आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो दूसरी ओर लोक जीवन की संवेदनाओं का सजीव चित्रण भी है।
निष्कर्ष
ये तीनों काव्य विधाएँ - नवगीत, प्रगीत और आख्यान हिंदी साहित्य के विविध पक्षों को उजागर करती हैं। जहां नवगीत आधुनिक समाज का दर्पण है, वहीं प्रगीत आत्मा की पुकार और आख्यान भारतीय परंपरा की गाथा है। इनका उद्देश्य न केवल भावों को व्यक्त करना है, बल्कि पाठक को सोचने, समझने और महसूस करने के लिए प्रेरित करना भी है। इस प्रकार, ये विधाएँ मिलकर साहित्य को न केवल सशक्त बनाती हैं, बल्कि समाज को भी दिशा देने का कार्य करती हैं।
0 Response