
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
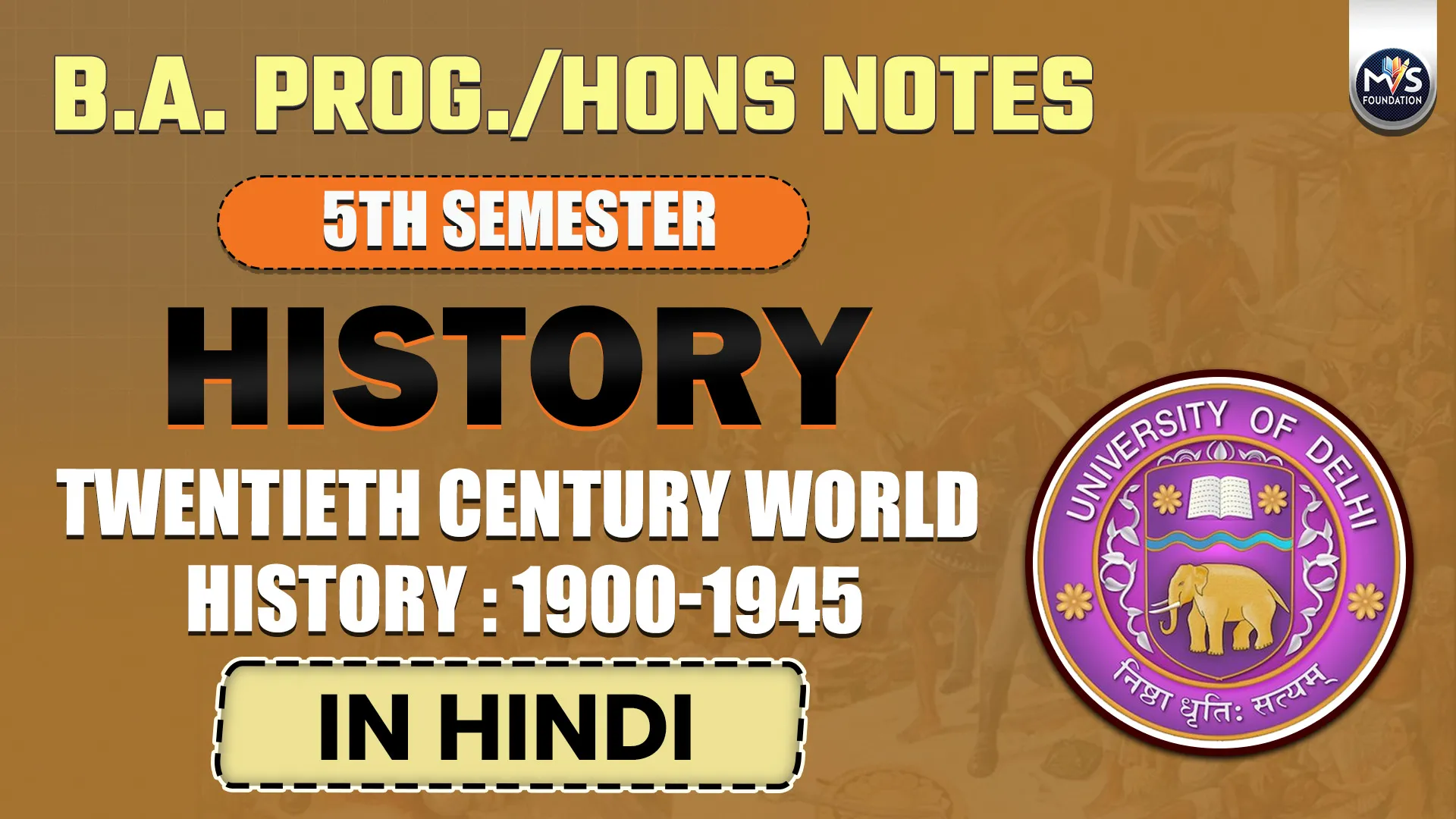
प्रश्न 1 - उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? उपनिवेशवाद के चरणों तथा इसके विरुद्ध किए गए संघर्षों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर -
परिचय
उपनिवेशवाद की जड़े मानव इतिहास में बहुत गहरी है, जिसकी शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी। हालांकि, इसने यूरोपीय अन्वेषण युग (खोज यात्रा का समय) और उसके बाद की शताब्दियों के दौरान प्रमुखता प्राप्त की। 15वीं सदी में स्पेन और पुर्तगाल के साहसी नाविकों, जैसे कोलम्बस और वास्कोडिगामा ने समुद्री यात्राएँ शुरू की और नए क्षेत्रों की खोज की। ये क्षेत्र ही सबसे पहले उपनिवेशवाद का शिकार बने। इस तरह 15वीं सदी में शुरू हुआ यूरोपीय विस्तार 18वीं और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के रूप में पहचान में आया।
उपनिवेशवाद
उपनिवेशवाद का सरल अर्थ : उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर कब्जा करके वहाँ की जमीन, संसाधन और लोगों पर अपना नियंत्रण कर लेता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है।
उपनिवेशवाद के अंतर्गत मुख्यत: दो प्रकार के उपनिवेश हैं -
उपनिवेशवाद के चरण:
उपनिवेशवाद की जटिल प्रक्रिया को यदि चरणबद्ध रूप से समझना हो, तो भारत में उपनिवेशवाद के विश्लेषण से इसे सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। भारत साम्राज्यवाद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश बनाए गए सबसे बड़े और पुराने देशों में से एक है, जिसकी जनसंख्या सभी उपनिवेशों की कुल आबादी से भी अधिक थी।
भारतीय उपनिवेशवाद पर कुछ प्रमुख विचार :
इतिहासकार रजनी पामदत्त लिखते हैं, भारत में औपनिवेशिक कार्यपद्धति का अध्ययन उपनिवेशवाद की सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है।
प्रो. विपिन चंद्र लिखते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन भी प्रभावित हुआ। उनमें एक सम्पूर्ण संसार ही खो गया सामाजिक जीवन का ताना-बाना नष्ट हो गया।
स्वयं लार्ड कर्जन के शब्दों में, 'भारत हमारे दुनिया भर में फैले ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी है। यदि ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधिराज्य का कोई दूसरा हिस्सा गंवा दे, तो भी हम जीवित रह सकते हैं, पर भारत को गंवाने से ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जायेगा।"
भारत में उपनिवेशवाद की उपस्थिति तीन चरणों में देखी जा सकती है:
| भारत में उपनिवेशवाद की उपस्थिति के चरण |
| 1. वाणिज्यवाद | 2. मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद | 3. वित्तीय पूंजीवाद |
Click Here For Full Notes
1. वाणिज्यवाद (1757-1813): 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियाँ भारत आई और व्यापारिक गोदामों व बस्तियों की स्थापना की। प्रारंभिक दौर में उन्होंने भारतीय वस्तुओं जैसे- मसाले, कपड़ा आदि को कम दाम पर खरीदकर अपने देश में ऊँचे दामों पर बेचा। शुरुआत में तो सोना-चाँदी देकर सामान खरीदा गया, लेकिन धीरे-धीरे इस महंगे व्यापार को सस्ता करने के लिए उन्होंने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। इस नियंत्रण ने उन्हें सस्ते में भारतीय सामान हासिल करने और व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने में मदद की।
2. मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद (1813-1858): ईग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद, ब्रिटेन ने भारत से कच्चा माल लेकर अपनी फैक्ट्रियों में सामान बनाया और फिर उसे ऊँचे दामों पर भारत में बेचा। भारत को कच्चे माल के निर्यातक और ब्रिटेन के सामान का बाजार बना दिया गया। इससे भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगी और यहाँ के शिल्पकार बेरोजगार होते गए।
3.वित्तीय पूंजीवाद (1858 के बाद): तीसरे चरण में, अंग्रेजों ने भारत में रेल, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया, जिसमें ऊँची ब्याज दरों की गारंटी के साथ ब्रिटिश पूंजी लगाई गई। इसके जरिए वित्तीय लाभ सीधे ब्रिटेन पहुँचता था, और इस खर्च की भरपाई के लिए भारतीय जनता से कड़ी कर वसूली की जाती थी।
वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद के विरुद्ध किए गए संघर्ष :
युद्ध के बीच के वर्षों में यूरोप के साथ ही एशिया और अफ्रीका में भी बड़े बदलाव हुए। ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तुर्की स्वतंत्र हुआ, और अन्य क्षेत्र विभिन्न शक्तियों में बंट गए। जर्मनी के एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विजयी देशों को मिले। और "राष्ट्रों के आत्मनिर्णय" के सिद्धांत ने दुनियाभर में राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा दिया।
एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन और अफ्रीका में आत्मनिर्णय की लड़ाई
1. यूरोप और मध्य पूर्व में प्रभावः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे तुर्की सहित कई क्षेत्रों में राजनीतिक बदलाव आए। युद्ध के बाद, मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, फ्रांस आदि) ने जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य के पूर्व उपनिवेशों पर नियंत्रण स्थापित किया। तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने तुर्की को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाया। लॉज़ेन की संधि (1923) ने तुर्की को स्वतंत्रता दी, लेकिन मध्य पूर्व के कई हिस्सों पर यूरोपीय शक्तियों का शासन बना रहा, जैसे कि फ्रांस के अधीन सीरिया और लेबनान तथा ब्रिटेन के अधीन इराक, फिलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन ।
2. फिलिस्तीन और यहूदी प्रवास: ब्रिटिश सरकार ने 1917 में बाल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदी समुदाय को बसाने का समर्थन किया। इससे स्थानीय अरबों में असंतोष पैदा हुआ। 1920 और 1930 के दशक में फिलिस्तीन में यहूदी आबादी तेजी से बढ़ी, जिससे यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया।
3. अरब क्षेत्र में संघर्ष मक्का और मदीना: जैसे पवित्र स्थलों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष जारी रहा। 1920 के दशक तक सऊद परिवार ने अरब के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया और 1932 में सऊदी अरब की स्थापना की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यूरोपीय शक्तियाँ अरब क्षेत्र में अपनी पकड़ आसानी से नहीं बना सकतीं।
4. अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन : प्रथम विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका में भी उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन बढ़े। युद्ध के दौरान कई अफ्रीकी सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया और इससे उनमें आत्मनिर्णय की भावना जागृत हुई। अफ्रीकी संसाधनों का यूरोपीय शक्तियों द्वारा शोषण जारी था, लेकिन इससे उत्पन्न असंतोष ने अफ्रीकियों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियोंने युद्ध के बाद अफ्रीका में आर्थिक विकास को लेकर थोड़े-बहुत कदम उठाए, लेकिन यह प्रयास 1930 के दशक में महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही बड़े स्तर पर किए गए।
निष्कर्ष
उपनिवेशवाद इतिहास का ऐसा जिद्दी दाग है जिसे पूरी तरह मिटाना संभव नहीं। इसका प्रभाव आर्थिक असमानताओं, राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक संघर्षों के रूप में आज भी दिखाई देता है। लेकिन यह सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है; उपनिवेशवाद के बाद के सिद्धांत, सुधार के आंदोलन और लोगों का अटूट संकल्प हमें इन ऐतिहासिक गलतियों से सीखकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0 Response