
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
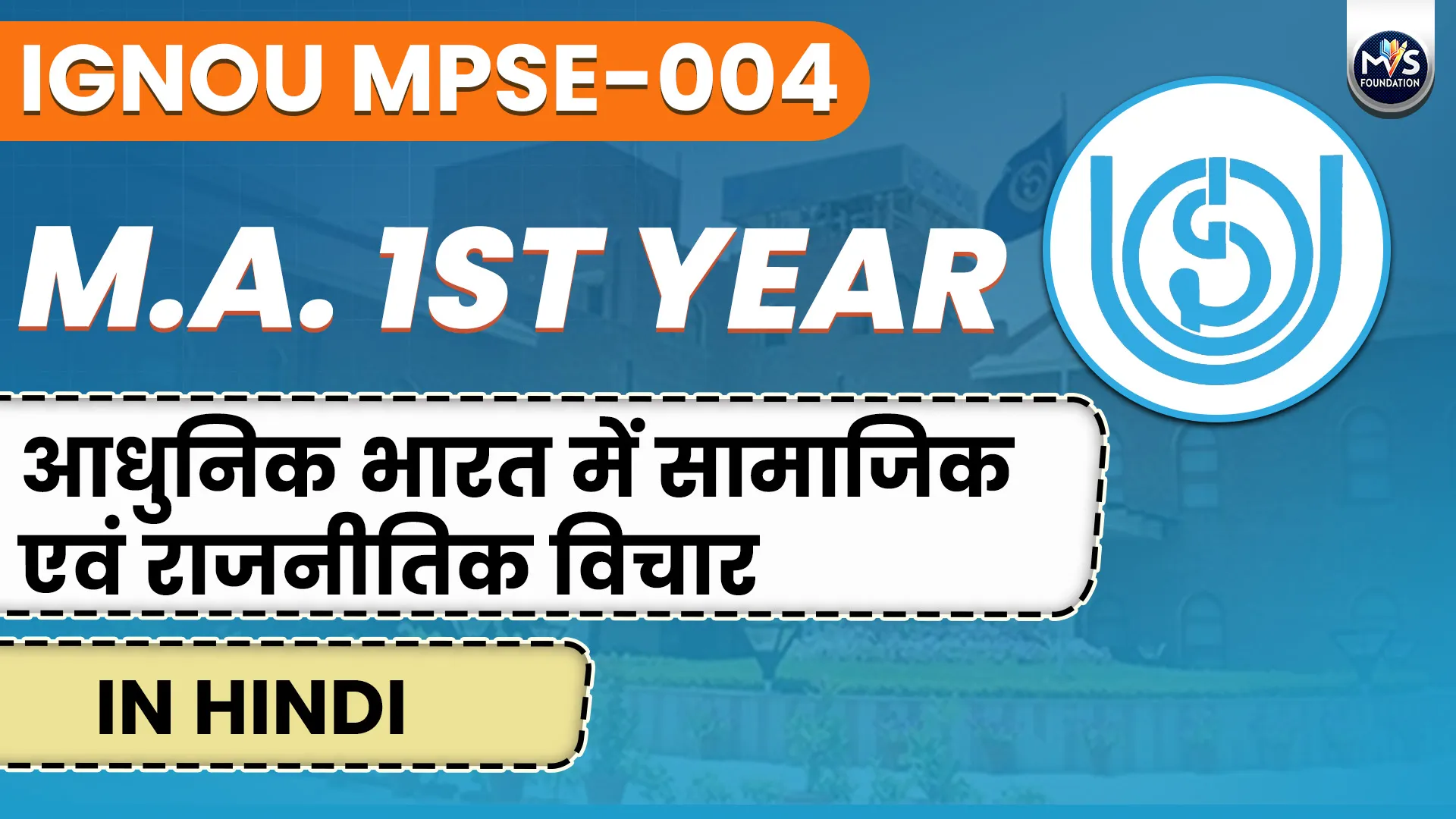
प्रश्न 1 - प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता के स्वरू प का वर्णन कीजिए।
उत्तर -
परिचय
भारत का इतिहास राज्यों और साम्राज्यों की रंगीन कहानियों से भरा है। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था जनपदों से शुरू होकर मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों तक पहुँची, जहाँ राजा धर्म, न्याय और प्रजा की रक्षा का दायित्व निभाता था। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान सत्ता अधिक केंद्रीकृत हो गई, और शासक सर्वसत्ता के प्रतीक बने। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और तिरुक्कुराल जैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर फतवा-ए-जहांदारी और आइने अकबरी जैसे मध्यकालीन ग्रंथों ने राज्य, शासन और संप्रभुता की अवधारणा को अलग-अलग नजरिए से समझाया है।
प्राचीन और मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक समझ :
प्राचीन और मध्यकालीन भारत सम्पूर्ण भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण कालखंड हैं। इन दोनों कालों में भारत में अनेक साम्राज्य, राज्य, राजवंश और शासक उभरे। प्राचीन भारत मानव के उदय से लेकर 1200 ईस्वी तक भारत के इतिहास को संदर्भित करता है, जबकि मध्यकालीन भारत 1200 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चलता है, जब भारत में ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत हुई।
प्राचीन भारत में राज्य और संप्रभुता का स्वरूप :
1. सामाजिक संरचना से राज्य का उदय
प्राचीन भारत में राज्य की अवधारणा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकसित हुई। भारतीय इतिहासकार 'रोमिला थापर' के अनुसार, प्रारंभिक समाज वंशपरंपरा (lineage society) पर आधारित था, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा नियंत्रण होता था। जब जनसंख्या बढ़ी और लोग पशुपालन छोड़कर खेती करने लगे, तब समाज में असमानता बढ़ने लगी, जिससे एक मजबूत शासन की जरूरत महसूस हुई।
महाभारत के शांति पर्व में वर्णित मत्स्यन्याय (जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है) ने यह दर्शाया कि शासन की अनुपस्थिति में समाज में अव्यवस्था फैलती है। इस स्थिति से बचने के लिए लोग एक शासक चुनने या ईश्वर से राजा की मांग करने पर सहमत हुए। यह विचार राजा की देवी उत्पत्ति (Divine Origin of Kingship) और सामाजिक संविदा सिद्धांत (Social Contract | Theory) का आधार बना।
2. राज्य के सात अंग (सप्तांग सिद्धांत)
3. मनुस्मृति में धर्म आधारित शासन:
मनुस्मृति में राजा को दैवी शक्ति प्राप्त बताया गया, परंतु उसका कर्तव्य धर्म, न्याय और व्यवस्था की स्थापना करना था। मनु के अनुसार राजा को ब्राह्मणों की सलाह से शासन करना था और समाज के चार वणो में संतुलन बनाए रखना था। जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकृत प्रशासन, न्याय प्रणाली और लोक कल्याण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए था।
5. बौद्ध, जैन परंपराएँ और तिरुक्कुराल में सुशासन:
बौद्ध धर्म में राजा को धम्मराजा के रूप में आदर्श बताया गया, जो सत्य और अहिंसा के आधार पर शासन करता है। जैन परंपरा में भी नैतिकता और अहिंसा प्रधान शासन का समर्थन मिलता है। तिरुक्कुराल (एक प्राचीन तमिल ग्रंथ) जैसे ग्रंथों में सेना, संसाधन, कूटनीति और योग्य मंत्रियों को सुशासन के लिए आवश्यक बताया गया है।
मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता का स्वरूप :
निष्कर्ष
प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राज्य की संकल्पना सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ क्रमशः विकसित होती रही। जहाँ प्राचीन काल में धर्म, नैतिकता और जनकल्याण पर आधारित शासन को महत्व दिया गया, वहीं मध्यकाल में धार्मिक अधिपत्य, शरियत आधारित नियम और केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली प्रमुख हो गई। हालाँकि, स्वरूपों में भिन्नता थी, लेकिन दोनों ही कालों में राज्य का मूल उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाना और जनहित की रक्षा करना था।
1 Response