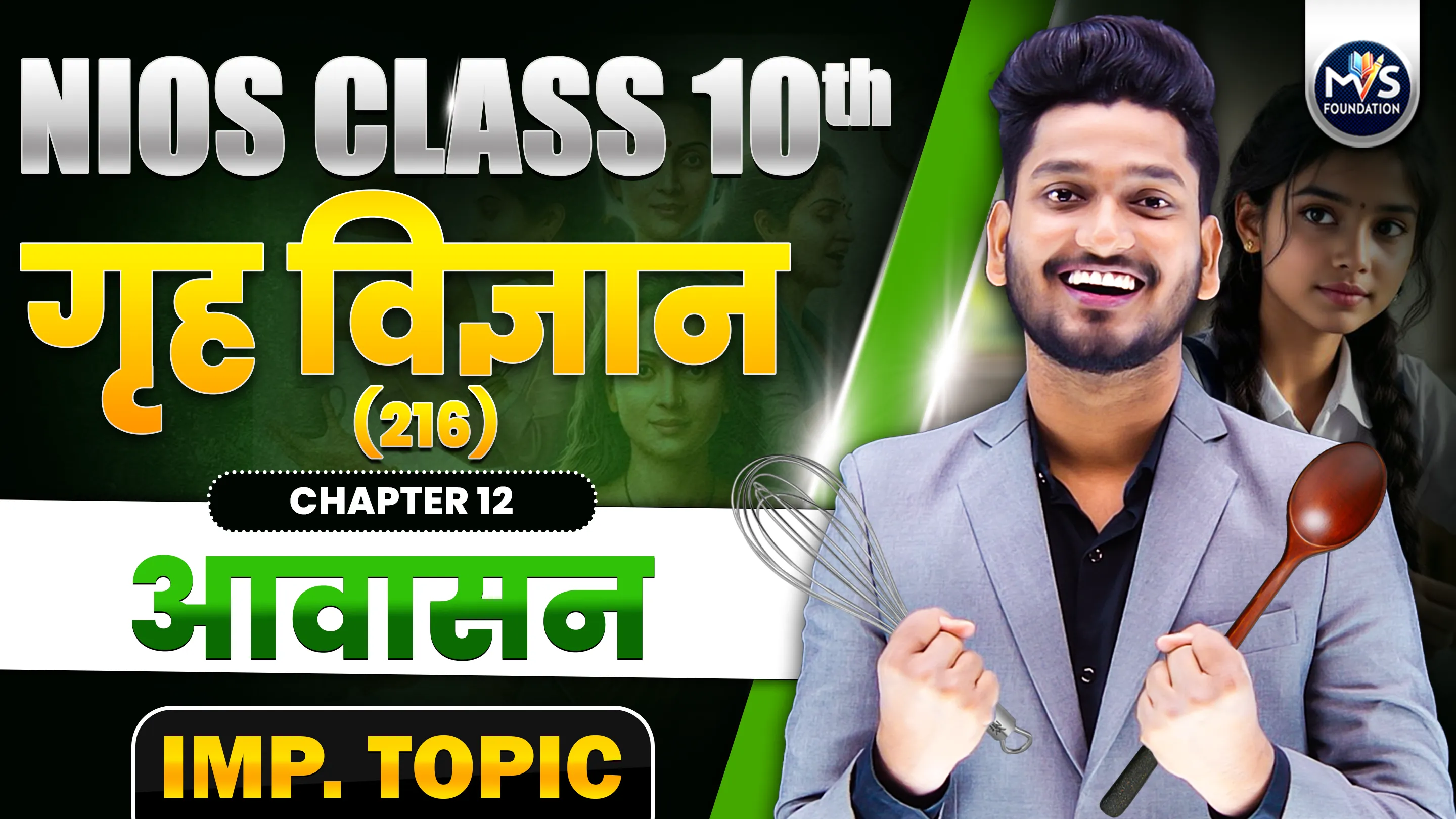NIOS Class-10th Chapter wise Important Topics
HOME SCIENCE(216)
पाठ - 12. आवासन
घर के लिए स्थल का चयन
घर के लिए स्थल का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैं :
- आस-पड़ोस : जहाँ घर का निर्माण करना है। उस स्थल के वातावरण तथा अड़ोस-पड़ोस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां सभी सुविधाएं मौजूद हों, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, यातायात के साधन और जल की निकासी। साथ ही, आस-पास डा कघर, बैंक, स्कूल तथा बाजार आदि सामान्य सुविधाएँ भी उपलब्ध होनी चाहिए।
- भौतिक विशेषताएँ : स्थल का चयन करते समय एक खुले क्षेत्र में घर का चयन करना चाहिए। घर भारी यातायात के समीप नहीं होना चाहिए। यातायात के समीप होने से वायु व ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निचले स्थानों पर भी घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वहां बाढ़ या पानी भराव का खतरा बना रहता है। ऊँचे स्थान पर घर होने से घर का परिदृश्य बेहतर नजर आता है।
- मृदा : मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए क्योंकि उस पर पूरा मकान टिका होता है। मकान की नींव वहाँ की मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। मृदा सतह से 2 से 5 फीट नीचे तक ठोस होनी चाहिए तभी मजबूत नींव पड़ सकती है। पोली मिट्टी में बनाए गए घरों में आगामी वर्षों में समस्या आ सकती है और मिट्टी के खिसकने के कारण मकान एक ओर झुक भी सकता है।
- स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएँ : स्वच्छता की दृष्टि ऐसे खाली प्लॉट, जिनमें कूड़ा- कचरा भरा होता है। ऐसे प्लाटों में मकान के निर्माण की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे प्लॉटों पर घर बनाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें जमीन असमतल होती है और पानी की निकासी की समस्या रहती है। इन जगहों को नई मिट्टी डालकर सड़क के स्तर तक समतल करना जरूरी होता है।
- व्यावहारिक सुविधा : एक घर में रहने वाले वयस्कों को नौकरी पर जाना होता है और बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाना होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपने घर के समीप बाजार की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यात्रा करने के लिए हमें यातायात सुविधाओं तथा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की जरुरत पड़ती है। इसी प्रकार एक परिवार को घर के समीप अन्य व्यावहारिक सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है जैसे डाकघर, बैंक, अस्पताल आदि। ये सुविधाएँ घर से पैदल दूरी पर ही होनी चाहिए।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
घर के भीतर के क्षेत्र
1. स्नानघर
स्नान के स्थान, वाटर क्लोजेट (शौचगृह) और धुलाई के स्थल के संयोजन को स्नानघर कहते हैं। स्नानघर के फर्श गैर-फिसलनभरा तथा आसानी से साफ होने वाला रखना चाहिए। साथ ही, एक दीवार में बाहर से उचित प्रकाश तथा वायु की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ घुटन न हो और हवादार बना रहे।
2. रसोईघर
- रसोईघर पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि सुबह की धूप मिले, जो कीटाणु नष्ट करती है।
- एक रसोईघर में अच्छी निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए रसोई में जाली वाले दरवाजे होने चाहिए ताकि मक्खियाँ और मच्छर वहाँ प्रवेश न कर सकें।
- रसोईघर की एक दीवार घर के बाहरी छोर पर होनी चाहिए ताकि वहाँ से अच्छा प्रकाश तथा स्वच्छ वायु प्राप्त हो सके।
- भोजन पकाने से होने वाले धुएँ को निकालने के लिए एक (एग्जास्ट फैन) भी लगाया जा सकता है। साथ ही, रसोई में संवातन की अच्छी व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए।
- रसोईघर पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि सुबह की धूप मिले, जो कीटाणु नष्ट करती है।
3. शयनकक्ष
शयनकक्ष की व्यवस्था ध्यान से करनी चाहिए क्योंकि हम जीवन का एक तिहाई समय सोने और आराम करने में बिताते हैं। इसमें निजता/अपनापन और शोर से मुक्त होना चाहिए। आयताकार शयनकक्ष में पलंग और अन्य फर्नीचर की सही व्यवस्था होती है। शयनकक्ष के साथ स्नानघर या शौचालय होना चाहिए, और इसमें एक श्रृंगार मेज भी होनी चाहिए।
घर के अंदर तथा बाहर स्वच्छता बनाए रखना
1. प्रकाश : घर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यह घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है, विशेष रूप से रात्रि के समय। प्रत्येक घर में दो प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होती है:
(i) प्राकृतिक प्रकाश : प्राकृतिक स्रोत अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। यह प्रकाश सिर्फ रसोई या बाथरूम के लिए नहीं, बल्कि सभी कमरों के लिए जरूरी है। यदि कमरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती, तो वे अंधेरे और घुटनभरे हो जाते हैं। ऐसे अंधेरे में मच्छर और कॉकरोच आसानी से आ सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इससे संक्रमण और फफूंदी की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
(ii) कृत्रिम प्रकाश : कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होने वाले प्रकाश को कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। जैसे ट्यूब लाईट, बल्ब आदि से प्राप्त प्रकाश। कभी-कभी, घर के सभी हिस्सों में प्राकृतिक प्रकाश मिलना संभव नहीं होता, इसलिए हमें कृत्रिम प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है। रात के समय कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है।
2. संवातन
|
संवातन का अर्थ है कि घर के अंदर ताजगी बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु का प्रवेश घर के अंदर किया जाए तथा अंदर की बासी हवा को बाहर निकाला जाए।
|
स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वायु अत्यंत आवश्यक है। इसे प्राकृतिक तथा कृत्रिम माध्यमों से पूरा किया जा सकता है।
- प्राकृतिक माध्यम : कमरों की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में, अत्यधिक ठंड होने पर भी कमरे की कम से कम एक खिड़की को अवश्य ही खोल कर रखना चाहिए ताकि स्वच्छ वायु सुगमता से घर में प्रवेश कर सके।
- कृत्रिम माध्यम : एक घर में वायु का संचरण/आवागमन की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए घर के दोनों छोरों पर खिड़कियाँ बनाई जा सकती हैं या एक कमरे में दरवाजा व खिड़की को आमने-सामने बनाकर भी इस प्रयोजन को पूरा किया जा सकता है।
3. स्वच्छता
(i)साफ-सफाई बनाए रखना,
साफ़-सफाई के प्रकार
- दैनिक सफाई
- फर्श पर झाडू व पोचा लगाना और सतहों पर झाड़न से सफाई (डस्टिंग) करना।
- दरियों व कालीनों की सफाई व प्रातः काल बिस्तर को ठीक करना।
- सभी वस्तुओं को सही तरीके से रखना।
- साप्ताहिक सफाई
- विभिन क्षेत्रों के फर्श की व्यापक रूप से सफाई जैसे बाथरूम, शौचालय तथा वॉश-बेसिन।
- मकड़ी के जालों को साफ करना और रसोईघर के खानों की सफाई करना।
- दरवाजों के हैंडलों / हत्थे तथा अन्य फिटिंग की सफाई करना।
- लकड़ी की सतहों तथा अन्य क्षेत्रों को पॉलिश करना।
- आइनों तथा तस्वीरों की सफाई करना।
- मौसमी सफाई
- गद्दों, कुशन, तकियों, दरियों तथा कालीनों को हवा लगाने के लिए धूप में रखना एवं परदों को धोना और साथ ही भंडारगृह की सफाई करना।
- पूरा फर्नीचर हटाने के बाद कमरों की व्यापक रूप से सफाई करना।
- लकड़ी की वस्तुओं की सफाई व पॉलिश करना और उनकी मरम्मत का कार्य।
(ii) कूड़े-कचरे को हटाना
(क) वॉटर क्लोजेट : अधिकतर बड़े शहरों में मानव मल की सफाई जल वहन प्रणाली द्वारा की जाती है। इस प्रणाली में घर के अपजल के साथ-साथ मल तथा मूत्र को भी निकासी तथा सीवरों की प्रणाली के माध्यम से जल द्वारा फ्लश किया जाता है। वॉटर क्लोजेट मानव शौच के लिए एक सेनिटरी संस्थापन है। यह एक पाईप के माध्यम से सीवर लाईन के साथ जुड़ा होता है।
(ख) सेप्टिक टैंक : मानव तथा अन्य अपशिष्टों के निपटान के लिए मल-निकास प्रणाली एक आदर्श समाधान है, किन्तु इसके निर्माण की लागत अत्यधिक होती है। इसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। सेप्टिक टैंक एक विकल्प है, जो अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उपयोग होता है जहाँ मल-निकास प्रणाली नहीं है। इसमें कंक्रीट के टैंक या गर्त बनाए जाते हैं, जिनसे घरेलू निकास पाइपों को जोड़ा जाता है।
सेप्टिक टैंक के लाभ :
- ये वॉटर क्लोजेट प्रणाली की तुलना में कम लागत तथा निर्माण में आसान होते हैं।
- सेप्टिक टैंक भूमि या भूमि जल को प्रदूषित नहीं करते हैं, एवं दुर्गंध से मुक्त है।
- मच्छरों, कीटाणुओं तथा मक्खियों को पनपने से रोकते हैं।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में