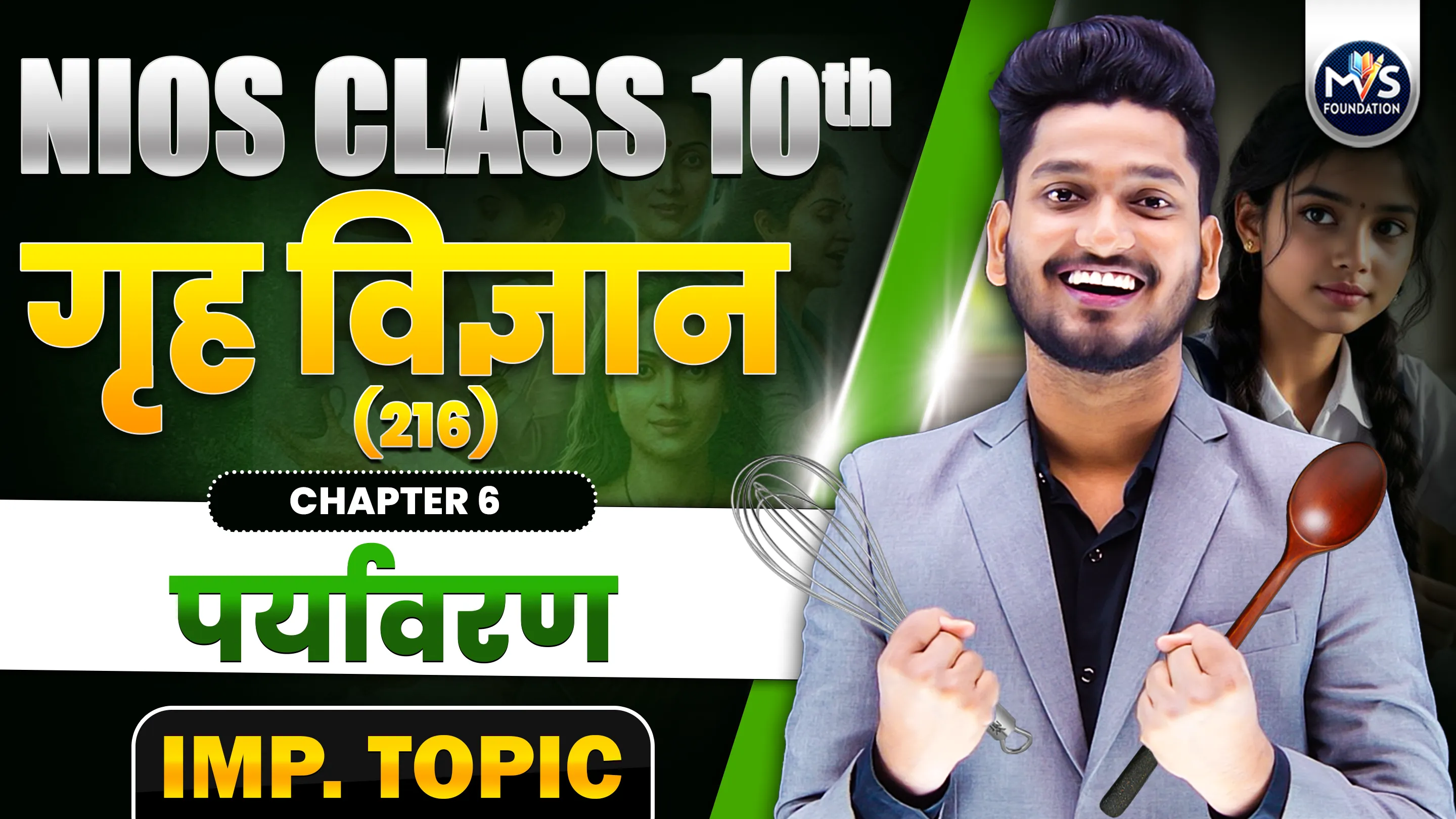NIOS Class-10th Chapter wise Important Topics
HOME SCIENCE(216)
पाठ - 6 पर्यावरण
प्रदूषण
पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का, उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना "प्रदूषण" कहलाता है।
प्रदूषक : वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट आदि सभी प्रदूषकों के उदाहरण हैं।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
प्रदुषण के प्रकार
1. वायु प्रदूषण :
वायु प्रदूषण से तात्पर्य हवा में होने वाले किसी भी भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन से हैं। यह हानिकारक गैसों, धूल व धुएं द्वारा होने वाला प्रदूषण है जो पौधों, जानवरों व मनुष्यों को प्रभावित करता है।
वायु प्रदूषण के प्रभाव
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम
- घर में धुआँ रहित चूल्हे का उपयोग करें। धुएँ को बाहर निकालने के लिए चूल्हे पर बड़ी चिमनी का प्रयोग करें। इसके अलावा, घर में सौर कुकर उपयोग करें, जिसमें सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है।
- बायोगैस का प्रयोग करें क्योंकि यह धुआँ-रहित ईंधन है।
- फैक्टरियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए।
- सीसा रहित पैट्रोल का उपयोग व सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए।
- कूड़े-कचरे को जलाना नहीं चाहिए। इसका निपटान साफ-सुथरे तरीके से करना चाहिए। संभव हो तो भूमि-भराव द्वारा कूड़े का निपटान किया जाए।
- सड़के पक्की होनी चाहिए ताकि धूल न उड़े और वातावरण में न मिल सके।
- वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे वायु को ताजा और शुद्ध रख सकें।
2. जल प्रदूषण:
जल प्रदूषण से तात्पर्य पानी में ऐसे हानिकारक तत्वों का मिल जाना जिससे पानी पीने व उपयोग करने योग्य नहीं रहता हैं।
जल प्रदूषण के प्रभाव
- प्रदूषित जल पीने से हैजा, टायफाइड, तपेदिक और पेचिश जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा, प्रदूषित पानी से नहाने पर त्वचा संबंधी रोग तथा एलर्जी हो जाती है।
- जल में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ और समुद्री पौधे भी प्रभावित होते हैं क्योंकि प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वे प्रदूषित जल में मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वे साँस नहीं ले पाते हैं।
जल प्रदूषण के नियंत्रण के तरीके
- सुनिश्चित करें कि जल के स्रोत में गंदा जल तो नहीं मिल रहा है।
- उद्योगों द्वारा गैर-उपचारित अपशिष्टों को नदियों या तालाबों में डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- खुले में तथा जल-स्रोत के समीप शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उचित शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए।
- जल स्रोत में या उसके समीप नहाना अथवा कपड़े धोना या पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। कपड़ों को धोने तथा पशुओं को नहलाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए तालाबों तथा कुओं में एकत्र वर्षा के जल का प्रयोग करना चाहिए।
- कूड़ा-कचरा नदियों और समुद्रों में नहीं डालना चाहिए।
- जल को साफ बर्तनों में भरकर तथा ढक कर रखना चाहिए। पानी निकालने के लिए हाथों को पानी में नहीं डुबोना चाहिए।
3. मृदा प्रदूषण:
मृदा प्रदूषण से तात्पर्य मृदा में होने वाले भौतिक, रासायिनिक तथा जैविक परिवर्तन से है, जिनका मनुष्यों और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मृदा तब प्रदूषित होती है जब उसमें फैक्टरियों के अपशिष्ट के रूप में रसायन और धातुओं को फेंका जाता है।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
मृदा प्रदूषण के प्रभाव
- घर, शौचालय, पेशाब और खुले में थूकने से मृदा में रोगाणु फैलते हैं। जब हम नंगे पाँव मिट्टी में चलते हैं, तो ये जीवाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं।
- औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट मिट्टी में हानिकारक रसायन छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। ऐसी मिट्टी में उगने वाले पौधे और सब्जियाँ इन हानिकारक रसायनों को अपने में अवशोषित कर लेती हैं। मनुष्य तथा पशु इन फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं।
मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के माध्यम
- कूड़े-कचरे का उचित निपटान : घर के कूड़े-कचरे का उचित निपटान होना चाहिए ताकि इस पर मक्खियाँ, मच्छर और कॉकरोच न पनप सकें। घर में इसे एक ढक्कनयुक्त कूड़ेदान में ही इकट्ठा करना चाहिए।
- भूमि-भरान : घर के अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में भर दिया जाता है और इन्हें टहनियों और पौधों से ढक दिया जाता है ताकि इन पर मक्खियाँ और मच्छर न पनप सकें। जब ये गड्ढे भर जाते हैं तो इन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है।
- खाद बनाना (कंपोस्टिंग) : बगीचे से एकत्र कूड़े-कचरे को बागीचे के एक कोने पर गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। प्रति-दिन शाम को इसे राख और पत्तियों से ढक दिया जाता है। धीरे-धीरे निचली परतें खाद बनती जाती हैं। इस खाद को बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- भस्मीकरण (Incineration) : कूड़े-कचरे के निपटान की सबसे आधुनिक तकनीक भस्मकारी संयंत्र का प्रयोग करना है। भस्मक एक भट्टी होती है, जिसमें कूड़ा-कचरा जल जाता है। यह एक मंहगा तरीका है, क्योंकि कूड़े-कचरे को जलाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, परन्तु यह बहुत सुरक्षित तरीका है। इससे धीरे-धीरे कूड़ा-कचरा राख के छोटे से ढेर में बदल जाता है।
मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपाय हैं :
- स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग
- कीटनाशक तथा उर्वरकों का सीमित प्रयोग
- पर्यावरणसहिष्णु वस्तुओं का प्रयोग
4. ध्वनि प्रदूषण
पर्यावरण में अवांछित या परेशान करने वाली ध्वनि जो मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है।
ध्वनि प्रदूषण के स्रोत
- मोटर-वाहन, रेलगाड़ियाँ और विमान
- लाउडस्पीकर, रेडियों तथा टेलीविजन, जब वे ऊँची आवाज में चल रहे हों।
- उद्योग तथा मशीनें
ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव
- अधिक शोर सुनने से नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द और श्रवण-शक्ति पर कुप्रभाव होता है।
- फैक्टरियों में काम करने वाले लोग, पायलट और ड्राइवर जो शोर भरे वातावरण में रहते हैं, अक्सर धीमी आवाज़ें ठीक से नहीं सुन पाते। उनके कान के पर्दे खराब हो जाते हैं और कभी-कभी वे बहरे भी हो जाते हैं।
- अधिक शोर के कारण तनाव बढ़ता है और मानसिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम
- रेडियो तथा टेलीविजन धीमी आवाज में चलाना।
- लाउडस्पीकर इस्तेमाल न करना।
- अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का हॉर्न बजाना।
- फैक्टरियों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना।
- हवाईअड्डों का निर्माण शहर से बाहर करना।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में