
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
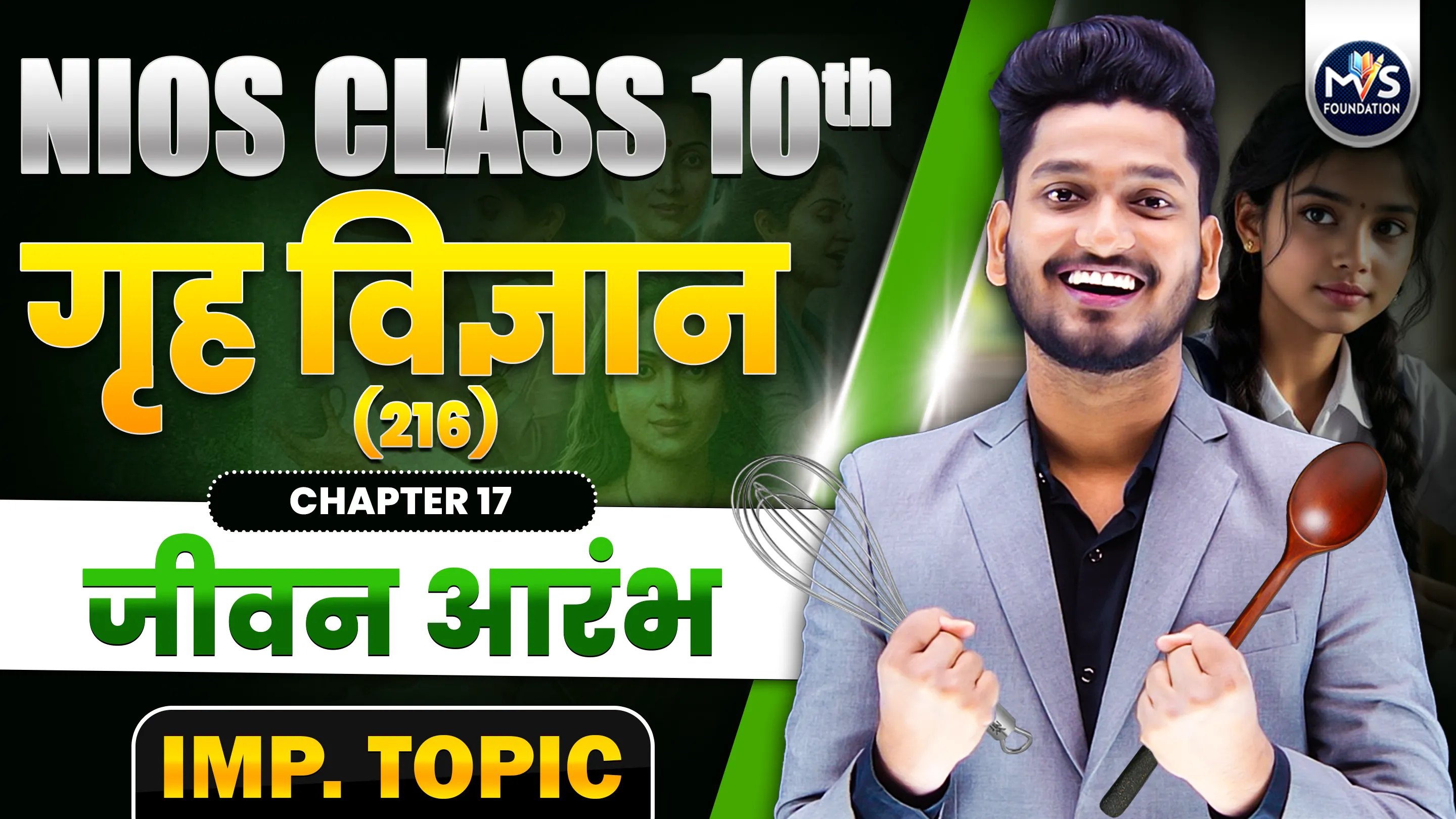
NIOS Class 10th Chapter 17th Important Topics
Home Science (216)
पाठ - 17 जीवन आरंभ
गर्भावस्था के चिह्न
निषेचन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही महिला के शरीर में अनेक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं अर्थात शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनी परिवर्तन और भावात्मक परिवर्तन। इनमें से कुछ परिवर्तन हैं -
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक
1. माँ की भावनात्मक स्थिति : मानसिक रूप से स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। इसलिए माँ को लंबे समय तक तनाव तथा दबाव की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। माँ की उत्तेजना, निराशा, भय या दुःख की भावनाओं से भ्रूण पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जन्म के पश्चात शिशु में चिड़चिड़ेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
2. माँ का आहार : एक माँ को उचित मात्रा में आहार लेना चाहिए ताकि शिशु को उचित आहार मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रूण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा भोजन उसे माँ के गर्भनाल से प्राप्त होता है। एक गर्भवती महिला के आहार में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए।
4. माँ की आयु
शिशु को जन्म देने के लिए माँ की सही उम्र 20 से 35 साल के बीच होती है। 20 साल से पहले माँ की जनन प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती, ऐसी स्थिति में शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर शिशु का जन्म हो सकता है साथ ही, माँ व शिशु के जीवन को जोखिम में डाल सकता है तथा गर्भपात का खतरा पैदा हो सकता है।
5. माँ द्वारा दवाईयों का सेवन
कुछ दवाईयाँ गर्भनाल से होते हुए शिशु के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए एक गर्भवती महिला को किसी प्रकार की दवा लेने से पूर्व डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। साथ ही, गर्भावस्था में एक्स-रे से बचना चाहिए क्योंकि इससे गर्भ में बच्चे के विकास को नुकसान हो सकता है।
6. भ्रूण को प्रभावित करने वाले रोग, कीटाणु : माँ को जर्मन मिजल्स, यौन संक्रामक रोग या एड्स जैसी बीमारियाँ होती हैं, तो उनके कीटाणु गर्भनाल से होकर बच्चे तक पहुँच सकते हैं और उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था में माँ को संक्रामक रोगों से बचना चाहिए।
7. नशीले पदार्थ, शराब, धूम्रपान : सिगरेट या बीड़ी का धुआँ, शराब या नशीली दवाओं के रसायन जैसे अफीम (मार्फिन) गर्भनाल के रास्ते से भ्रूण की रक्तनलिकाओं में पहुँचते हैं और उसे भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं।
गर्भवती महिला की देख-रेख (प्रसव पूर्व देखरेख)
चिकित्सा जाँच :
पोषण :
दवाईयाँ लेना :
व्यायाम तथा आराम :
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
नवजात शिशु तथा माँ की देखभाल (प्रसव पश्चात् देखभाल)
1. स्वच्छता :
(क) नवजात शिशु की साफ-सफाई : नवजात शिशु की त्वचा में प्रायः झुर्रियाँ होती हैं, और उसकी त्वचा सफेद मक्खन जैसे तत्व या कुछ महीन बालों से आवरित होती है। उसके शरीर को गुनगुने पानी से भीगे हुए स्वच्छ कपड़े से साफ करें। उसकी त्वचा को रगड़े नहीं क्योंकि ये दोनों ही तत्व संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और समय के साथ अपने-आप निकल जाते हैं।
(ख) नाल को काटते समय सावधानी : विकसित भ्रूण अम्बिलिका नामक नलिका द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। शिशु का जन्म होने पर उस नाल को काटकर प्लेसेंटा से अलग किया जाता है। काटी गई नाल को उसे शुष्क रखने के लिए उस पर हवा लगना आवश्यक है। यदि घर साफ-सुथरा है और वहाँ मक्खियाँ नहीं हैं तो काटी गई नाल को खुला छोड़ दीजिए। यदि घर में धूल-मिट्टी या मक्खियाँ हैं तो उसे हल्के से ढ़क लें।
2. टीकाकरण :
शिशु को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किए जाने की आवश्यकता होती है। माँ के रूप में आपको अपने शिशु के लिए उचित टीकाकरण कार्यक्रम का पता लगाना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को सही समय पर सही टीका लगा सकें।
माँ के दूध तथा बोतल के दूध के बीच तुलनात्मक विवरण :
|
स्तनपान |
बोतल का दूध |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
परिवार नियोजन : परिवार नियोजन से तात्पर्य परिवार में दो बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर से है। परिवार का नियोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रह सकें।
1. अनियोजित परिवार : अनियोजित परिवार वह परिवार होता है जिसमें बच्चों की संख्या माता-पिता की इच्छाओं या आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं होती। ऐसे परिवारों में बिना योजना के अधिक बच्चे होते हैं, जो संसाधनों और जीवन स्तर पर दबाव डाल सकते हैं।
2. नियोजित परिवार : नियोजित परिवार वह है जिसमें दंपत्ति संतान की संख्या और उनके जन्म का समय तय करते हैं, ताकि माता-पिता और बच्चों का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति संतुलित रहे। इसमें परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग किया जाता है।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
0 Response