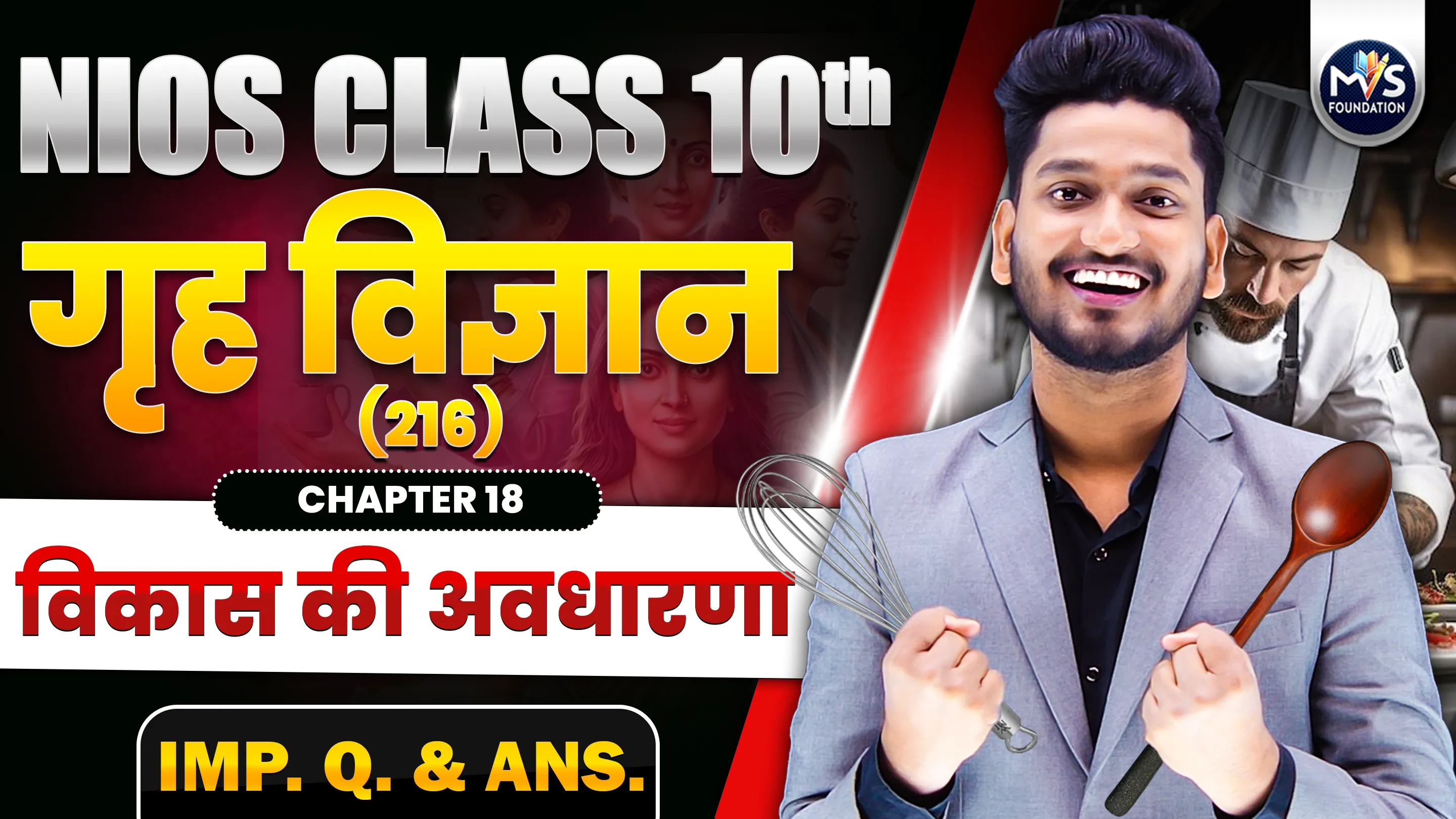NIOS Class-10th Chapter wise Important Topics
गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
Ch- 18. विकास की अवधारणा
प्रश्न 45. अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर - अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर :
|
अभिवृद्धि
|
विकास
|
|
|
- विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है।
|
- अभिवृद्धि शरीर की ऊंचाई, वजन और विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क के आकार और संरचना में वृद्धि से संबंधित है।
|
- इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संवेदी परिवर्तन भी शामिल हैं।
|
- जीवन की एक निश्चित अवधि में विकास रुक जाता है।
|
- विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
|
- अभिवृद्धि को देखा, मापा व तोला जा सकता है, उदाहरण के लिए - शरीर की लंबाई और वजन में वृद्धि और दांत निकालना आदि।
|
- व्यक्ति के परिपक्व आचरण से ही विकास देखा जा सकता है।
|
- अभिवृद्धि का संबंध व्यक्तित्व के एक आयाम अर्थात, मुख्यता शारीरिक संरचना से सम्बंधित हैं।
|
- विकास व्यक्तित्व के सभी आयामों को दर्शाता है, क्योंकि यह शारीरिक संरचना के साथ-साथ कार्यात्मकताओं को भी दर्शाता है।
|
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में
प्रश्न 46. विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए ।
उत्तर - विकास के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं :
- विकास का एक निश्चित क्रम होता है : सभी शिशुओं में विकास एक निश्चित क्रम में दो प्रकार से होता है-
(a) मस्तकाधोमुखी विकास : इस क्रम में विकास सदैव सिर से शुरू होकर पैर की तरफ होता है। इसी कारण गर्भावस्था में पहले भ्रूण के सिर का, फिर धड़ का तथा आखिर में पैरों का विकास होता है। इसलिए जन्म के समय नवजात का धड़ उसके सिर के अनुपात में छोटा होता है।
(b) निकट से दूर दिशा में विकास : इस क्रम में शारीरिक विकास शरीर के केन्द्रीय भागों से शुरू होकर आगे की ओर होता है। जैसे कि- पहले हृदय तथा पेट, फिर कंधे, बाजू और फिर हाथ विकसित होते है। इसी कारण बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना तथा बाद में चलना सीखता हैं।
 |
- विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है : विकास जीवनभर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज तो हो सकती है परन्तु रुकती नहीं।
- विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है : बच्चों में पहले सामान्य योग्यताओं का विकास होता है और फिर धीरे-धीरे विशिष्टताओं का विकास होता है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, आयु में वृद्धि के साथ-साथ वह उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है, क्योंकि छोटी मांसपेशियों का विकास अधिक समय लेता है।
- विकास की सभी अवस्थाएँ समान होती हैं : प्रत्येक बालक के लिए विकास की सभी अवस्थाओं का एक जैसा क्रम होता है। जैसे कि- बालक पहले भ्रूणावस्था, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था से गुजरता है और फिर किशोरावस्था में पदार्पण करता है। कोई भी बालक शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में नहीं जा सकता।
- विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग-अलग होती है : शरीर के सभी अंगों के विकास की अपनी अलग गति होती हैं, जैसे कि किशोरावस्था में हाथों-पैरों का विकास पूर्ण हो जाता है जबकि कंधे अधिक देर से विकसित होते हैं।
- जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न होती जाती है : वृद्धि एवं विकास की दर प्रारम्भिक बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ कम होती है जबकि भ्रूणावस्था तथा किशोरावस्था में अधिक।
- सभी बच्चे अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँचते हैं : बच्चों के विकास की गति अलग-अलग होने के कारण वह जल्दी या देर से अपने विकास की चरम सीमा अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इस चरम सीमा तक पहुँचने के लिए उचित पोषण, स्वस्थ वातावरण, सही निर्देशन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण एवं प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रश्न 47. विकास को प्रभावित करने वाले कारको को लिखिए ।
उत्तर - विकास को प्रभावित करने वाले कारक:
- आनुवांशिकता तथा वातावरण : आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों प्रभावपूर्ण कारक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विकास के प्रति इसे सकारात्मक बनाने के लिए वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ वातावरणिक कारक हैं: पोषण, आरंभिक प्रेरणा तथा बच्चे के पालन-पोषण की विधियाँ।
- पोषण : बहुत अधिक या बहुत कम खाना स्वस्थ या अस्वस्थ भोजन करना, ये सब हमारी शारीरिक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक तथा मानसिक गुणों की दृष्टि से बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए उचित पोषण अनिवार्य है। बच्चे को इष्टतम वृद्धि तथा विकास के लिए नियमित आधार पर संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के कारण बच्चे में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं जो न केवल उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
- आरंभिक उत्प्रेरक : प्ररेक वातावरण बच्चे के आनुवांशिक गुणों को विकसित करने में सहायक होता है। प्रेरक वातावरण अच्छे शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक होता है, जबकि गैर-प्ररेक वातावरण के कारण बच्चे का विकास उसकी क्षमताओं से कम होता है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से बच्चा अपनी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है।
- बच्चों के पालन-पोषण की विधियाँ : अनुज्ञात्मक माता-पिता के बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना की कमी होती है, भावात्मक नियंत्रण खराब होता है तथा जो भी काम वे करते हैं उसमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों को पालन-पोषण उदारवादी या दृढ़ चित्त माता-पिता द्वारा किया जाता है वे व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से बहेतर ढंग से समायोजन कर पाते हैं।
समग्र रूप में आनुवांशिक कारक तथा वातावरणिक कारकों का संयोजन बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है और उनमें अंतर निर्धारित करता है।
प्रश्न 48. स्कूल - पूर्व बच्चों में किन सकल गत्यात्मक गतिविधियों तथा कौशलों को देखा जा सकता है ?
उत्तर - स्कूल-पूर्व बच्चों में निम्नलिखित सकल गत्यात्मक गतिविधियों तथा कौशलों को देखा जा सकता है :
- दौड़ना : पहले दौड़ना चलने से कुछ अधिक कठिन होता है। किन्तु 5 या 6 वर्ष की आयु तक बच्चा बिना गिरे आसानी से दौड़ने लगता है।
- उछलना : बच्चा अपने चौथे जन्मदिन तक आसानी से छलाँग लगाता है। वह लगभग 12 इंच की ऊँचाई से छलाँग लगा सकता है। पाँच वर्ष की आयु के बच्चे को अवरोधों के ऊपर से छलाँग लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
- रस्सी कूदना तथा छल्ला घुमाना : रस्सी कूदना तथा छल्ला घुमाना उछलने के परिवर्तित रूप हैं। यदि उसे अवसर दिया जाए तो 6 वर्ष की आयु तक बच्चा अच्छी तरह से रस्सी कूदने लगता है
- चढ़ना : दो वर्ष की आयु से पूर्व बच्चा रेलिंग पकड़ कर या किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ कर सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जा सकता है। सीढियाँ चढ़ने की वयस्कों की विधि जिसमें पहले एक पैर फिर दूसरे पैर का प्रयोग किया जाता है, इस विधि को बच्चा 4 वर्ष की आयु में सीख लेता है, बशर्ते बच्चे को ऐसा करने का व्यापक अवसर प्राप्त हो ।
- तिपहिया साइकिल चलाना : दो वर्ष की आयु तक, बहुत कम बच्चे तिपहिया साइकिल चला पाते हैं। 3 से 4 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे, जिन्हें ऐसा करने का अवसर प्राप्त होता है वे इस साइकिल को चला पाते हैं।
- गेंद फेंकना तथा पकड़ना : 6 वर्ष की आयु तक बच्चे इस कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, हालाँकि प्रत्येक आयु में इस कौशल में व्यापक अंतर होता है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम बच्चा बॉल को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का प्रयोग करता है। उसके बाद वह केवल अपने हाथों का प्रयोग करता है। बाद में वह पूर्णत समन्वयित रूप से अपनी हथेलियों के बीच में बॉल को पकड़ लेता है।
✅ सभी महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here: गृह विज्ञान (216) | हिंदी में