
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
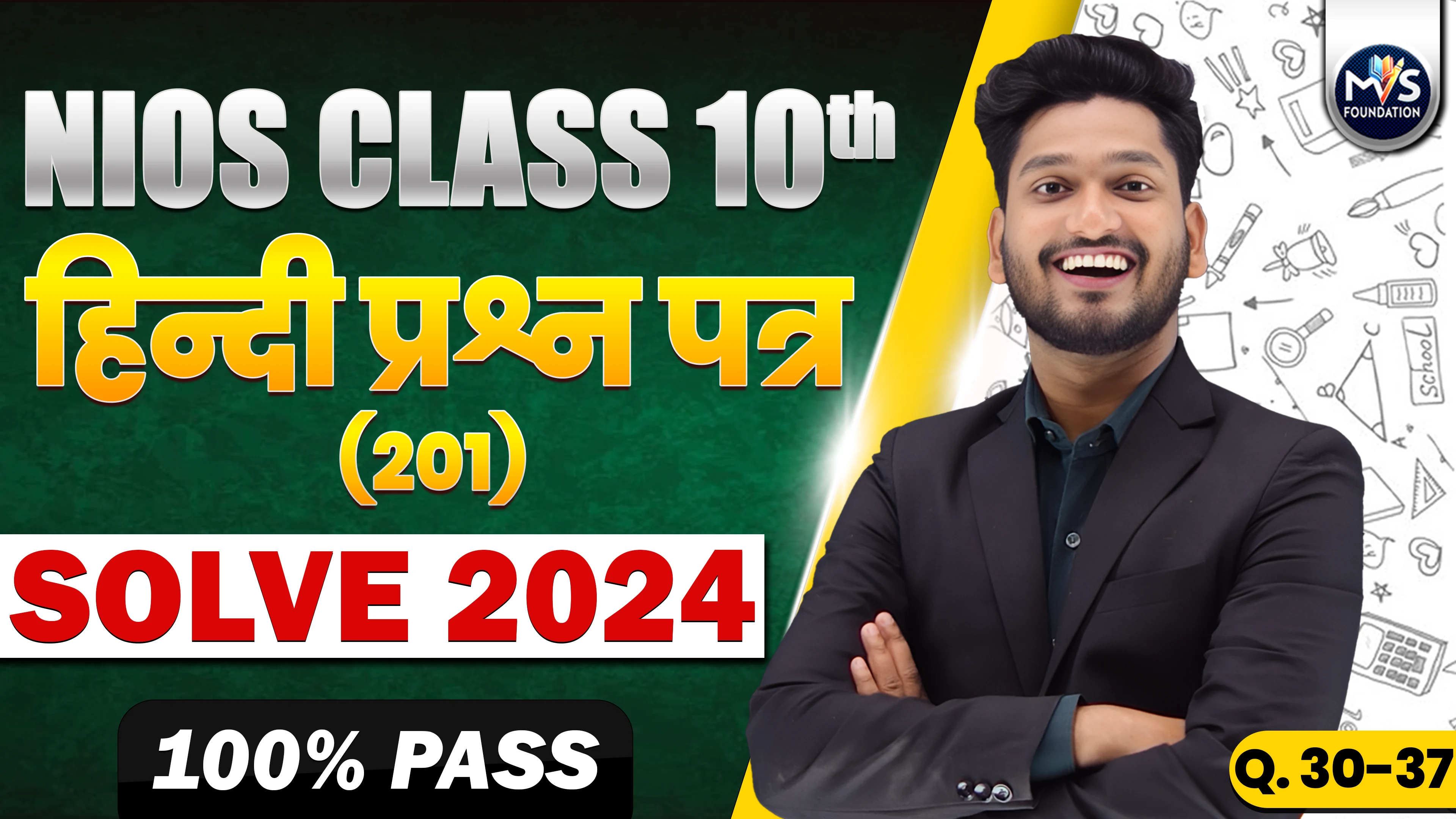
NIOS Question PAPER 2024 Solution
Question 30-37
HINDI (201)
30. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए –
(क) आपके विचार में आज़ादी का वास्तविक अर्थ क्या है?
उत्तर - आज़ादी का मतलब है, बिना किसी बाधा के अपनी मर्ज़ी से सोचना, बोलना, काम करना, और जीना। आज़ादी का मतलब सिर्फ़ अधिकारों का लाभ उठाना नहीं है, बल्कि समाज और देश के प्रति ज़िम्मेदारी निभाना भी है।
(ख) 'आह्वान' कविता के कवि ने 'उद्बोधन और 'आह्वान' में क्या अंतर बताया है?
उत्तर - 'आह्वान' कविता के कवि ने बताया है कि किसी व्यक्ति, समूह अथवा समाज को संबोधित करना उद्बोधन कहलाता है। कवि देश की जनता का उद्बोधन कर रहा है। जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करने की प्रेरणा दी जाती है, तो उसे आह्वान कहते हैं।
(ग) 'बूढ़ी पृथ्वी का दुःख' कविता में कवयित्री ने किन विषयों पर चिंता प्रकट की है?
उत्तर - 'बूढ़ी पृथ्वी का दुःख' कविता में कवयित्री ने घटते वृक्ष, हरियाली की कमी, नदियों में घटते पानी और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने पहाड़ों के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार और पर्यावरण पर इसके विनाशकारी प्रभाव को भी उजागर किया है।
(घ) कबीर के अनुसार एक व्यक्ति में ऊँचे कुल में जन्म लेने के साथ-साथ और क्या होना आवश्यक है?
उत्तर - कबीर के अनुसार, केवल ऊँचे कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। बल्कि व्यक्ति में अच्छे कर्म, ज्ञान और सद्गुणों का होना भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति में अच्छे आचरण और विनम्रता नहीं है, तो ऊँचे कुल का होना व्यर्थ है।
31. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए -
(क) 'अंधेर नगरी' नाटक में दिखाए गए परिवेश का उल्लेख कीजिए।
उत्तर - 'अंधेर नगरी' नाटक में बाजार, जंगल और राजभाषा के दृश्य प्रमुख है, बाजार के दृश्य के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति का पता चलता है।
(ख) 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी के इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए - "कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा!"
उत्तर - 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी में प्रेमचंद व्यंग्य करते हुए कहते हैं- कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। इसका तात्पर्य है कि मिरज़ा और मीर अपनी शतरंज की लत में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें लखनऊ की त्रासदी और परिवार की चिंता का कोई एहसास नहीं होता।
(ग) लेखक ने राजकुमार को सुखी राजकुमार क्यों कहा है?
उत्तर - राजकुमार का नाम सुखी इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में सुखी था जो आनंद-महल में रहता था। जो कभी किसी दुख का सामना नहीं किया। साथ ही, कभी किसी का दुख नहीं देखा।
(घ) 'बहादुर ईमानदार है।‘ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर - बहादुर कहानी में जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, तो वाचक उसका बचाव करता है और बताता है कि उसने कभी भी किसी का सामान नहीं चुराया। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता है, जब कभी उसने दो-चार आने इधर-उधर पड़े देखे, तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए।
32. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए -
(क) बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक किन्हें अपनी गलतियों का अहसास होता है और क्यों?
उत्तर - बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक अपनी गलतियों का अहसास वाचक को होता है क्योंकी उसे लगता है कि अगर उसने बहादुर को मारा नहीं होता, तो बहादुर कभी नहीं भागता। वह बहादुर के भागने पर उतना दुखी नहीं है, जितना उसके भागने के कारण से दुखी है।
(ख) 'सुखी राजकुमार' कहानी में ईश्वर द्वारा राजकुमार और गौरैया को स्वर्ग में स्थान देने की बात से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है?
उत्तर - 'सुखी राजकुमार' कहानी में ईश्वर द्वारा राजकुमार और गौरैया को स्वर्ग में स्थान देने से कहानीकार यह दिखाना चाहते हैं कि आज के समाज में दया, त्याग और दूसरों की मदद जैसे अच्छे गुणों की अनदेखी की जाती है। कहानीकार समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की स्थिति को खत्म करने की बात करता है।
(ग) 'अंधेर नगरी' नाटक का कौन-सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों?
उत्तर - अंधेर नगरी' नाटक में महंत जी का किरदार सबसे अच्छा लगा क्योंकि वे एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे और लोभ-लालच में नहीं पड़ते थे।
33. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए -
नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है; अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र-शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाज़ा है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास - बिना सिखाये - आ जाती है, वह पशुत्व की घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से वस्तुएँ, मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं।
(क) उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए।
उत्तर - उपर्युक्त गद्यांश पाठ “नाखून क्यों बढ़ते है?” से लिया गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है।
(ख) गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर - गद्यांश का मूल भाव यह है कि मनुष्य का असली आदर्श संयम, आत्म-नियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मान है। लेखक का कहना है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से जो घृणा, हिंसा और पशुता होती है, वह उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, जिनका नियंत्रण करना ही उसकी असली पहचान है।
(ग) आज के परिवेश में नई पीढ़ी में सद्गुणों का विकास किन-किन उपायों द्वारा हो सकता है?
उत्तर - नई पीढ़ी में सद्गुणों का विकास शिक्षा, परिवार, समाज में प्रेरणादायक व्यक्तित्वों, स्वयंसेवी कार्य, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, आत्म-निर्भरता, अनुशासन, और प्रेरणादायक पुस्तकों के माध्यम से किया जा सकता है, जो उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करें।
अथवा
बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ-बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियाँ न लेकर अफ़ीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश गंजीफ़ा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है - वे दलीलें/ज़ोरों के साथ पेश की जाती थीं (इस सम्प्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए, अगर मिरज़ा सज्जाद अली और मीर रौशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती है?
(क) उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए।
उत्तर - यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी "शतरंज के खिलाड़ी" से लिया गया है।
(ख) इस गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर - गद्यांश में नवाबी संस्कृति के पतन का चित्रण किया गया है, जहाँ लोग कर्तव्यों की ओर ध्यान न देकर खेल, नशे और मनोरंजन में लिप्त थे। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में यह दिखाते हैं कि समाज अपने समय और संसाधनों को व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद कर रहा था, जो मानसिक और नैतिक पतन को दर्शाता है।
(ग) उपर्युक्त गद्यांश की भाषा-शैली पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर - प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों और पतनशीलता पर कटाक्ष करते हुए सरल, प्रवाहपूर्ण और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग उस समय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, "चौसर", "अफ़ीम", "गंजीफ़ा", आदि शब्द उस समय की नवाबी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
|
तो बच्चा! ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में हज़ार मन मिठाई मुफ़्त की मिले, तो किस काम की? यहाँ एक छन नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार-भर में कोई देस ही नहीं है। दो पैसा पास रहने ही मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। |
34. निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :
उत्तर -
तो बच्चा! ऐसी नगरी में रहना……………. नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा।
प्रसंग : प्रस्तुत प्रसंग ‘अंधेरी नगरी’ नाटक से लिया गया हैं, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक हैं। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार “भारतेंदु हरिश्चंद्र” हैं। इस नाटक में गुरु और उनके दो शिष्यों – गोबरधनदास और नारायणदास की कथा है। यहाँ गुरु (महंत) अंधेर नगरी की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को देखकर वहाँ से जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन उनका एक शिष्य (गोबरधनदास) ठहरने की जिद करता है।
व्याख्या : इन पंक्तियों में महंत जी अपने शिष्य गोबरधनदास को समझाते हैं कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, जहाँ चीजों का उचित मूल्य नहीं होता और शासन व्यवस्था अराजक होती है। 'टके सेर भाजी और टके सेर खाजा' का अर्थ यह है कि वहाँ हर वस्तु का मूल्य एक समान है, चाहे वह सस्ती हो या महंगी। इससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ का राजा या शासक अत्यंत मूर्ख और अन्यायी है। गुरु के अनुसार, ऐसे स्थान पर रहना विनाशकारी हो सकता है, चाहे वहाँ कितनी भी सुविधाएँ मिलें, क्योंकि वहाँ न्याय और नीति का कोई मूल्य नहीं होता। अतः वे अपने शिष्य से वहाँ से चलने को कहते हैं।
परंतु गोबरधनदास अपने गुरु की सलाह को नहीं मानता। वह कहता है कि ऐसी नगरी संसार में कहीं और नहीं मिलेगी, जहाँ केवल दो पैसे होने से भी पेट भर भोजन मिल सकता है। वह तत्कालिक लाभ और सस्ती वस्तुओं के लोभ में अंधेर नगरी में रहने का निर्णय लेता है, बिना यह सोचे कि ऐसी अनुचित व्यवस्था उसके लिए खतरा भी बन सकती है।
विशेष :
|
गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख-सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म-निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है! लेकिन, मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। |
अथवा
उत्तर -
गौतम ने ठीक ही कहा था ……………… बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था।
प्रसंग : प्रस्तुत अवतरण हिंदी निबंधकार हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध "नाखून क्यों बढ़ते हैं" से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने मनुष्यता, सहानुभूति, अहिंसा और सत्य जैसे मूल्यों पर प्रकाश डाला है। वे बताते हैं कि मनुष्य की विशेषता उसकी संवेदनशीलता और दूसरों के दुख-सुख को समझने की क्षमता में निहित है।
व्याख्या : प्रस्तुत पंक्तियों में हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून की चर्चा करते हुए मानवता, सभ्यता और प्राचीनता पर विचार किया है। वे बताते हैं कि मनुष्य में ही मनुष्यता का भाव होता है, जिसके कारण वह सबकी संवेदनाओं को समझता है। इसके साथ ही, स्वयं की समझ ही मनुष्य को एक मनुष्य बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, मनुष्यता के लिए मनुष्य में अहिंसा, सत्य और क्रोध से मुक्त होना ही वास्तव में उचित धर्म का स्त्रोत है। लेखक आगे कहते है कि मुझे इस बात पर आश्यर्च है कि ये नाखूनों की बढ़ोतरी मानव जीवन के विकास और उसके प्रतीकों के रूप वर्णित है, अर्थात मनुष्य के नाखून उसकी भयंकरता के प्रतीक है, जिसे देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ है।
विशेष :
35. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सार एक-तिहाई शब्दों में लिखिए -
प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है। कोई व्यापारी बनना चाहता है तो कोई सरकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर बनने की लालसा से प्रेरित है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया काम उच्च कोटि की संज्ञा नहीं पा सकता। स्वार्थ के पीछे तो संसार पागल है। लोग भूल गए हैं कि जीवन का रहस्य निष्काम सेवा है। जो व्यक्ति लालच से प्रेरित होकर काम करता है, वह कभी सुपरिणाम नहीं ला सकता। उससे समाज का कोई भला नहीं होता। निष्काम सेवा के द्वारा ही मनुष्य समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा सकता है। निष्काम सेवा के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। समाज और देश को उन्नति की ओर ले जाने का श्रेष्ठतम तथा सरलतम साधन यही है। हमारे संत कवियों तथा समाज सुधारकों ने इसी भाव से प्रेरित होकर अपनी चिंता छोड़ देश और समाज के कल्याण का रास्ता चुना। वे राष्ट्र और समाज के लिए बहुत कुछ कर पाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन अमर हो जाता है। वही मनुष्य महान है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे।
उत्तर - जीवन का उद्देश्य स्वार्थ से परे होना चाहिए। व्यक्ति को निष्काम सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वार्थपूर्ण कार्य समाज के भले के लिए नहीं होते। जो लोग दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, वही असली सफलता और महानता प्राप्त करते हैं। संतों और समाज सुधारकों ने इसी भावना से प्रेरित होकर समाज और देश के कल्याण के लिए कार्य किया। उनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित था, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।
36. किसी प्रतिष्ठित पत्र के संपादक को पत्र लिखकर नगर में डेंगू फैलने के कारणों की चर्चा करते हुए इससे निपटने की अपर्याप्त तैयारियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर -
सेवा में
संपादक
नवभारत टाइम्स (समाचार-पत्र)
दिल्ली
विषय - डेंगू फैलने के कारण
सविनय निवेदन है कि मैं आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से प्रशासन और नगरवासियों का ध्यान नगर में डेंगू की बढ़ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हर गली और मोहल्ले में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण नगर में जगह-जगह गंदगी, जलभराव और मच्छरों के पनपने के अनुकूल वातावरण का होना है। इसके अलावा, खुले में कूड़े के ढेर, नालों की सफाई की कमी, और नियमित फॉगिंग न होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर, दवाएँ और खून उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, लोगों को डेंगू से बचाव के तरीके बताने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
मैं आपके माध्यम से प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वे शीघ्र उपाय अपनाएँ। जैसे - सफाई अभियान को चलाना, फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव करना आदि। आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर अपने प्रतिष्ठित पत्र में स्थान प्रदान कर प्रशासन और नागरिकों को इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करें।
धन्यवाद
आपका भवदीय
अंकित
दिनांक : 28/01/2025
अथवा
अपनी वायुयान-यात्रा के आनंद का वर्णन करते हुए अपने मित्र/सखी को पत्र लिखिए।
उत्तर -
प्रिय मित्र/सखी,
नमस्ते! आशा है तुम स्वस्थ और खुशहाल होगी। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें अपनी वायुयान-यात्रा के अनुभव के बारे में बताना चाहती हूं। यह यात्रा सच में अद्वितीय थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे महसूस कर सको।
जैसे ही मैंने विमान में प्रवेश किया, मुझे एक अजीब सी उत्सुकता महसूस हुई। सीट पर बैठते ही मैं खिड़की से बाहर देखने लगी, और फिर जो दृश्य सामने आया, वह अविस्मरणीय था। आकाश में उड़ते हुए, नीचे ज़मीन की छोटी-छोटी बातें, जैसे घर, सड़कें, पेड़, सब कुछ छोटे खिलौनों जैसा लगता था। हवा की नमी और हल्की सी ठंडक ने यात्रा को और भी सुखद बना दिया।
विमान के अंदर का माहौल भी बहुत आरामदायक था। एयरहोस्टेस ने बहुत विनम्रता से स्वागत किया और हमें भोजन भी परोसा। आस-पास के लोग बहुत शांत थे, और विमान की हलचल भी बहुत कम थी, जिससे मुझे यात्रा का हर क्षण बहुत शांति और आरामदायक अनुभव हुआ। जब विमान ऊँचाई पर पहुँच गया, तो मैं खिड़की से सूरज की रौशनी और बादलों के बीच की रंगीन छायाएँ देखती रही। यह दृश्य सच में जादुई था।
यात्रा के दौरान समय बहुत जल्दी बीत गया, और जैसे ही हम गंतव्य पर पहुँचे, मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष था। यह अनुभव मेरे लिए एक नई और रोमांचक शुरुआत जैसा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी यात्रा के अनुभव से आनंद मिलेगा।
तुम्हारी मित्र,
अनिशा ठाकुर
37. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए :
(क) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
(ख) भारतीय गाँव
(ग) कंप्यूटर : आज की आवश्यकता
(घ) मेले का दृश्य
उत्तर -
(क) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य योग के महत्व को दुनिया भर में फैलाना और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और तभी से यह दिन पूरी दुनिया में योगाभ्यास के महत्व को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
योग भारत की प्राचीन विद्या है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके माध्यम से हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन और आत्मा के बीच सामंजस्य भी स्थापित करते हैं। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम शरीर को लचीला बनाते हैं, रक्तसंचार को बेहतर करते हैं और तनाव को कम करते हैं। योग का नियमित अभ्यास मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है, जो हमारे जीवन को अधिक उत्पादक और संतुष्टिपूर्ण बनाता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन दुनिया भर में हजारों लोग एक साथ मिलकर योग करते हैं। इस दिन विभिन्न देशों में योग शिविर और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, जहाँ विशेषज्ञ योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इसके माध्यम से न केवल योग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को बताया जाता है, बल्कि यह भी एक वैश्विक संदेश भेजता है कि योग किसी एक देश या संस्कृति की नहीं, बल्कि समूची मानवता की धरोहर है।
आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में योग एक उत्तम साधन बन गया है, जो हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। योग दिवस न केवल एक दिन के आयोजन के रूप में अपनाया जाता है, बल्कि यह हर दिन योग को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है।
✅ अब सभी सटीक Question & Answer पाने के लिए यहाँ क्लिक करें!

1 Response