
Get in Touch
We will get back to you within 24 hours.
Welcome to MVS Blog
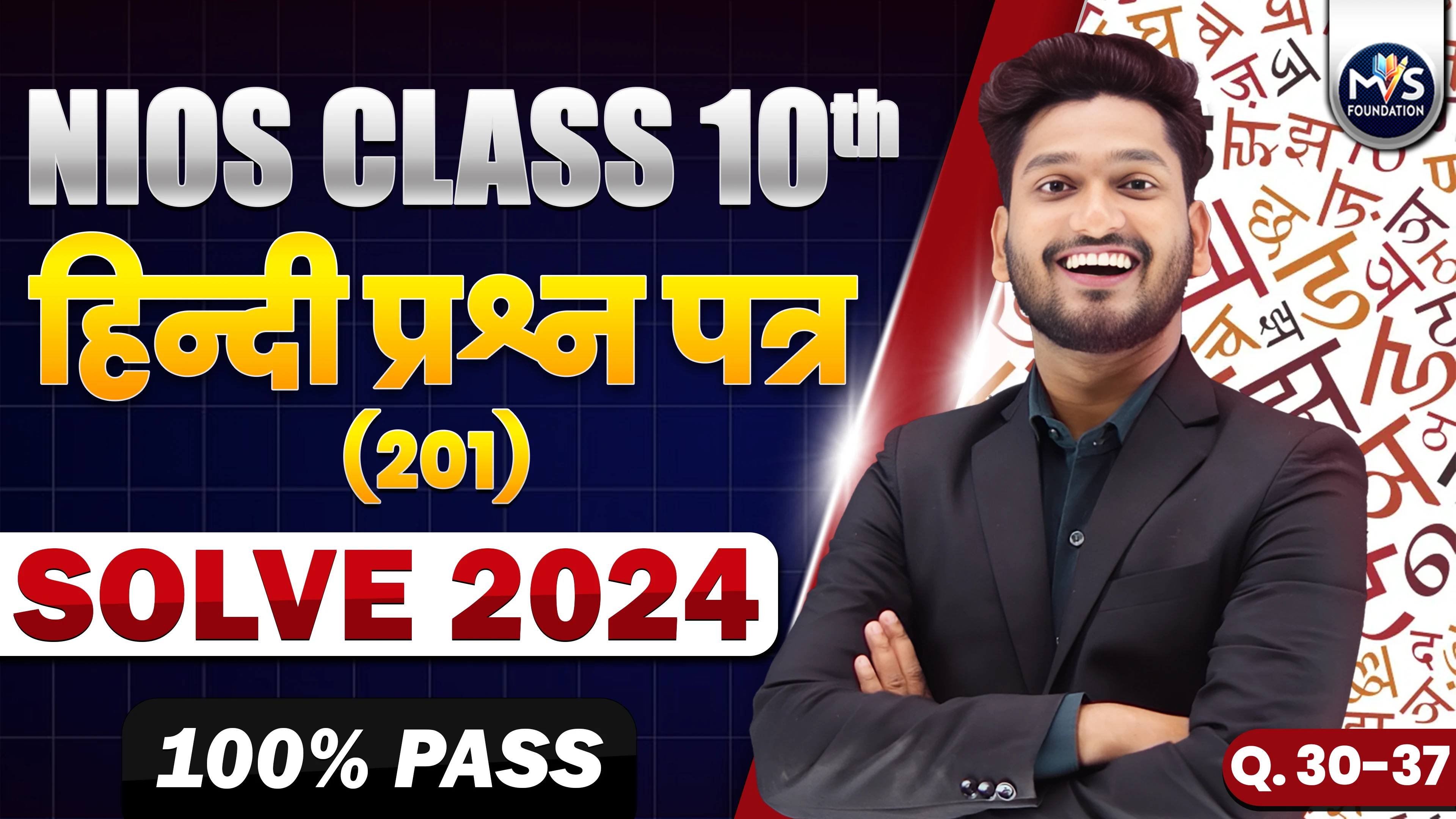
NIOS Question Paper 2024 Solution
HINDI (201)
Question 30-37
30. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए।
(i) कवि 'वृंद' के अनुसार अभ्यास करने का क्या अर्थ होता है ?
उत्तर - कवि ‘वृंद’ के अनुसार, अभ्यास करने का अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानी बन जाता है; ठीक उसी तरह, जैसे रस्सी के बार-बार रगड़ने से पत्थर पर निशान बन जाता है। इसीलिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास करने से इंसान अपने कौशल को निखारता है और लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
(ii) 'आह्वान' कविता के अनुसार सुख और शांति कैसे आएगी ? 'चंद्रगहना से लौटती बेर' कविता के संदर्भ में लिखिए।
उत्तर - 'आह्वान' कविता के अनुसार, 'चंद्रगहना से लौटती बेर' की तरह सरल, ग्रामीण जीवन में समर्पण, श्रम और प्रकृति से जुड़ाव से सुख-शांति प्राप्त होती है, जहां सादगी और संतुलन प्रमुख हैं।
(iii) नगरों की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए अधिक उर्वर क्यों माना गया है ?
उत्तर - नगरों की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए अधिक उर्वर माना गया है क्योंकि ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर व्यावसायिक हो गए हैं और वहाँ प्यार की भावना कम होती है। वहीं, ग्रामीण अंचल की भूमि प्रेम-प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है, जहाँ प्रकृति के हर हिस्से में प्रेम झलकता है। प्राकृतिक जीवनशैली मन को शांति और सच्चे प्रेम के लिए प्रेरित करती है।
(iv) 'चंद्रगहना से लौटती बेर' कविता के संदर्भ में लिखिए कि क्या प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग करना हमारा अधिकार है ? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।
उत्तर - 'चंद्रगहना से लौटती बेर' कविता के संदर्भ में, प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग करना हमारा अधिकार नहीं है। कविता प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के सरल पहलुओं को सम्मानित करती है। इसका संदेश है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। स्वार्थी और अति उपयोग से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे जीवन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सम्मान करना चाहिए।
31. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए।
(i) बहादुर के, व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए।
उत्तर - बहादुर का व्यक्तित्व :
(ii) 'सुखी राजकुमार' कहानी के आधार पर राजकुमार के जीवन-काल और प्रतिमा बनने के बाद के राजकुमार के व्यक्तित्व की तुलना कीजिए और बताइए कि आपको कौन-सा रूप पसंद है और क्यों ?
उत्तर - 'सुखी राजकुमार' कहानी में राजकुमार का जीवन प्रारंभ में भौतिक सुख-संपत्ति और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। वह अपने महल में खुश रहने के लिए अंधेरे में छिपे दुखों को नहीं देखता था। पर जब उसकी प्रतिमा बनती है, तो वह दुनिया की पीड़ा और दुख को महसूस करता है। इस रूप में, वह दयालु और संवेदनशील बन जाता है।
हमें राजकुमार का प्रतिमा रूप पसंद है, क्योंकि वह समाज के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाता है। उसका निर्णय दूसरों की मदद करना दर्शाता है, जो असली खुशी और मानवता की पहचान है।
(iii) 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' पाठ के संदर्भ में लिखिए कि - गाँधी जी किस प्रकार के सुखों को मानव-जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे ?
उत्तर - गाँधी जी ने ऐसे सुखों को मानव-जाति के लिए श्रेष्ठ माना जो आत्मा की शांति और सच्ची संतोषजनकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने भौतिक सुख और विलासिता के बजाय सादगी, दया, और नैतिकता पर आधारित सुखों को महत्वपूर्ण माना, जो समाज की भलाई और व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं।
(iv) मूल्यवान वस्तुएँ सस्ती होने पर भी महंत ने अंधेर नगरी में रहने के लिए मना क्यों किया ?
उत्तर - महंत ने अंधेर नगरी में रहने से मना इसलिए किया क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका गलत था। महंत ने देखा कि वहां का राजा मूर्ख है और प्रजा भी मूर्ख है। वहां किसी वस्तु का मूल्य उसके गुण से न तय होकर बल्कि सभी का मूल्य एक ही था। महंत को लगा कि वहां चारों ओर अव्यवस्थता फैली हुई है इसलिए उन्होंने तुरंत राज्य छोड़ने का फ़ैसला लिया।
✅ सभी सटीक Question & Answer पाने के लिए यहाँ क्लिक करें!
32. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 20-25 शब्दों में लिखिए।
(i) आप ऐसे कौन से दो मानवीय मूल्य को अपनाना चाहेंगे जिससे आपका भविष्य निर्मित हो। वर्णन कीजिए।
उत्तर - हम दो मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहेंगे :
(ii) 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी को लिखने के पीछे प्रेमचन्द का क्या उद्देश्य था ?
उत्तर - प्रेमचंद जी 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मिरज़ा और मीर जैसे लोग यदि अपना दिमाग देश के बचाव में लगाते तो गुलामी से बचा जा सकता था। लेकिन 'शतरंज के खिलाड़ी' के दोनों खिलाड़ी देश और समाज की उपेक्षा करके शतरंज में ही व्यस्त रहते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में भी स्वाधीनता-आंदोलन में लगे नेताओं और उनके पीछे चलने वाली जनता को यह सीख दी कि देश और स्वाधीनता के हित में हमें आराम तथा विलास को छोड़ देना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए।
(iii) समाचारों की चयन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर - समाचारों का चयन अख़बारों में एक सामूहिक प्रक्रिया है। संवाददाता अपने क्षेत्रों से ख़बरें लाते हैं और सरकारी व गैर-सरकारी एजेंसियाँ, जैसे पी.टी.आई. और रायटर, भी समाचार भेजती हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएँ और विभाग प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फ़ैक्स या ई-मेल के द्वारा अख़बारों के दफ़्तरों में भेजते हैं। इस तरह अख़बारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हज़ारों समाचार एकत्र हो जाते हैं। लेकिन, अख़बारों में स्थान सीमित होता है, ऐसी स्थिति में उनके महत्त्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है। समाचारों का चयन पहले संवाददाता खुद अपने विवेक से करते हैं। फिर प्रमुख संवाददाता उन समाचारों की छँटनी करते हैं। इसके बाद, पृष्ठ की जगह को ध्यान में रखते हुए, समाचार-संपादक और प्रमुख संपादक मिलकर निर्णय लेते हैं।
33. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(i)
गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंगरलियाँ मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख माँग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे ज़र्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे दो बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं - "भागो यहाँ से!" चौकीदार बोला और वे बारिश में भीगते हुए चल दिए।
(क) पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर - पाठ का नाम : ‘सुखी राजकुमार’
लेखक का नाम : ऑस्कर वाइल्ड
(ख) लेखक ने इस गद्यांश में धनी और निर्धन वर्ग के जीवन और व्यवहार की किन विषमताओं को दर्शाया है ?
उत्तर - लेखक ने इस गद्यांश में धनी और निर्धन वर्ग के जीवन की विषमताओं को बड़ी ही मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। अमीर लोग अपने महलों में खुशियों का आनंद ले रहे हैं और तकलीफों से बेखबर अपनी मस्ती में मग्न हैं जबकि गरीब लोग भीख माँगने को मजबूर हैं। गरीब बच्चों की स्थिति और भी दर्दनाक दिखाई गई है, जो भूख और ठंड से तड़प रहे हैं। यह समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता को उजागर करता है।
(ग) आपकी राय में गौरैया सुखी राजकुमार के सान्निध्य में क्या सीखती है ?
उत्तर - गौरैया जब सुखी राजकुमार के सान्निध्य मे होती है, तो वह उसकी सुखी-सुविधाओ और आनंदमय जीवन को देखकर यह सीखती है कि दुनिया मे बहुत से लोग ऐसे है जो केवल भौतिक सुख मे लिप्त है। इसके विपरीत, गरीब और असहाय लोगों की स्थिति देख कर उसे सामाजिक असमानता और दया की महत्वपूर्णता का अहसास होता है। वह समझती है की सच्ची खुशी और संतोष सिर्फ भौतिक समृद्धि मे नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने मे भी है।
अथवा
(ii)
बात यह है कि कल कोतवाल को फाँसी का हुक्म हुआ था। जब फाँसी देने को उनको ले गए, तो फाँसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज़ किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फाँसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फाँसी दें।
(क) पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर - पाठ का नाम : ‘अंधेर नागरी’
लेखक का नाम : भारतेंदु हरिश्चंद्र
(ख) पाठ के इस अंश में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है ?
उत्तर - इस गद्यांश में न्यायिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है, जहाँ वास्तविक अपराधी को सजा देने के बजाय किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है। कहानी में कोतवाल को फाँसी दिए जाने की बात है, लेकिन जब वह फाँसी के फंदे में फिट नहीं होते, तो न्याय के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को फाँसी देने का निर्णय लिया जाता है। इससे न्याय प्रक्रिया की विडंबना और उसके असंगत तरीके को उजागर किया गया है, जहाँ केवल सजा देने के लिए कोई भी व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही वह निर्दोष हो।
(ग) गद्यांश की भाषा-शैली लिखिए।
उत्तर - गद्यांश की भाषा-शैली :
निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए -
(i)
एक दिन दोनों मित्र मसजिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मिरज़ा साहब उन्हें किश्त-पर-किश्त दे रहे थे। इतने में कम्पनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फ़ौज थी, जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी।
उत्तर -
एक दिन दोनों ........... आ रही थी।
प्रसंग - प्रस्तुत गद्यांश कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ से लिया गया है जिसके रचयिता “प्रेमचंद जी” है। यह घटना एतिहासिक संदर्भ मे 1857 के विद्रोह के समय की है, जब भारतीय राज्य धीरे-धीरे अंग्रेजों के अधीन आ रहे थे।
व्याख्या - इस गद्यांश में दो मित्र, मीर और मिर्जा, मस्जिद के खंडहर में शतरंज खेलते समय अपने खेल में इतने लीन हैं कि उन्हें लखनऊ पर आ रही ब्रिटिश सेना की ओर ध्यान नहीं है। मीर कमजोर स्थिति मे है और मिरज़ा उसे लगातार मात दे रहे है। इस कहानी मे यह दर्शाया गया कि किस तरह देश पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वे लोग अपनी खेल-सुख में इतने व्यस्त हैं कि वास्तविकता से बेखबर हैं। यह स्थिति अव्यवस्था और सामाजिक उदासीनता को भी दर्शाती है।
विशेष -
अथवा
(ii)
मैं अपने को बहुत ऊँचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान-बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मुहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं सीधे मुँह किसी से बात नहीं करता। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली-सी शरारत पर डाँट डपट देता था।
उत्तर -
मैं अपने को ........... डपट देता था।
प्रसंग - प्रस्तुत गद्यांश “बहादुर” कहानी से लिया गया है जिसके रचयिता अमरकांत है। गद्यांश में एक व्यक्ति का आत्ममुग्ध और अहंकारी स्वभाव दिखाया गया है। वह अपने परिवार और संबंधियों की स्थिति पर गर्व महसूस करता है और इसी गर्व के कारण मुहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगता है।
व्याख्या - इस गद्यांश में व्यक्ति की अहंकारी भावना का चित्रण किया गया है। वह अपने परिवार और संबंधियों की शान पर गर्व महसूस करता है और अपने आप को ऊँचा मानता है। इस गर्व ने उसे मुहल्ले के लोगों को तुच्छ समझने पर मजबूर कर दिया है। वह दूसरों से सीधे मुह बात नहीं करता, उन्हें नजरअंदाज करता है और मामूली बातों पर भी कठोरता दिखाता है। यह अहंकार उसकी संवेदनशीलता को कम कर देता है और उसे दूसरों के प्रति अमानवीय बना देता है।
विशेष -
✅ सभी सटीक Question & Answer पाने के लिए यहाँ क्लिक करें!
35. निम्नलिखित गद्यांश का सार एक तिहाई शब्दों में लिखिए।
धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान की जड़ में पाप-भाव पलता है। हमें शरीर में प्राण रहने तक दया-भाव को त्यागना नहीं चाहिए। संसार का प्रत्येक धर्म दया और करूणा का पाठ पढ़ाता है। परोपकार की भावना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। यह एक सात्विक-भाव है। परोपकार की भावना रखने वाला न तो अपने-पराए का भेदभाव रखता है और न ही अपनी हानि की परवाह करता है। दयावान किसी को कष्ट में देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसकी आत्मा उसे मज़बूर करती है कि वह दुखी प्राणी के लिए कुछ करे। गुरुनानक, गौतम बुद्ध, महावीर जैसे संतों ने मानव-जाति के कल्याण की कामना करते हुए कर्म किए। ऐसे ही लोगों के बल पर आज हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। अगर कोई किसी पर अत्याचार करे या बेकसूर को यातना दे, तो हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम बेकसूर का सहारा बनें। न्याय व धर्म की रक्षा करना सदा से धर्म है। दया-भाव विहीन मनुष्य भी पशु समान ही होता है। जो दूसरों की रक्षा करते हैं, वे इस सृष्टि को चलाने में भगवान की सहायता करते हैं। धर्म का मर्म ही दया है। दया-भाव से ही धर्म का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है।
उत्तर - गद्यांश का सार
धर्म हमें दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है, जो मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। दयालु व्यक्ति किसी को कष्ट में देखकर मदद करने के लिए प्रेरित होता है। गुरुनानक, गौतम बुद्ध और महावीर जैसे संतों ने मानव कल्याण के लिए कार्य किए। धर्म का असली अर्थ दया है और जो दूसरों की रक्षा करते हैं, वे भगवान के काम में सहायक होते हैं। दया-भाव से ही धर्म का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है।
36. अपने मोहल्ले में 'जल संकट' से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार-पत्र के संपादक को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए।
उत्तर -
सेवा में
संपादक महोदय,
दैनिक भास्कर (समाचार-पत्र)
आगर-मालवा, मध्य प्रदेश
विषय : जल संकट से उत्पन्न कठिनाइयों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र।
महोदय,
मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के माध्यम से अपने मोहल्ले में जल संकट की गंभीर समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विगत कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति अत्यधिक कम हो गई है। पानी की कमी के कारण पीने, खाना पकाने और साफ-सफाई जैसे आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई बार पानी की टैंकर समय पर नहीं पहुँचतीं, जिससे दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएँ पूरी करना कठिन हो रहा है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है। ताकि हमारे मोहल्ले के निवासी सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके अलावा जल संचयन और पाइपलाइन मरम्मत जैसे स्थायी समाधान की आवश्यकता है। कृपया इस मुद्दे को उजागर कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करें।
धन्यवाद
भवदीय/आपका
सोनिया
[आगर-मालवा, मध्य प्रदेश]
दिनांक – 12/02/2024
अथवा
अपने मित्र को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए जिसमें सिनेमा देखने के दुर्व्यसन से बचने के लिए सलाह दी गई हो।
उत्तर -
विजय नगर, सेक्टर - 12,
इंद्रा कॉलोनी, दिल्ली
5-3-2024
प्रिय मित्र
नमस्ते,
आशा है, तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मुझे पता चला है कि तुम सिनेमा देखने के दुर्व्यसन में पड़ रहे हो। सिनेमा मनोरंजन का अच्छा माध्यम है, लेकिन अधिक समय और पैसा बर्बाद करने से पढ़ाई और जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें सलाह दूँगी कि सिनेमा देखने की आदत को नियंत्रित करो और अपने समय का सदुपयोग पढ़ाई, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में करो। सच्ची सफलता मेहनत और अनुशासन से ही मिलती है।
तुम्हारा शुभचिंतक,
मोहन
37. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए।
(i) शहरीकरण से बढ़ता प्रदूषण
(ii) जहाँ चाह वहाँ राह
(iii) समय प्रबंधन का महत्त्व
(iv) भारत के बदलते गाँव
उत्तर -
(i) शहरीकरण से बढ़ता प्रदूषण
शहरीकरण, यानि शहरों का तेजी से विकास, आधुनिक जीवनशैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च जीवन स्तर और सुविधाओं की लालसा ने लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आकर्षित किया है। हालांकि, शहरीकरण के कारण कई सकारात्मक बदलाव आए है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिनमे सबसे प्रमुख समस्या प्रदूषण है। बढ़ते शहरीकरण के कारण वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण जैसे मुद्दे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे है।
वायु प्रदूषण : शहरी क्षेत्रों मे वाहनों की बढ़ती संख्या, उद्योगों से निकलने वाला धुआँ और निर्माण कार्यों के कारण वायु प्रदूषण से तेजी से वृद्धि हो रही है। वाहन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिलकर हवा को दूषित करती हैं। शहरों में जनसंख्या की वृद्धि के कारण ट्रैफिक जाम एक सामान्य दृश्य हो गया है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या और भी विकट हो गई है। शहरी क्षेत्रों में फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे निकली हानिकारक गैसें और धूल कण वायुमंडल में मिलकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। यह समस्या सांस संबंधी बीमारियों, हृदय रोगों और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है।
जल प्रदूषण : शहरीकरण के कारण जल प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में बहाया जाता है, जिससे ये जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में कूड़े-कचरे का उचित निस्तारण न होने के कारण यह कचरा जल निकायों में मिल जाता है, जिससे इनका पानी पीने और कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसके अलावा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री भी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं, जो न केवल जल जीवों के लिए हानिकारक है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
ध्वनि प्रदूषण : शहरों में बढ़ती जनसंख्या के साथ ध्वनि प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ट्रैफिक, उद्योगों, निर्माण कार्यों और लाउडस्पीकरों के अत्यधिक प्रयोग से ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा से काफी अधिक हो जाता है, जिससे मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ध्वनि प्रदूषण का बच्चों, बूढ़ों और बीमार व्यक्तियों पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
भूमि प्रदूषण : शहरीकरण के साथ-साथ भूमि प्रदूषण की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से निकलने वाला मलबा, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कचरे, और घरेलू कचरे का उचित निस्तारण न होने के कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके अलावा, प्लास्टिक, धातु और अन्य अपशिष्ट पदार्थों की अत्यधिक मात्रा भूमि में जाकर मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
समाधान : शहरीकरण से उत्पन्न प्रदूषण की समस्याओं को रोकने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्योगों को पर्यावरणीय नियमों का पालन करना चाहिए और उनके द्वारा निकाले जाने वाले कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए। इसके साथ ही, स्वच्छता और सफाई के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि कचरा जल और भूमि को दूषित न कर सके। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पेड़ हवा को शुद्ध करने का प्राकृतिक साधन हैं। सरकार को भी कड़े कानून बनाकर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए और हरित ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए।
(iv) भारत के बदलते गाँव
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सदियों से भारतीय गाँव अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, कृषि आधारित जीवनशैली और सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। परंतु समय के साथ, तकनीकी प्रगति, शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव से गाँवों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।आज के गाँव पहले की तुलना में काफी बदल चुके हैं, जिनमें जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
कृषि में बदलाव : भारत के गाँवों में कृषि मुख्य आजीविका का साधन रही है, लेकिन अब कृषि के तरीकों में बड़े बदलाव आ गए हैं। पारंपरिक कृषि पद्धतियों की जगह अब आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों ने ले ली है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग आम हो गया है, जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ी है। पहले किसान प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर रहते थे, पर अब उर्वरकों, कीटनाशकों और हाईब्रिड बीजों का उपयोग बढ़ गया है।अब किसानों को इंटरनेट के माध्यम से नई-नई जानकारियाँ और बाजार के रुझान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसने किसानों को बेहतर फसल प्रबंधन और फसल बेचने के नए अवसर दिए हैं। हालांकि, इस तकनीकी बदलाव से छोटे किसानों को कभी-कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन उपकरणों और साधनों का खर्च उठाना उनके लिए कठिन हो जाता है।
शिक्षा और जागरूकता : आज के गाँवों में शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। गाँवों में पहले जहाँ केवल कुछ लोग ही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, अब अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हैं। सरकारी प्रयासों और नीतियों के तहत गाँवों में स्कूलों की संख्या बढ़ी है, और शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है। डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट ने ग्रामीण बच्चों के लिए नए अवसर खोले हैं। महिलाएँ भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, जो गाँवों में सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। इससे गाँवों में जागरूकता और आत्मनिर्भरता का माहौल बना है।
स्वास्थ्य सुविधाएँ : स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गाँवों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पहले जहाँ छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को शहरों की ओर रुख करना पड़ता था, अब सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों से गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ और दवाइयाँ अब गाँवों तक आसानी से पहुंचाई जा रही हैं। मोबाइल क्लीनिक और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को आसान बना दिया है।
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन : गाँवों में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहले जहाँ जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादी सोच का बोलबाला था, अब धीरे-धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। शिक्षा और जागरूकता ने सामाजिक भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग अब एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रहते हैं और परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी है। हालाँकि, परंपरागत त्यौहार, रीति-रिवाज और सामूहिक आयोजन अभी भी गाँवों की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं।
भारत के गाँव आज तेज़ी से बदल रहे हैं, और यह बदलाव गाँवों को आत्मनिर्भर, आधुनिक और सशक्त बना रहा है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक संरचना में आए परिवर्तन गाँवों को नए आयाम दे रहे हैं। हालाँकि चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं, लेकिन यदि इन्हें सही तरीके से संबोधित किया जाए, तो आने वाले समय में भारत के गाँव देश के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
✅ सभी सटीक Question & Answer पाने के लिए यहाँ क्लिक करें!

0 Response