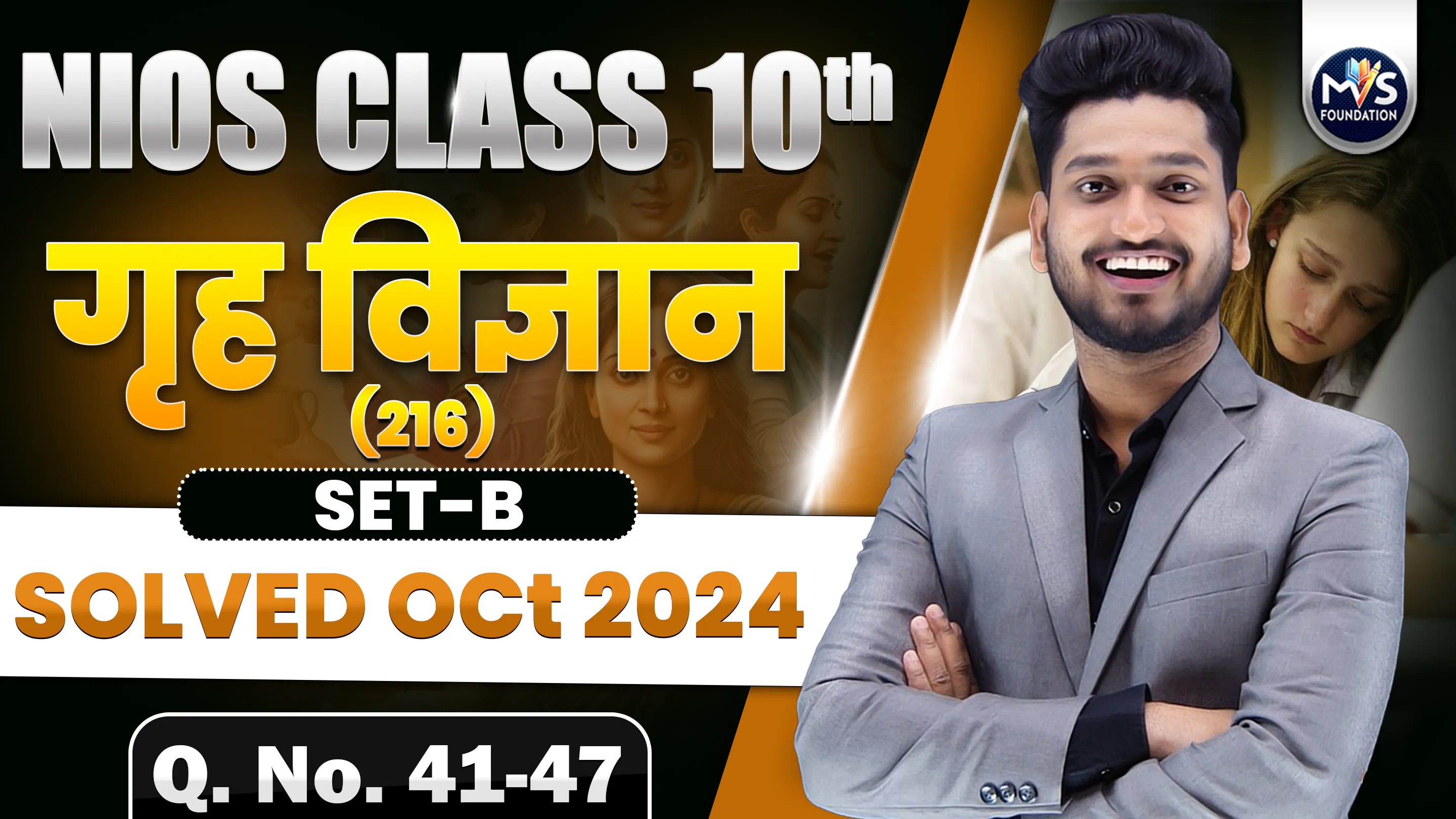NIOS Question Paper OCT 2024 SET B
गृह विज्ञान (216) - खण्ड 'ब' (Section B) | हिंदी में
Question 41-47
41. खाद्य संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? चार कारण बताइये।
उत्तर - खाद्य संरक्षण : "वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है"।
खाद्य संरक्षण के चार महत्वपूर्ण कारण है :
- संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है।
- संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है।
- संरक्षित भोजन को उन स्थानों पर भेजना जहाँ इन्हें उगाया नहीं जाता है।
- खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुगमता से हो जाता है।
42. सुलभ शौचालय लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? इसके कोई छः कारण लिखिए।
उत्तर - सुलभ शौचालय के लोकप्रिय होने के छः कारण इस प्रकार हैं :
- साफ-सफाई और स्वच्छता : सुलभ शौचालयों में नियमित साफ-सफाई और देखभाल की जाती है, जिससे स्वच्छता सुनिश्चित होती है।
- सुलभता और पहुंच : ये शौचालय सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होते हैं।
- कम लागत और किफायती शुल्क : सुलभ शौचालयों का उपयोग मामूली शुल्क पर किया जा सकता है, जिससे सभी वर्गों के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण : खुले में शौच की समस्या को कम करने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में ये शौचालय सहायक हैं।
- महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ : सुलभ शौचालयों में महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, जैसे अलग से शौचालय, पानी की सुविधा और रैंप।
- रोजगार सृजन : सुलभ शौचालयों में सफाई और रखरखाव के लिए स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे सफाईकर्मियों, प्रबंधकों और देखरेख करने वालों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होते हैं।
अथवा
किसी भवन को बनाने के लिए स्थल पर किन छः विशेषताओं की जाँच की जाती है?
उत्तर - भवन निर्माण के लिए स्थल पर निम्नलिखित छः विशेषताओं की जाँच की जाती है :
- आस-पास का वातावरण : भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ स्वच्छ, हरा-भरा और विकासशील वातावरण हो। साथ ही सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय और बाजार जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों।
- भौतिक विशेषताएँ : स्थल का चयन करते समय एक खुले क्षेत्र में घर का चयन करना चाहिए। घर भारी यातायात के समीप नहीं होना चाहिए। यातायात के समीप होने से वायु व ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- मृदा की प्रकृति : भवन की नींव मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है इसलिए इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। मजबूत नींव के लिए मृदा सतह से 2 से 5 फीट नीचे तक ठोस होनी चाहिए तभी मजबूत नींव पड़ सकती है।
- स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएँ : भवन निर्माण स्थल का चयन करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे स्थल का चयन किया जाना चाहिए जहाँ आसपास गंदगी, कूड़ा-करकट, जलभराव की समस्या न हो। ताकि कीटाणु, मक्खी-मच्छर और बीमारियों से बचाव हो सके।
- व्यावसायिक सुविधा : भवन स्थल ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बैंक, डाकघर और अन्य आवश्यक सेवाएँ पास में उपलब्ध हों। ये सुविधाएँ नजदीक होने से समय और ऊर्जा की बचत होती है और आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता मिलती है।
- सामाजिक वातावरण: घर के आस-पास का माहौल सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण होना चाहिए, जहाँ अच्छे पड़ोसी, सामुदायिक सुविधा और आपसी समझ का माहौल हो।
43. निर्जलीकरण के चरणों का क्रम बताइए।
उत्तर - निर्जलीकरण : निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थों से पानी या नमी दूर करना। उदाहरण के लिए, आलू के चिप्स, पापड़, केले के चिप्स, बड़ियाँ आदि खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण किया जाता हैं।
निर्जलीकरण के चरणों का क्रम :
चरण 1 : खाद्य पदार्थ को सुखाने व उन्हें संभाल कर रखने के लिए प्रयोग होने वाले सभी डिब्बों और प्लेटों आदि को साफ कर लें तथा उन्हें धूप में सुखा लें। इन डिब्बों के ढक्कन वायुरोधी होने चाहिए।
चरण 2 : सुखाने से पहले सब्जियों और फलों को धो लें। आवश्यक हो तो उन्हें काट लें। डंठल, बीज, छिलके हटा लें। यदि कोई सड़ा गला भाग हो तो उसे निकाल दें।
चरण 3 : सब्जियों को विवर्ण (blanch) कर लें अर्थात उन्हें उबलते हुए पानी में डालें। विवर्ण करने का समय फल/सब्जियों की कठोरता पर निर्भर करता है। वे जब गर्म हो जाएँ तब उन्हें निकाल लें। विवर्ण करने की प्रक्रिया से एँजाइमों की गतिविधियों में कमी आती है।
चरण 4 : सब्जियों को 5-10 मिनट के लिए नमक और पोटैशियम मेटाबाईसल्फाइट (KMS) युक्त ठंडे पानी में डालें। इससे खाद्य पदार्थों का रंग काला नहीं पड़ता। हरी पत्तेदार सब्जियों और गहरे रंग की अन्य सब्जियाँ इस घोल में न डालें क्योंकि यह सब्जियों के रंग को ब्लीच करता है।
चरण 5 : सब्जियों को साफ कपड़े पर धूप में फैला दें। इन्हें धूल और मक्खियों से बचाने के लिए पतले वस्त्र से ढक दें।
चरण 6 : जब खाद्य पदार्थ सूख जाएँ (कड़ेपन की जांच करके देखें) तो इसे कमरे के सामान्य तापमान तक ठंडा कर लें। अब इन्हें वायुरोधी ढ़क्कन वाले डिब्बों में भर लें।
44. इस महीने सुचिता को बीमार होने के कारण 2,000 रुपये की दवाइयां खरीदनी पड़ी। उसे तीन-तीन तरीके सुझाइए जिससे वह
(i) अपनी आय बढ़ा सके और (ii) अपने खर्चे कम कर सके।
उत्तर -
(i) आय बढ़ाने के तीन तरीके :
- अपनी क्षमताओं, ज्ञान व कौशल के आधार पर कार्य करना। जैसे- ट्यूशन पढ़ाना, कपड़े सिलना, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएँ बनाना आदि।
- पार्ट टाइम कार्य करना।
- ओवर टाइम कार्य करना।
(ii) खर्चे कम करने के तीन तरीके :
- मौसम के अनुसार फल व सब्जियों की खरीदारी करें।
- भोजन को बर्बाद न करें व बाहर भोजन करने की आदत को कम करें।
- बिजली, पानी आदि पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करें।
45. मृदा प्रदूषण के कारण होने वाले किन्हीं दो स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान कीजिए। इस प्रदूषण को रोकने के लिए चार सुझाव दीजिए।
उत्तर - मृदा प्रदूषण के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम इस प्रकार हैं :
- हृदय रोग व कैंसर
- तंत्रिका संबंधी समस्याएं
मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए चार सुझाव :
- घर के कूड़े-कचरे का उचित निपटान होना चाहिए ताकि इस पर मक्खियाँ, मच्छर और कॉकरोच न पनप सकें। साथ ही, पर्यावरणसहिष्णु वस्तुओं का प्रयोग करें।
- खुले में शौच जाने के बजाय स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए।
- कीटनाशक तथा उर्वरकों का सीमित प्रयोग करना चाहिए।
- पेड़-पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें।
अथवा
प्रदूषित वायु में वृद्धि के छः संभवित कारण क्या हैं?
उत्तर - प्रदूषित वायु में वृद्धि के छः संभवित कारण :
- घरेलू ईंधन (लकड़ी, कोयला आदि) का जलना।
- पटाखों और आतिशबाजी का धुआँ।
- निर्माण कार्यों और सड़क धूल से उत्पन्न प्रदूषण।
- पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैसें होती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती हैं।
- फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण में वृदि करती हैं।
- विलायकों तथा स्प्रे पेंट के प्रयोग से भी पर्यावरण प्रदूषित होता हैं।
46. किशोरों की संज्ञानात्मक विशेषताओं के कोई पाँच उदाहरण दीजिए।
उत्तर - किशोरों की संज्ञानात्मक विशेषताओं के पाँच उदाहरण निम्नलिखित हैं :
- अमूर्त विचारधारा : इस स्तर पर, किशोर असंभव की भी कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे यह कहावत सुनते हैं कि चीता अपने शरीर के धब्बों को मिटा नहीं सकता है तो वे समझ जाते है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इनकी इसी क्षमता के कारण वे कविता भी लिख सकते हैं और व्यंग्यों को भी समझ लेते हैं।
- व्यक्तिगत आख्यान : किशोर स्वयं को विशिष्ट मानते हैं और जोखिम लेने में संकोच नहीं करते। वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे- अपने समवर्ती वर्ग तथा परिवार की सहायता करना, देश की सेवा करना आदि। लेकिन कभी-कभी जोखिमपूर्ण कार्यों को करने का खतरा भी उठाते हैं, जैसे- तीव्र गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट पहने दुपहिया के पीछे बैठना आदि। इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- सुव्यवस्थित विचारधारा : किशोर जटिल समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं और तार्किक रूप से निर्णय लेते हैं। जैसे, यात्रा योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना।
- आदर्शवादिता : किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता आदर्शवादिता है। उनमें सही और गलत के प्रति गहरी समझ होती है। आदर्शवादिता के कारण सकारात्मक सोच तथा क्रियाशीलता का विकास होता है। जैसे- अनेक नवयुवक आपदा, विवाद जैसी कठिन परिस्थितियों में सहायता करते हैं।
- काल्पनिक दर्शक : किशोरों को लगता है कि हर कोई उन्हें देख रहा है। उदाहरण के लिए, यदि उनकी टी-शर्ट में एक छोटा-सा छिद्र है तो उन्हें लगता है कि हर कोई उस छेद को देख रहा है। वे अपने परिवेश के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं।
अथवा
किशोरों के व्यक्तित्व पर मीडिया के दो नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? माता-पिता किन तीन तरीकों से इस प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं?
उत्तर - किशोरों के व्यक्तित्व पर मीडिया के दो नकारात्मक प्रभाव :
- किशोर प्रायः प्रसिद्ध लोगों से काफी प्रभावित होते हैं और फिल्मी सितारों, व्यावसायिक खिलाड़ियों तथा टेलीविजन के कलाकारों को अपना आदर्श मानकर अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास करने के बजाय दूसरों की नकल करने लगते हैं।
- कलाकार तथा मॉडल अपने आदर्श शारीरिक आकार से युवावर्ग को प्रभावित करते हैं। अधिकतर लड़कियाँ अपने आहार को नियंत्रित करने लगती हैं जिसके कारण अनेक प्रकार के भोजन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही, लड़के भी मांसपेशियाँ बढ़ाने के जुनून में वजन प्रशिक्षण पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। वे अपनी माँसपेशियों को बढ़ाने तथा अधिक भार उठाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए दवाईयाँ तथा आहारीय पूरक लेते हैं।
माता-पिता मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं :
- कल्पना और वास्तविकता में अंतर समझाना : माता-पिता किशोरों को बता सकते हैं कि मीडिया में दिखाई जाने वाली छवियाँ अक्सर वास्तविकता से दूर होती हैं और उन्हें बिना सोचे-समझे नहीं अपनाना चाहिए।
- हिंसा और जोखिम भरे व्यवहार के परिणामों पर चर्चा करना : किशोरों को यह समझाया जा सकता है कि मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा और जोखिमपूर्ण कार्य वास्तविक जीवन में खतरनाक हो सकते हैं।
- समीक्षात्मक विचारधारा और निर्णय कौशल का विकास करना : माता-पिता किशोरों में सही-गलत की पहचान करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर सकते हैं, जिससे वे मीडिया संदेशों का सही मूल्यांकन कर सकें।
47. अपनी बहन को रंगीन सूती कपड़े घर पर धोने के लिए कोई पाँच निर्देश दीजिए।
उत्तर - रंगीन सूती कपड़े घर पर धोने के लिए निर्देश इस प्रकार हैं :
- यदि किसी सूती कपड़े का रंग निकलता हो तो उसे भिगो कर न रखें।
- रंगीन सूती कपड़ों को धोने के लिए हल्के या न्यूट्रल साबुन का प्रयोग करें।
- रंगीन सूती कपड़ों को धोने के लिए मसलने व निचोड़ने की पद्धति का प्रयोग करें।
- कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ें तथा अंतिम बारी में कपड़े को उल्टा करके उस पर माँड लगाएँ।
- रंगीन सूती कपड़ों को छाया में सुखाना चाहिए। यदि कपड़े में कुछ नमी रह जाए तो इस्त्री करने के पश्चात जब कपड़ें पूरी तरह से सूख जाएँ तभी उन्हें संभाल कर रखें।
अथवा
आपने एक रंगाई इकाई स्थापित की है। अपने कर्मचारियों को बाटिक प्रक्रिया और चार अलग-अलग चरणों के बारे में समझाइए, जिनसे विभिन्न वस्त्रों को रंगा जाता है।
उत्तर - बाटिक प्रक्रिया का परिचय : बाटिक एक प्राचीन कला है, जिसमें मोम और रंगों का उपयोग करके कपड़े पर सुंदर और जटिल डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कपड़े के उन हिस्सों को मोम से ढक दिया जाता है, जिन्हें रंग से बचाना होता है, और फिर डाई का उपयोग किया जाता है।
बाटिक प्रक्रिया के चार चरण :
1) डिज़ाइन और मोम लगाना (Waxing) :
- कपड़े पर मनचाहा डिज़ाइन तैयार किया जाता है।
- गर्म मोम (पिघला हुआ) का उपयोग करके डिज़ाइन के अनुसार कपड़े के कुछ हिस्सों को कवर किया जाता है।
- यह मोम उस क्षेत्र को डाई से बचाता है, जिससे पैटर्न उभरता है।
2) पहली रंगाई (Dyeing) :
- मोम लगे कपड़े को पहले हल्के रंग की डाई में डुबोया जाता है।
- मोम लगे हिस्से रंग से सुरक्षित रहते हैं, जबकि बाकी कपड़ा रंग को सोख लेता है।
- रंगाई के बाद कपड़े को सुखाया जाता है।
3) अधिक रंग और मोम लगाना (Waxing and Overdyeing) :
- डिज़ाइन में और गहराई और विविधता जोड़ने के लिए मोम को फिर से नए क्षेत्रों पर लगाया जाता है।
- कपड़े को एक गहरे रंग की डाई में फिर से डुबोया जाता है।
- यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सभी रंगों को प्राप्त नहीं कर लिया जाता।
4) मोम हटाना और अंतिम रूप (Wax Removal and Finishing) :
- कपड़े को गर्म पानी में उबालकर या इस्त्री करके मोम हटाया जाता है।
- मोम हटने के बाद कपड़े पर सुंदर और जटिल डिज़ाइन उभरकर आता है।
- अंतिम कपड़े को धोकर सुखाया जाता है और उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।
✅ सभी सटीक Question & Answer पाने के लिए यहाँ क्लिक करें!
Click Here For Home Science Q. 01-20
Click Here For Home Science Q. 21-31
Click Here For Home Science Q. 32-40